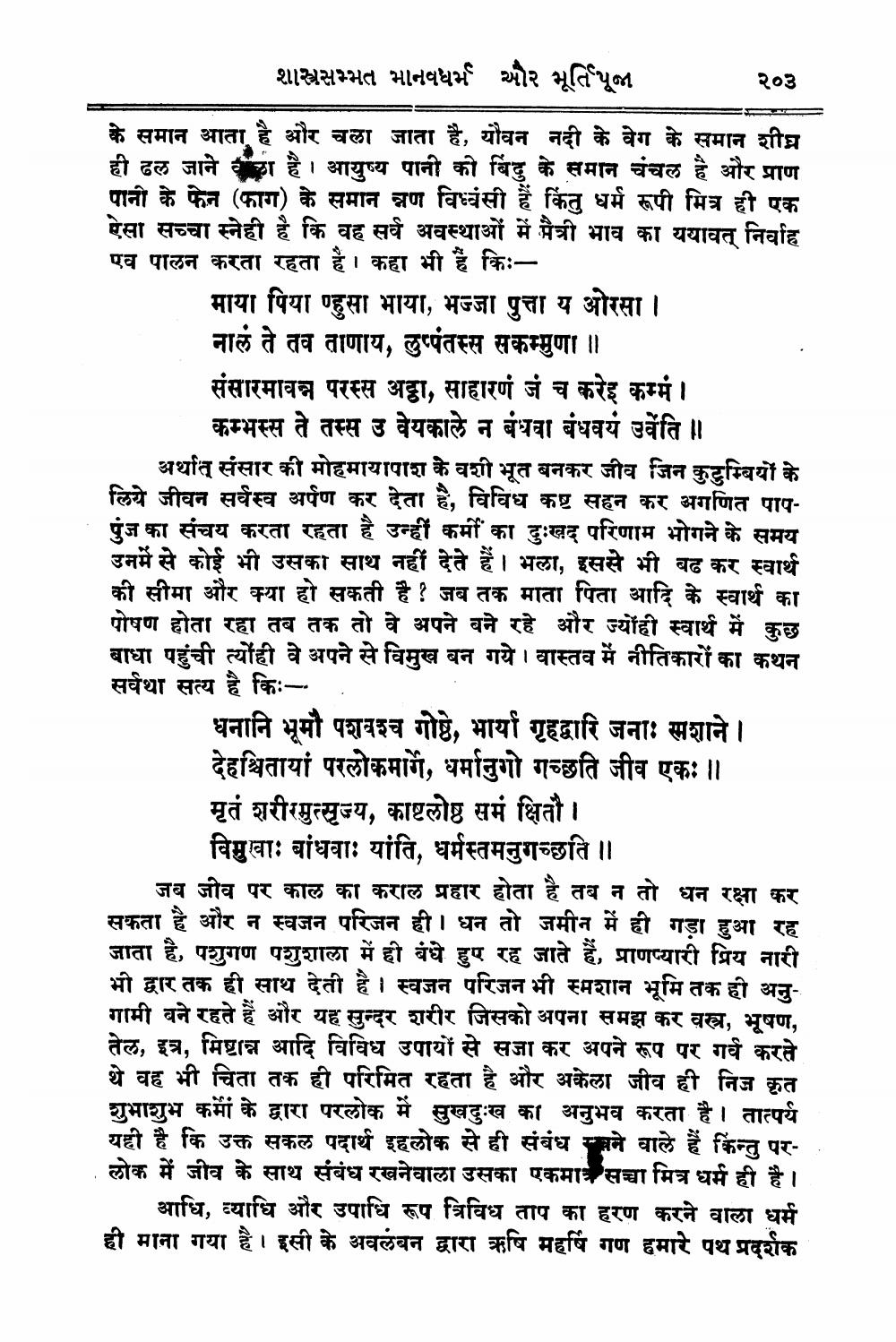________________
શાસ્ત્રસમ્મત માનવધર્મ ઔર મૂર્તિપૂજા
२०3
के समान आता है और चला जाता है, यौवन नदी के वेग के समान शीघ्र ही ढल जाने वाला है। आयुष्य पानी को बिंदु के समान चंचल है और प्राण पानी के फेन (फाग) के समान नण विध्वंसी हैं किंतु धर्म रूपी मित्र ही एक ऐसा सच्चा स्नेही है कि वह सर्व अवस्थाओं में मैत्री भाव का ययावत् निर्वाह एव पालन करता रहता है। कहा भी है किः
माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा। नालं ते तव ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ संसारमावन्न परस्स अट्ठा, साहारणं जंच करेइ कम्मं ।
कम्भस्स ते तस्स उ वेयकाले न बंधवा बंधवयं वेंति ॥ अर्थात् संसार की मोहमायापाश के वशीभूत बनकर जीव जिन कुटुम्बियों के लिये जीवन सर्वस्व अर्पण कर देता है, विविध कष्ट सहन कर अगणित पापपुंज का संचय करता रहता है उन्हीं कर्मी का दुःखद परिणाम भोगने के समय उनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देते हैं। भला, इससे भी बढ कर स्वार्थ की सीमा और क्या हो सकती है ? जब तक माता पिता आदि के स्वार्थ का पोषण होता रहा तब तक तो वे अपने बने रहे और ज्योंही स्वार्थ में कुछ बाधा पहुंची त्योंही वे अपने से विमुख बन गये । वास्तव में नीतिकारों का कथन सर्वथा सत्य है किः--
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः स्मशाने । देहश्चितायां परलोकमार्ग, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः॥ मृतं शरीरमुत्सृज्य, काष्टलोष्ठ समं क्षितौ ।
विमुखाः बांधवाः यांति, धर्मस्तमनुगच्छति ॥ जब जीव पर काल का कराल प्रहार होता है तब न तो धन रक्षा कर सकता है और न स्वजन परिजन ही। धन तो जमीन में ही गड़ा हुआ रह जाता है, पशुगण पशुशाला में ही बंधे हुए रह जाते है, प्राणप्यारी प्रिय नारी भी द्वार तक ही साथ देती है। स्वजन परिजन भी स्मशान भूमि तक ही अनुगामी बने रहते हैं और यह सुन्दर शरीर जिसको अपना समझ कर वस्त्र, भूषण, तेल, इत्र, मिष्टान्न आदि विविध उपायों से सजा कर अपने रूप पर गर्व करते थे वह भी चिता तक ही परिमित रहता है और अकेला जीव ही निज कृत शुभाशुभ कर्मों के द्वारा परलोक में सुखदुःख का अनुभव करता है। तात्पर्य यही है कि उक्त सकल पदार्थ इहलोक से ही संबंध स्मने वाले हैं किन्तु परलोक में जीव के साथ संबंध रखनेवाला उसका एकमात्र सच्चा मित्र धर्म ही है।
आधि, व्याधि और उपाधि रूप त्रिविध ताप का हरण करने वाला धर्म ही माना गया है। इसी के अवलंबन द्वारा ऋषि महर्षि गण हमारे पथ प्रदर्शक