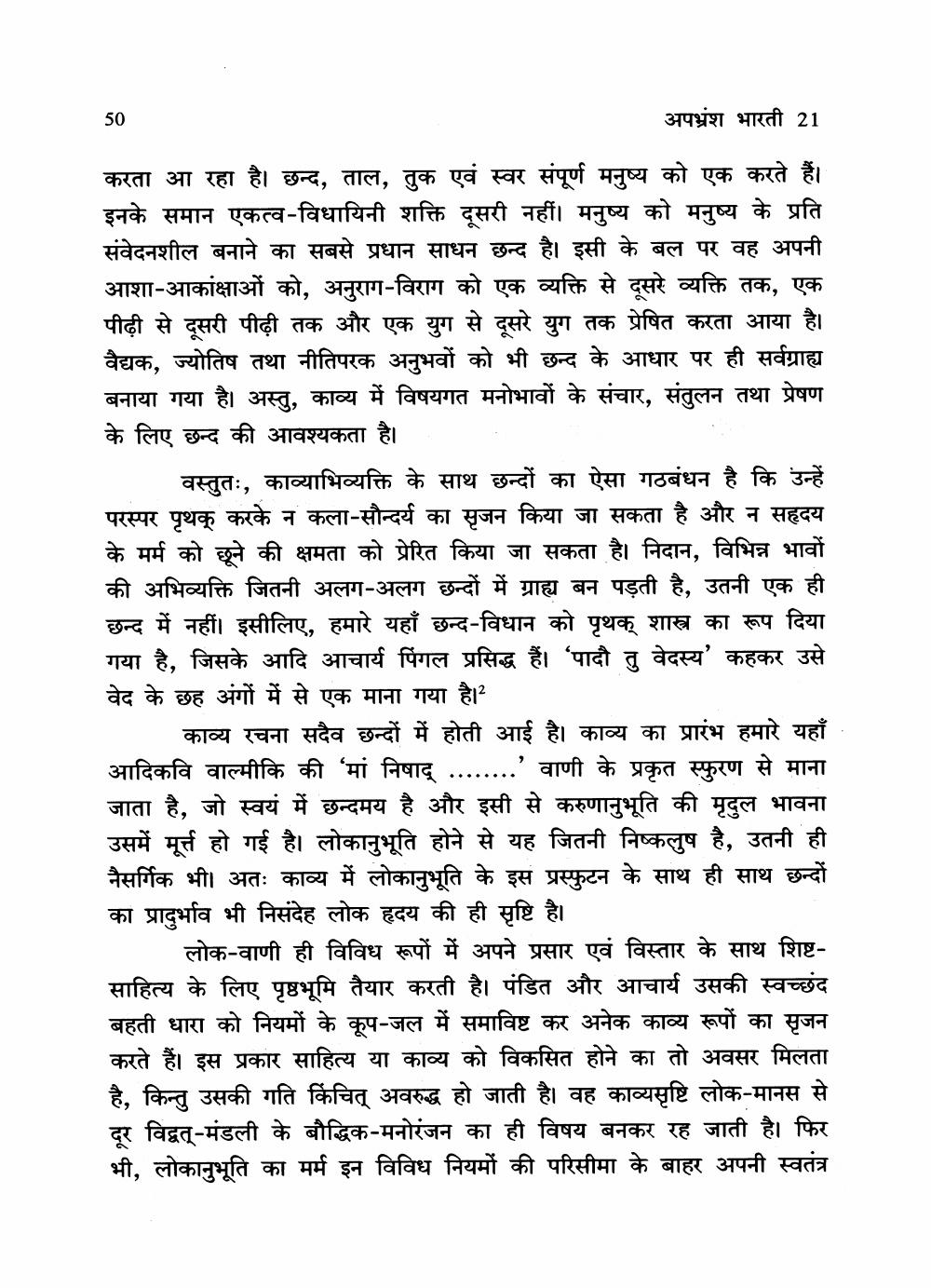________________
अपभ्रंश भारती 21
करता आ रहा है। छन्द, ताल, तुक एवं स्वर संपूर्ण मनुष्य को एक करते हैं। इनके समान एकत्व - विधायिनी शक्ति दूसरी नहीं। मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे प्रधान साधन छन्द है। इसी के बल पर वह अपनी आशा-आकांक्षाओं को, अनुराग विराग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और एक युग से दूसरे युग तक प्रेषित करता आया है। वैद्यक, ज्योतिष तथा नीतिपरक अनुभवों को भी छन्द के आधार पर ही सर्वग्राह्य बनाया गया है। अस्तु, काव्य में विषयगत मनोभावों के संचार, संतुलन तथा प्रेषण के लिए छन्द की आवश्यकता है।
50
वस्तुतः, काव्याभिव्यक्ति के साथ छन्दों का ऐसा गठबंधन है कि उन्हें परस्पर पृथक् करके न कला-सौन्दर्य का सृजन किया जा सकता है और न सहृदय के मर्म को छूने की क्षमता को प्रेरित किया जा सकता है। निदान, विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति जितनी अलग-अलग छन्दों में ग्राह्य बन पड़ती है, उतनी एक ही छन्द में नहीं। इसीलिए, हमारे यहाँ छन्द - विधान को पृथक् शास्त्र का रूप दिया गया है, जिसके आदि आचार्य पिंगल प्रसिद्ध हैं। 'पादौ तु वेदस्य' कहकर उसे वेद के छह अंगों में से एक माना गया है। 2
काव्य रचना सदैव छन्दों में होती आई है। काव्य का प्रारंभ हमारे यहाँ आदिकवि वाल्मीकि की 'मां निषाद् वाणी के प्रकृत स्फुरण से माना जाता है, जो स्वयं में छन्दमय है और इसी से करुणानुभूति की मृदुल भावना उसमें मूर्त हो गई है। लोकानुभूति होने से यह जितनी निष्कलुष है, उतनी ही नैसर्गिक भी। अतः काव्य में लोकानुभूति के इस प्रस्फुटन के साथ ही साथ छन्दों का प्रादुर्भाव भी निसंदेह लोक हृदय की ही सृष्टि है।
लोक-वाणी ही विविध रूपों में अपने प्रसार एवं विस्तार के साथ शिष्टसाहित्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। पंडित और आचार्य उसकी स्वच्छंद बहती धारा को नियमों के कूप-जल में समाविष्ट कर अनेक काव्य रूपों का सृजन करते हैं। इस प्रकार साहित्य या काव्य को विकसित होने का तो अवसर मिलता है, किन्तु उसकी गति किंचित् अवरुद्ध हो जाती है। वह काव्यसृष्टि लोक-मानस से दूर विद्वत्-मंडली के बौद्धिक-मनोरंजन का ही विषय बनकर रह जाती है। फिर भी, लोकानुभूति का मर्म इन विविध नियमों की परिसीमा के बाहर अपनी स्वतंत्र