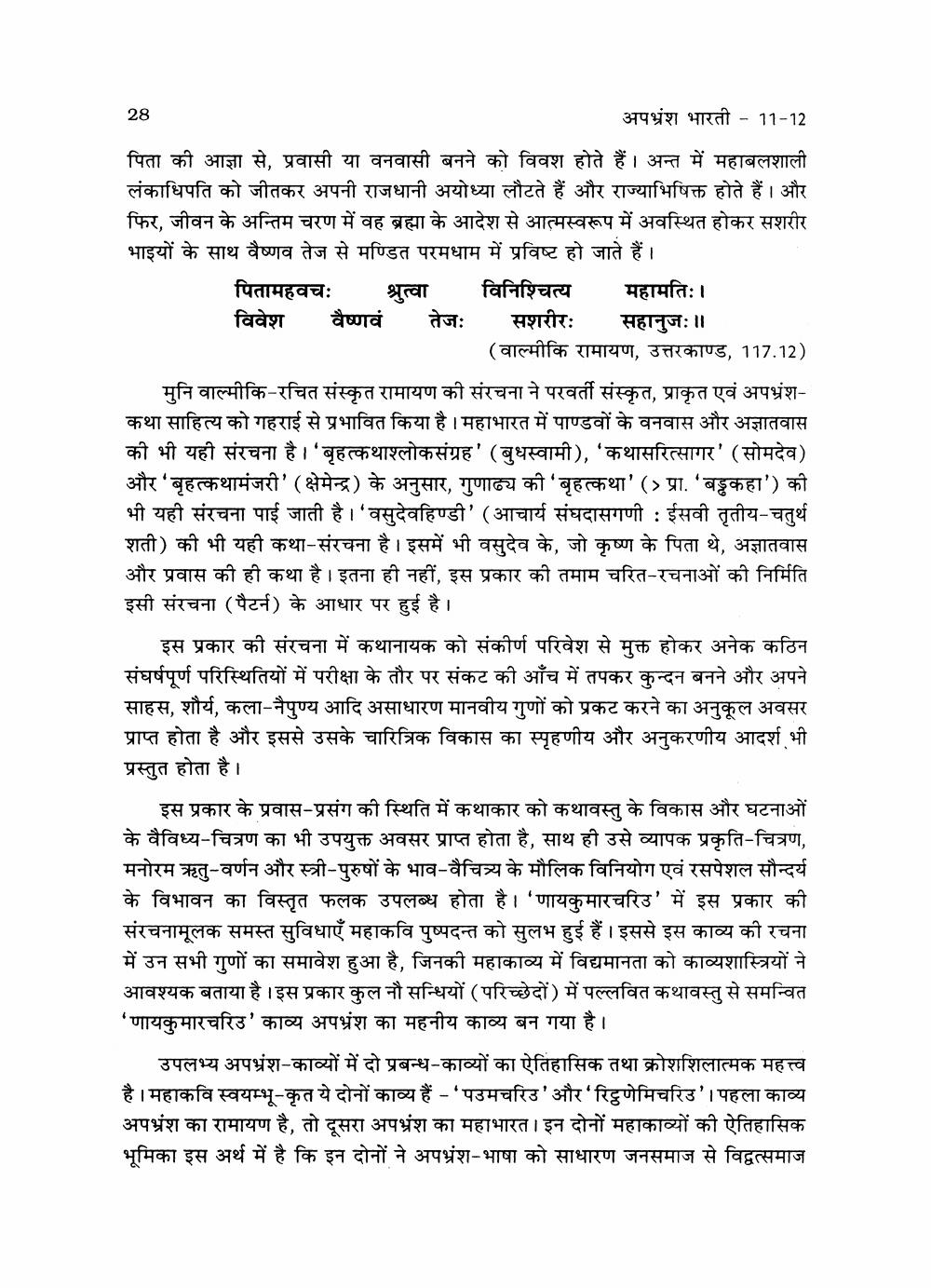________________
28
अपभ्रंश भारती - 11-12 पिता की आज्ञा से, प्रवासी या वनवासी बनने को विवश होते हैं। अन्त में महाबलशाली लंकाधिपति को जीतकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटते हैं और राज्याभिषिक्त होते हैं। और फिर, जीवन के अन्तिम चरण में वह ब्रह्मा के आदेश से आत्मस्वरूप में अवस्थित होकर सशरीर भाइयों के साथ वैष्णव तेज से मण्डित परमधाम में प्रविष्ट हो जाते हैं।
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः। विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः॥
(वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाण्ड, 117.12) मुनि वाल्मीकि-रचित संस्कृत रामायण की संरचना ने परवर्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंशकथा साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। महाभारत में पाण्डवों के वनवास और अज्ञातवास की भी यही संरचना है। 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' (बुधस्वामी), 'कथासरित्सागर' (सोमदेव) और 'बृहत्कथामंजरी' (क्षेमेन्द्र) के अनुसार, गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' (> प्रा. 'बड्डकहा') की भी यही संरचना पाई जाती है। 'वसुदेवहिण्डी' (आचार्य संघदासगणी : ईसवी तृतीय-चतुर्थ शती) की भी यही कथा-संरचना है। इसमें भी वसुदेव के, जो कृष्ण के पिता थे, अज्ञातवास और प्रवास की ही कथा है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की तमाम चरित-रचनाओं की निर्मिति इसी संरचना (पैटर्न) के आधार पर हुई है।
इस प्रकार की संरचना में कथानायक को संकीर्ण परिवेश से मुक्त होकर अनेक कठिन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में परीक्षा के तौर पर संकट की आँच में तपकर कुन्दन बनने और अपने साहस, शौर्य, कला-नैपण्य आदि असाधारण मानवीय गणों को प्रकट करने का अनकल अवसर प्राप्त होता है और इससे उसके चारित्रिक विकास का स्पृहणीय और अनुकरणीय आदर्श भी प्रस्तुत होता है।
इस प्रकार के प्रवास-प्रसंग की स्थिति में कथाकार को कथावस्तु के विकास और घटनाओं के वैविध्य-चित्रण का भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है, साथ ही उसे व्यापक प्रकृति-चित्रण, मनोरम ऋतु-वर्णन और स्त्री-पुरुषों के भाव-वैचित्र्य के मौलिक विनियोग एवं रसपेशल सौन्दर्य के विभावन का विस्तृत फलक उपलब्ध होता है। ‘णायकुमारचरिउ' में इस प्रकार की संरचनामूलक समस्त सुविधाएँ महाकवि पुष्पदन्त को सुलभ हुई हैं। इससे इस काव्य की रचना में उन सभी गुणों का समावेश हुआ है, जिनकी महाकाव्य में विद्यमानता को काव्यशास्त्रियों ने आवश्यक बताया है। इस प्रकार कुल नौ सन्धियों (परिच्छेदों) में पल्लवित कथावस्तु से समन्वित 'णायकुमारचरिउ' काव्य अपभ्रंश का महनीय काव्य बन गया है।
उपलभ्य अपभ्रंश-काव्यों में दो प्रबन्ध-काव्यों का ऐतिहासिक तथा क्रोशशिलात्मक महत्त्व है। महाकवि स्वयम्भू-कृत ये दोनों काव्य हैं - 'पउमचरिउ' और 'रिट्ठणेमिचरिउ'। पहला काव्य अपभ्रंश का रामायण है, तो दूसरा अपभ्रंश का महाभारत । इन दोनों महाकाव्यों की ऐतिहासिक भूमिका इस अर्थ में है कि इन दोनों ने अपभ्रंश-भाषा को साधारण जनसमाज से विद्वत्समाज