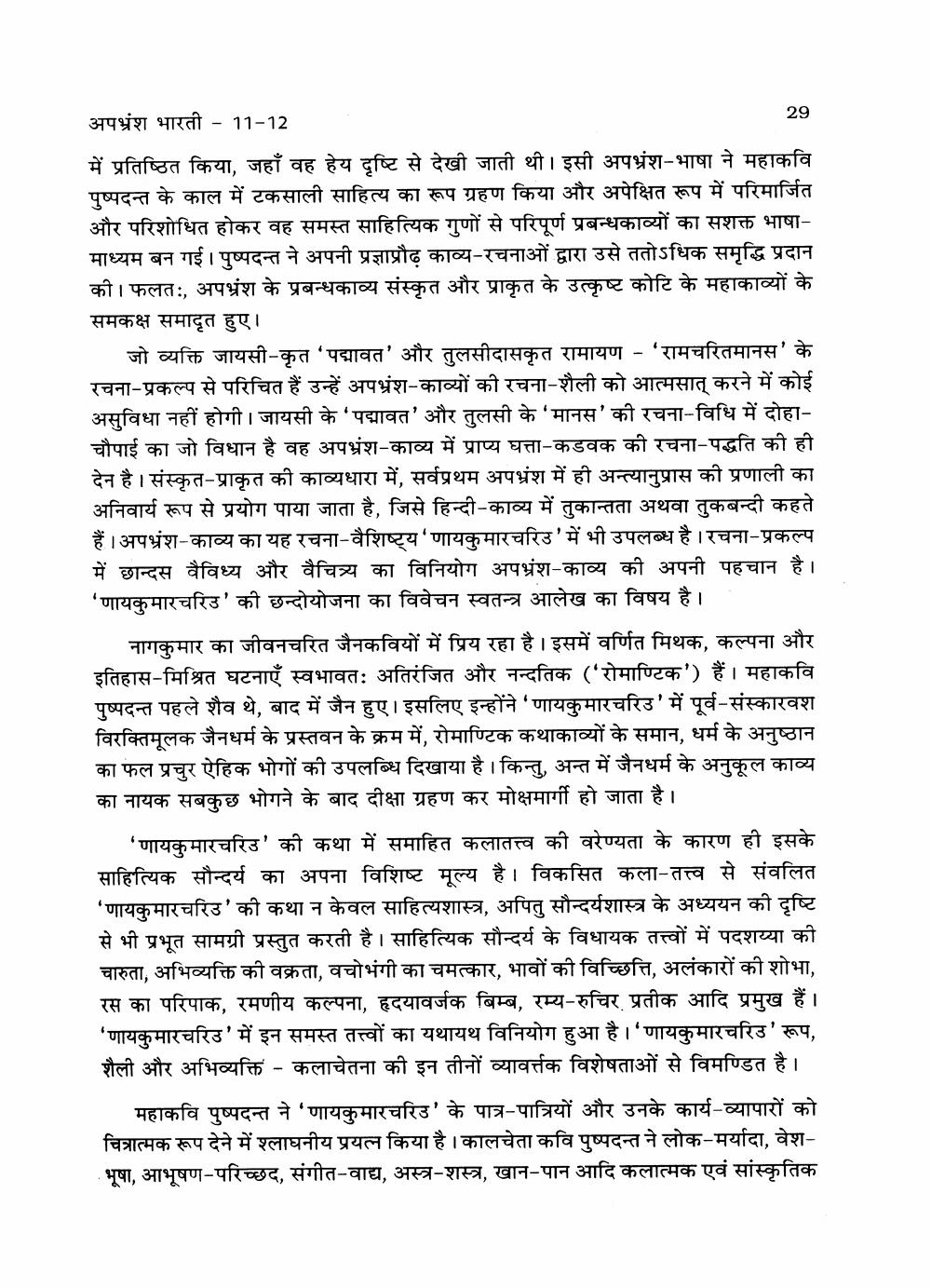________________
29
अपभ्रंश भारती - 11-12 में प्रतिष्ठित किया, जहाँ वह हेय दृष्टि से देखी जाती थी। इसी अपभ्रंश-भाषा ने महाकवि पुष्पदन्त के काल में टकसाली साहित्य का रूप ग्रहण किया और अपेक्षित रूप में परिमार्जित
और परिशोधित होकर वह समस्त साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण प्रबन्धकाव्यों का सशक्त भाषामाध्यम बन गई। पुष्पदन्त ने अपनी प्रज्ञाप्रौढ़ काव्य-रचनाओं द्वारा उसे ततोऽधिक समृद्धि प्रदान की। फलतः, अपभ्रंश के प्रबन्धकाव्य संस्कृत और प्राकृत के उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्यों के समकक्ष समादृत हुए। ___ जो व्यक्ति जायसी-कृत 'पद्मावत' और तुलसीदासकृत रामायण - 'रामचरितमानस' के रचना-प्रकल्प से परिचित हैं उन्हें अपभ्रंश-काव्यों की रचना-शैली को आत्मसात् करने में कोई असुविधा नहीं होगी। जायसी के 'पद्मावत' और तुलसी के 'मानस' की रचना-विधि में दोहाचौपाई का जो विधान है वह अपभ्रंश-काव्य में प्राप्य पत्ता-कडवक की रचना-पद्धति की ही देन है। संस्कृत-प्राकृत की काव्यधारा में, सर्वप्रथम अपभ्रंश में ही अन्त्यानुप्रास की प्रणाली का अनिवार्य रूप से प्रयोग पाया जाता है, जिसे हिन्दी-काव्य में तुकान्तता अथवा तुकबन्दी कहते हैं। अपभ्रंश-काव्य का यह रचना-वैशिष्ट्य 'णायकुमारचरिउ' में भी उपलब्ध है। रचना-प्रकल्प में छान्दस वैविध्य और वैचित्र्य का विनियोग अपभ्रंश-काव्य की अपनी पहचान है। 'णायकुमारचरिउ' की छन्दोयोजना का विवेचन स्वतन्त्र आलेख का विषय है।
नागकुमार का जीवनचरित जैनकवियों में प्रिय रहा है। इसमें वर्णित मिथक, कल्पना और इतिहास-मिश्रित घटनाएँ स्वभावतः अतिरंजित और नन्दतिक ('रोमाण्टिक') हैं। महाकवि पुष्पदन्त पहले शैव थे, बाद में जैन हुए। इसलिए इन्होंने 'णायकुमारचरिउ' में पूर्व-संस्कारवश विरक्तिमूलक जैनधर्म के प्रस्तवन के क्रम में, रोमाण्टिक कथाकाव्यों के समान, धर्म के अनुष्ठान का फल प्रचुर ऐहिक भोगों की उपलब्धि दिखाया है। किन्तु, अन्त में जैनधर्म के अनुकूल काव्य का नायक सबकुछ भोगने के बाद दीक्षा ग्रहण कर मोक्षमार्गी हो जाता है। ___णायकुमारचरिउ' की कथा में समाहित कलातत्त्व की वरेण्यता के कारण ही इसके साहित्यिक सौन्दर्य का अपना विशिष्ट मूल्य है। विकसित कला-तत्त्व से संवलित 'णायकुमारचरिउ' की कथा न केवल साहित्यशास्त्र, अपितु सौन्दर्यशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से भी प्रभूत सामग्री प्रस्तुत करती है। साहित्यिक सौन्दर्य के विधायक तत्त्वों में पदशय्या की चारुता, अभिव्यक्ति की वक्रता, वचोभंगी का चमत्कार, भावों की विच्छित्ति, अलंकारों की शोभा, रस का परिपाक, रमणीय कल्पना, हृदयावर्जक बिम्ब, रम्य-रुचिर प्रतीक आदि प्रमुख हैं। 'णायकुमारचरिउ' में इन समस्त तत्त्वों का यथायथ विनियोग हुआ है। ‘णायकुमारचरिउ' रूप, शैली और अभिव्यक्ति - कलाचेतना की इन तीनों व्यावर्त्तक विशेषताओं से विमण्डित है।
महाकवि पुष्पदन्त ने 'णायकुमारचरिउ' के पात्र-पात्रियों और उनके कार्य-व्यापारों को चित्रात्मक रूप देने में श्लाघनीय प्रयत्न किया है । कालचेता कवि पुष्पदन्त ने लोक-मर्यादा, वेशभूषा, आभूषण-परिच्छद, संगीत-वाद्य, अस्त्र-शस्त्र, खान-पान आदि कलात्मक एवं सांस्कृतिक