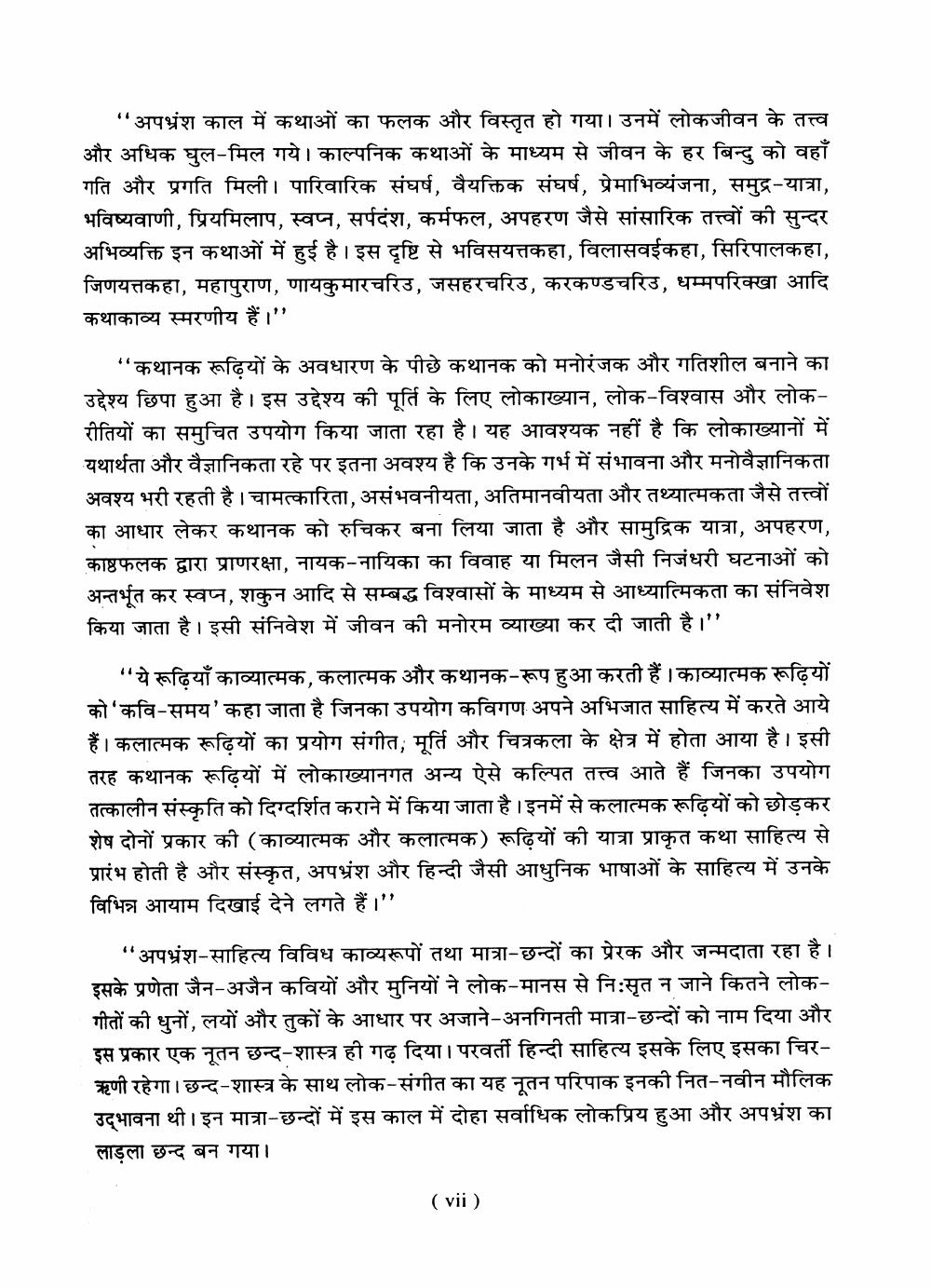________________
"अपभ्रंश काल में कथाओं का फलक और विस्तृत हो गया। उनमें लोकजीवन के तत्त्व और अधिक घुल-मिल गये। काल्पनिक कथाओं के माध्यम से जीवन के हर बिन्दु को वहाँ गति और प्रगति मिली। पारिवारिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, प्रेमाभिव्यंजना, समुद्र-यात्रा, भविष्यवाणी, प्रियमिलाप, स्वप्न, सर्पदंश, कर्मफल, अपहरण जैसे सांसारिक तत्त्वों की सुन्दर अभिव्यक्ति इन कथाओं में हुई है। इस दृष्टि से भविसयत्तकहा, विलासवईकहा, सिरिपालकहा, जिणयत्तकहा, महापुराण, णायकुमारचरिउ, जसहरचरिउ, करकण्डचरिउ, धम्मपरिक्खा आदि कथाकाव्य स्मरणीय हैं।"
"कथानक रूढ़ियों के अवधारण के पीछे कथानक को मनोरंजक और गतिशील बनाने का उद्देश्य छिपा हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकाख्यान, लोक-विश्वास और लोकरीतियों का समुचित उपयोग किया जाता रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि लोकाख्यानों में यथार्थता और वैज्ञानिकता रहे पर इतना अवश्य है कि उनके गर्भ में संभावना और मनोवैज्ञानिकता अवश्य भरी रहती है । चामत्कारिता, असंभवनीयता, अतिमानवीयता और तथ्यात्मकता जैसे तत्त्वों का आधार लेकर कथानक को रुचिकर बना लिया जाता है और सामुद्रिक यात्रा, अपहरण, काष्ठफलक द्वारा प्राणरक्षा, नायक-नायिका का विवाह या मिलन जैसी निजंधरी घटनाओं को अन्तर्भूत कर स्वप्न, शकुन आदि से सम्बद्ध विश्वासों के माध्यम से आध्यात्मिकता का संनिवेश किया जाता है। इसी संनिवेश में जीवन की मनोरम व्याख्या कर दी जाती है।"
"ये रूढ़ियाँ काव्यात्मक, कलात्मक और कथानक-रूप हुआ करती हैं। काव्यात्मक रूढ़ियों को'कवि-समय' कहा जाता है जिनका उपयोग कविगण अपने अभिजात साहित्य में करते आये हैं। कलात्मक रूढ़ियों का प्रयोग संगीत, मूर्ति और चित्रकला के क्षेत्र में होता आया है। इसी तरह कथानक रूढ़ियों में लोकाख्यानगत अन्य ऐसे कल्पित तत्त्व आते हैं जिनका उपयोग तत्कालीन संस्कृति को दिग्दर्शित कराने में किया जाता है। इनमें से कलात्मक रूढ़ियों को छोड़कर शेष दोनों प्रकार की (काव्यात्मक और कलात्मक) रूढ़ियों की यात्रा प्राकृत कथा साहित्य से प्रारंभ होती है और संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी जैसी आधुनिक भाषाओं के साहित्य में उनके विभिन्न आयाम दिखाई देने लगते हैं।"
"अपभ्रंश-साहित्य विविध काव्यरूपों तथा मात्रा-छन्दों का प्रेरक और जन्मदाता रहा है। इसके प्रणेता जैन-अजैन कवियों और मुनियों ने लोक-मानस से निःसृत न जाने कितने लोकगीतों की धुनों, लयों और तुकों के आधार पर अजाने-अनगिनती मात्रा-छन्दों को नाम दिया और इस प्रकार एक नूतन छन्द-शास्त्र ही गढ़ दिया। परवर्ती हिन्दी साहित्य इसके लिए इसका चिरऋणी रहेगा। छन्द-शास्त्र के साथ लोक-संगीत का यह नूतन परिपाक इनकी नित-नवीन मौलिक उद्भावना थी। इन मात्रा-छन्दों में इस काल में दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ और अपभ्रंश का लाडला छन्द बन गया।
(vii)