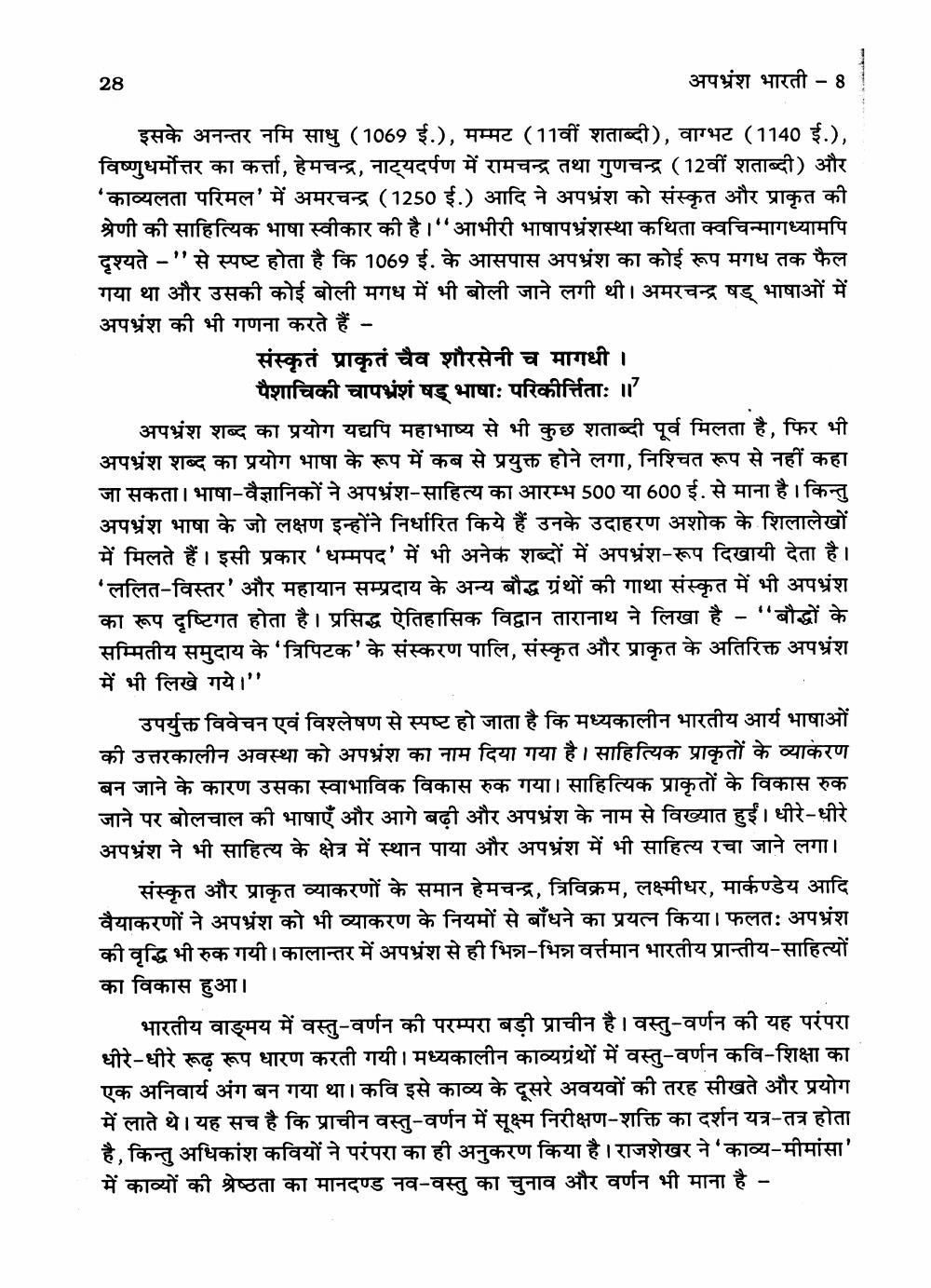________________
28
अपभ्रंश भारती - 8
इसके अनन्तर नमि साधु (1069 ई.), मम्मट (11वीं शताब्दी), वाग्भट (1140 ई.), विष्णुधर्मोत्तर का कर्ता, हेमचन्द्र, नाट्यदर्पण में रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र (12वीं शताब्दी) और 'काव्यलता परिमल' में अमरचन्द्र (1250 ई.) आदि ने अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत की श्रेणी की साहित्यिक भाषा स्वीकार की है। "आभीरी भाषापभ्रंशस्था कथिता क्वचिन्मागध्यामपि दृश्यते -" से स्पष्ट होता है कि 1069 ई. के आसपास अपभ्रंश का कोई रूप मगध तक फैल गया था और उसकी कोई बोली मगध में भी बोली जाने लगी थी। अमरचन्द्र षड् भाषाओं में अपभ्रंश की भी गणना करते हैं -
संस्कृतं प्राकृतं चैव शौरसेनी च मागधी।
पैशाचिकी चापभ्रंशं षड् भाषा: परिकीर्त्तिताः ॥' अपभ्रंश शब्द का प्रयोग यद्यपि महाभाष्य से भी कुछ शताब्दी पूर्व मिलता है, फिर भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में कब से प्रयुक्त होने लगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भाषा-वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश-साहित्य का आरम्भ 500 या 600 ई. से माना है। किन्तु अपभ्रंश भाषा के जो लक्षण इन्होंने निर्धारित किये हैं उनके उदाहरण अशोक के शिलालेखों
ते हैं। इसी प्रकार 'धम्मपद' में भी अनेक शब्दों में अपभ्रंश-रूप दिखायी देता है। 'ललित-विस्तर' और महायान सम्प्रदाय के अन्य बौद्ध ग्रंथों की गाथा संस्कृत में भी अपभ्रंश का रूप दृष्टिगत होता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान तारानाथ ने लिखा है - "बौद्धों के सम्मितीय समुदाय के 'त्रिपिटक' के संस्करण पालि, संस्कृत और प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रंश में भी लिखे गये।"
उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की उत्तरकालीन अवस्था को अपभ्रंश का नाम दिया गया है। साहित्यिक प्राकृतों के व्याकरण बन जाने के कारण उसका स्वाभाविक विकास रुक गया। साहित्यिक प्राकृतों के विकास रुक जाने पर बोलचाल की भाषाएँ और आगे बढ़ी और अपभ्रंश के नाम से विख्यात हुईं। धीरे-धीरे अपभ्रंश ने भी साहित्य के क्षेत्र में स्थान पाया और अपभ्रंश में भी साहित्य रचा जाने लगा।
संस्कृत और प्राकृत व्याकरणों के समान हेमचन्द्र, त्रिविक्रम, लक्ष्मीधर, मार्कण्डेय आदि वैयाकरणों ने अपभ्रंश को भी व्याकरण के नियमों से बाँधने का प्रयत्न किया। फलतः अपभ्रंश की वृद्धि भी रुक गयी। कालान्तर में अपभ्रंश से ही भिन्न-भिन्न वर्तमान भारतीय प्रान्तीय-साहित्यों का विकास हुआ।
भारतीय वाङ्मय में वस्तु-वर्णन की परम्परा बड़ी प्राचीन है। वस्तु-वर्णन की यह परंपरा धीरे-धीरे रूढ़ रूप धारण करती गयी। मध्यकालीन काव्यग्रंथों में वस्तु-वर्णन कवि-शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बन गया था। कवि इसे काव्य के दूसरे अवयवों की तरह सीखते और प्रयोग में लाते थे। यह सच है कि प्राचीन वस्तु-वर्णन में सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का दर्शन यत्र-तत्र होता है, किन्तु अधिकांश कवियों ने परंपरा का ही अनुकरण किया है। राजशेखर ने 'काव्य-मीमांसा' में काव्यों की श्रेष्ठता का मानदण्ड नव-वस्तु का चुनाव और वर्णन भी माना है -