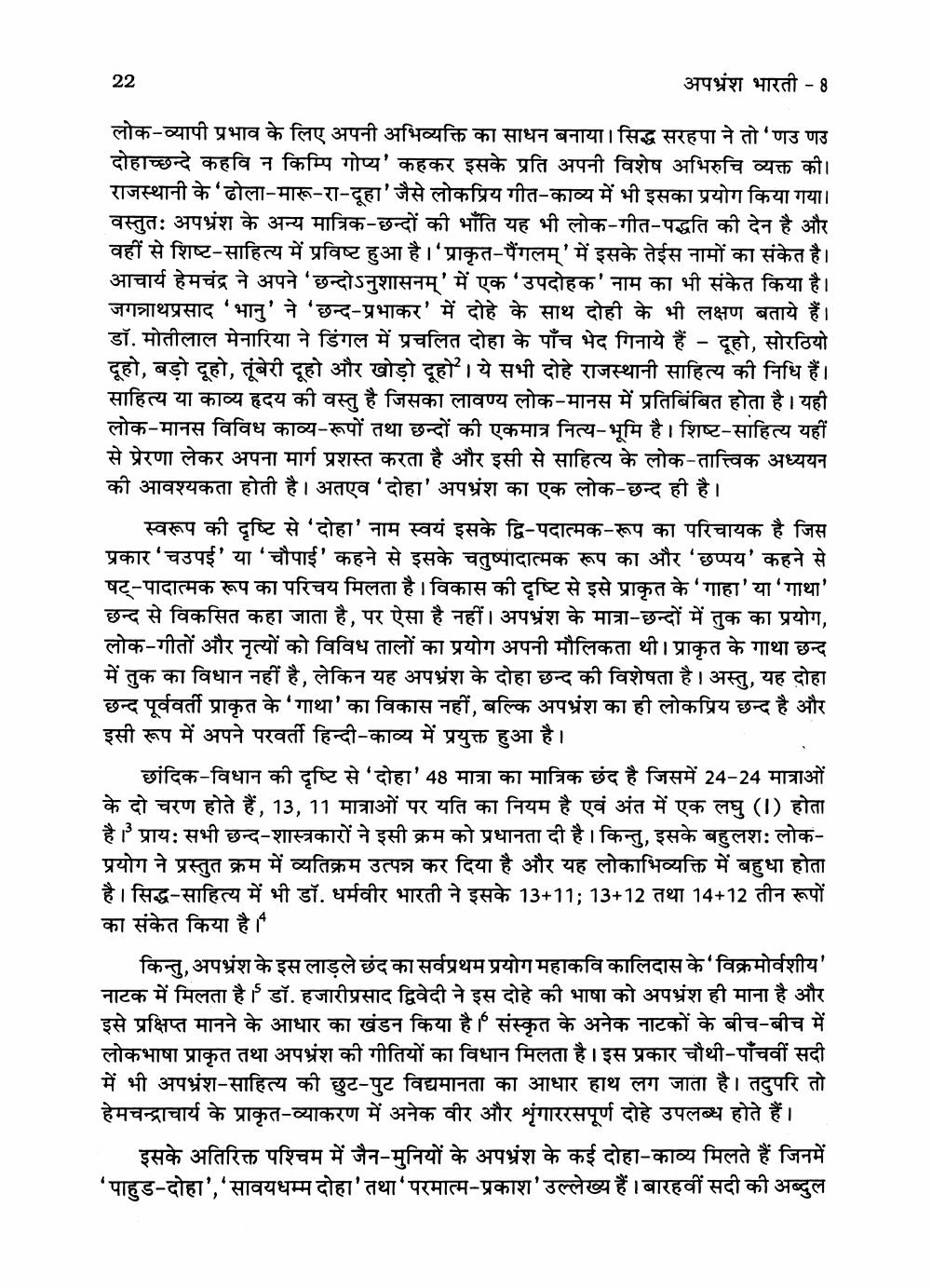________________
22
अपभ्रंश भारती - 8
लोक-व्यापी प्रभाव के लिए अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया। सिद्ध सरहपा ने तो 'णउ णउ दोहाच्छन्दे कहवि न किम्पि गोप्य' कहकर इसके प्रति अपनी विशेष अभिरुचि व्यक्त की। राजस्थानी के 'ढोला-मारू-रा-दूहा' जैसे लोकप्रिय गीत-काव्य में भी इसका प्रयोग किया गया। वस्तुतः अपभ्रंश के अन्य मात्रिक-छन्दों की भाँति यह भी लोक-गीत-पद्धति की देन है और वहीं से शिष्ट-साहित्य में प्रविष्ट हुआ है। 'प्राकृत-पैंगलम्' में इसके तेईस नामों का संकेत है। आचार्य हेमचंद्र ने अपने 'छन्दोऽनुशासनम्' में एक 'उपदोहक' नाम का भी संकेत किया है। जगन्नाथप्रसाद 'भानु' ने 'छन्द-प्रभाकर' में दोहे के साथ दोही के भी लक्षण बताये हैं। डॉ. मोतीलाल मेनारिया ने डिंगल में प्रचलित दोहा के पाँच भेद गिनाये हैं - दूहो, सोरठियो दूहो, बड़ो दूहो, तूंबेरी दूहो और खोड़ो दूहो। ये सभी दोहे राजस्थानी साहित्य की निधि हैं। साहित्य या काव्य हृदय की वस्तु है जिसका लावण्य लोक-मानस में प्रतिबिंबित होता है। यही लोक-मानस विविध काव्य-रूपों तथा छन्दों की एकमात्र नित्य-भूमि है। शिष्ट-साहित्य यहीं से प्रेरणा लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करता है और इसी से साहित्य के लोक-तात्त्विक अध्ययन की आवश्यकता होती है। अतएव 'दोहा' अपभ्रंश का एक लोक-छन्द ही है।
स्वरूप की दृष्टि से 'दोहा' नाम स्वयं इसके द्वि-पदात्मक-रूप का परिचायक है जिस प्रकार 'चउपई' या 'चौपाई' कहने से इसके चतष्पादात्मक रूप का और 'छप्पय' कहने से षट-पादात्मक रूप का परिचय मिलता है। विकास की दष्टि से इसे प्राकत के 'गाहा' या 'गाथा' छन्द से विकसित कहा जाता है, पर ऐसा है नहीं। अपभ्रंश के मात्रा-छन्दों में तुक का प्रयोग, लोक-गीतों और नृत्यों को विविध तालों का प्रयोग अपनी मौलिकता थी। प्राकृत के गाथा छन्द में तुक का विधान नहीं है, लेकिन यह अपभ्रंश के दोहा छन्द की विशेषता है। अस्तु, यह दोहा छन्द पूर्ववर्ती प्राकृत के 'गाथा' का विकास नहीं, बल्कि अपभ्रंश का ही लोकप्रिय छन्द है और इसी रूप में अपने परवर्ती हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त हुआ है।
छांदिक-विधान की दृष्टि से 'दोहा' 48 मात्रा का मात्रिक छंद है जिसमें 24-24 मात्राओं के दो चरण होते हैं, 13, 11 मात्राओं पर यति का नियम है एवं अंत में एक लघु (1) होता है। प्रायः सभी छन्द-शास्त्रकारों ने इसी क्रम को प्रधानता दी है। किन्तु, इसके बहुलशः लोकप्रयोग ने प्रस्तुत क्रम में व्यतिक्रम उत्पन्न कर दिया है और यह लोकाभिव्यक्ति में बहुधा होता है। सिद्ध-साहित्य में भी डॉ. धर्मवीर भारती ने इसके 13+11; 13+12 तथा 14+12 तीन रूपों का संकेत किया है।
किन्तु, अपभ्रंश के इस लाड़ले छंद का सर्वप्रथम प्रयोग महाकवि कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में मिलता है। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस दोहे की भाषा को अपभ्रंश ही माना है और इसे प्रक्षिप्त मानने के आधार का खंडन किया है। संस्कृत के अनेक नाटकों के बीच-बीच में लोकभाषा प्राकृत तथा अपभ्रंश की गीतियों का विधान मिलता है। इस प्रकार चौथी-पाँचवीं सदी में भी अपभ्रंश-साहित्य की छुट-पुट विद्यमानता का आधार हाथ लग जाता है। तदुपरि तो हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत-व्याकरण में अनेक वीर और शृंगाररसपूर्ण दोहे उपलब्ध होते हैं।
इसके अतिरिक्त पश्चिम में जैन-मुनियों के अपभ्रंश के कई दोहा-काव्य मिलते हैं जिनमें ‘पाहुड-दोहा', 'सावयधम्म दोहा' तथा परमात्म-प्रकाश' उल्लेख्य हैं। बारहवीं सदी की अब्दुल