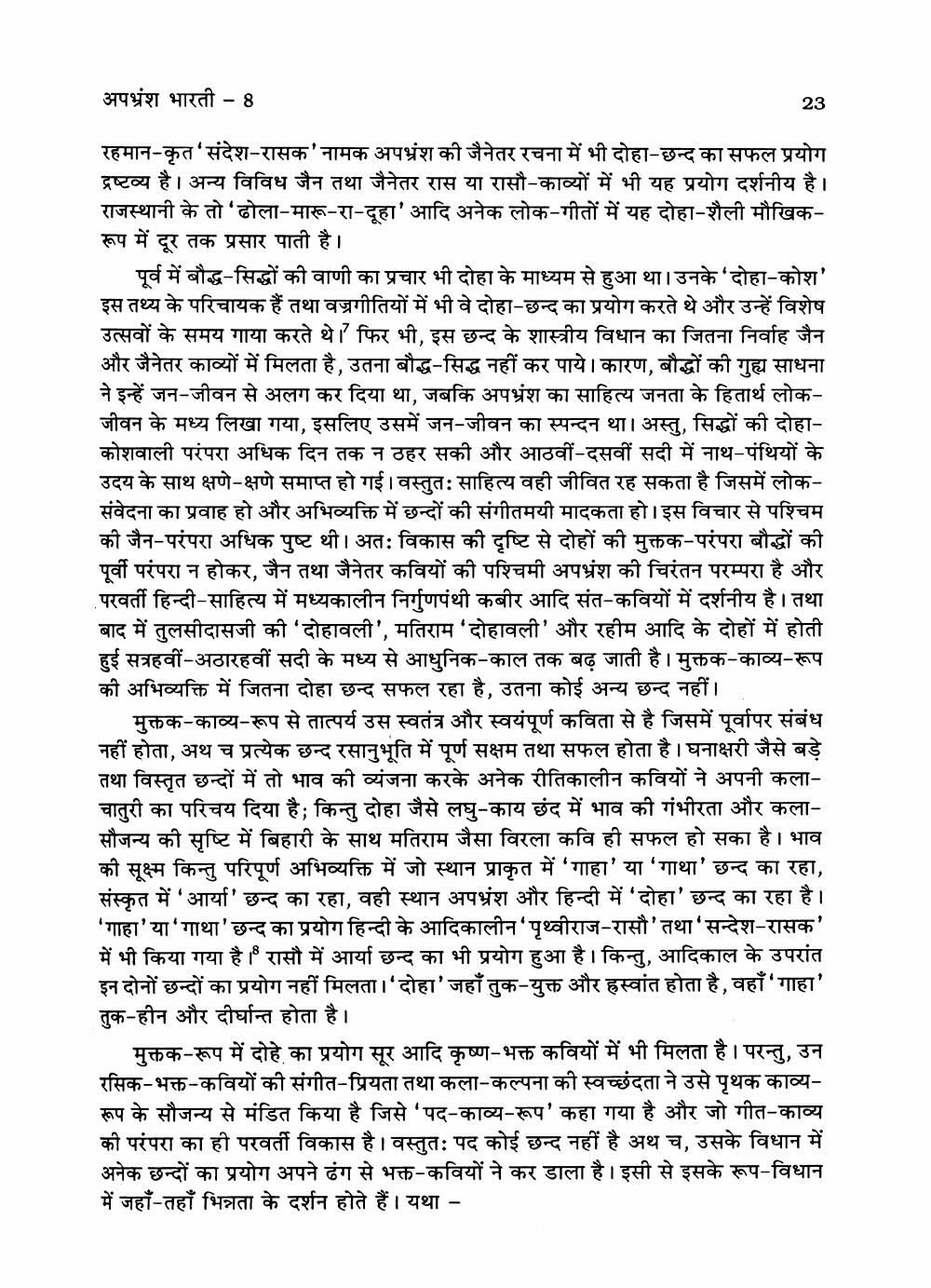________________
अपभ्रंश भारती
-
8
23
रहमान - कृत 'संदेश- रासक' नामक अपभ्रंश की जैनेतर रचना में भी दोहा-छन्द का सफल प्रयोग द्रष्टव्य है । अन्य विविध जैन तथा जैनेतर रास या रासौ-काव्यों में भी यह प्रयोग दर्शनीय है । राजस्थानी के तो 'ढोला-मारू-रा- दूहा' आदि अनेक लोक-गीतों में यह दोहा-शैली मौखिकरूप में दूर तक प्रसार पाती है।
पूर्व में बौद्ध-सिद्धों की वाणी का प्रचार भी दोहा के माध्यम से हुआ था । उनके 'दोहा-कोश' इस तथ्य के परिचायक हैं तथा वज्रगीतियों में भी वे दोहा-छन्द का प्रयोग करते थे और उन्हें विशेष उत्सवों के समय गाया करते थे। फिर भी, इस छन्द के शास्त्रीय विधान का जितना निर्वाह जैन और जैनेतर काव्यों में मिलता है, उतना बौद्ध-सिद्ध नहीं कर पाये । कारण, , बौद्धों की गुह्य साधना ने इन्हें जन-जीवन से अलग कर दिया था, जबकि अपभ्रंश का साहित्य जनता के हितार्थ लोकजीवन के मध्य लिखा गया, इसलिए उसमें जन-जीवन का स्पन्दन था । अस्तु, सिद्धों की दोहाकोशवाली परंपरा अधिक दिन तक न ठहर सकी और आठवीं दसवीं सदी में नाथ-पंथियों के उदय के साथ क्षण-क्षणे समाप्त हो गई। वस्तुत: साहित्य वही जीवित रह सकता है जिसमें लोकसंवेदना का प्रवाह हो और अभिव्यक्ति में छन्दों की संगीतमयी मादकता हो। इस विचार से पश्चिम की जैन परंपरा अधिक पुष्ट थी । अतः विकास की दृष्टि से दोहों की मुक्तक-परंपरा बौद्धों की पूर्वी परंपरा न होकर, जैन तथा जैनेतर कवियों की पश्चिमी अपभ्रंश की चिरंतन परम्परा है और परवर्ती हिन्दी-साहित्य में मध्यकालीन निर्गुणपंथी कबीर आदि संत कवियों में दर्शनीय है । तथा बाद में तुलसीदासजी की 'दोहावली', मतिराम 'दोहावली' और रहीम आदि के दोहों में होती हुई सत्रहवीं - अठारहवीं सदी के मध्य से आधुनिक काल तक बढ़ जाती है। मुक्तक काव्य-रूप की अभिव्यक्ति में जितना दोहा छन्द सफल रहा है, उतना कोई अन्य छन्द नहीं ।
मुक्तक-काव्य रूप से तात्पर्य उस स्वतंत्र और स्वयंपूर्ण कविता से है जिसमें पूर्वापर संबंध नहीं होता, अथ च प्रत्येक छन्द रसानुभूति में पूर्ण सक्षम तथा सफल होता है। घनाक्षरी जैसे बड़े तथा विस्तृत छन्दों में तो भाव की व्यंजना करके अनेक रीतिकालीन कवियों ने अपनी कलाचातुरी का परिचय दिया है; किन्तु दोहा जैसे लघु-काय छंद में भाव की गंभीरता और कलासौजन्य की सृष्टि में बिहारी के साथ मतिराम जैसा विरला कवि ही सफल हो सका है। भाव की सूक्ष्म किन्तु परिपूर्ण अभिव्यक्ति में जो स्थान प्राकृत में 'गाहा' या 'गाथा' छन्द का रहा, संस्कृत में 'आर्या' छन्द का रहा, वही स्थान अपभ्रंश और हिन्दी में 'दोहा' छन्द का रहा 'गाहा' या 'गाथा' छन्द का प्रयोग हिन्दी के आदिकालीन 'पृथ्वीराज - रासौ' तथा ' सन्देश - रासक' में भी किया गया है। रासौ में आर्या छन्द का भी प्रयोग हुआ है। किन्तु, आदिकाल के उपरांत इन दोनों छन्दों का प्रयोग नहीं मिलता। 'दोहा' जहाँ तुक-युक्त और हस्वांत होता है, वहाँ 'गाहा' तुक - हीन और दीर्घान्त होता
1
1
मुक्तक रूप में दोहे का प्रयोग सूर आदि कृष्ण-भक्त कवियों में भी मिलता है । परन्तु, उन रसिक-भक्त-कवियों की संगीत-प्रियता तथा कला-कल्पना की स्वच्छंदता ने उसे पृथक काव्यरूप के सौजन्य से मंडित किया है जिसे 'पद - काव्य-रूप' कहा गया है और जो गीत-काव्य की परंपरा का ही परवर्ती विकास है। वस्तुतः पद कोई छन्द नहीं है अथ च, उसके विधान में अनेक छन्दों का प्रयोग अपने ढंग भक्त-कवियों कर डाला । इसी से इसके रूप-विधान में जहाँ-तहाँ भिन्नता के दर्शन होते हैं । यथा -