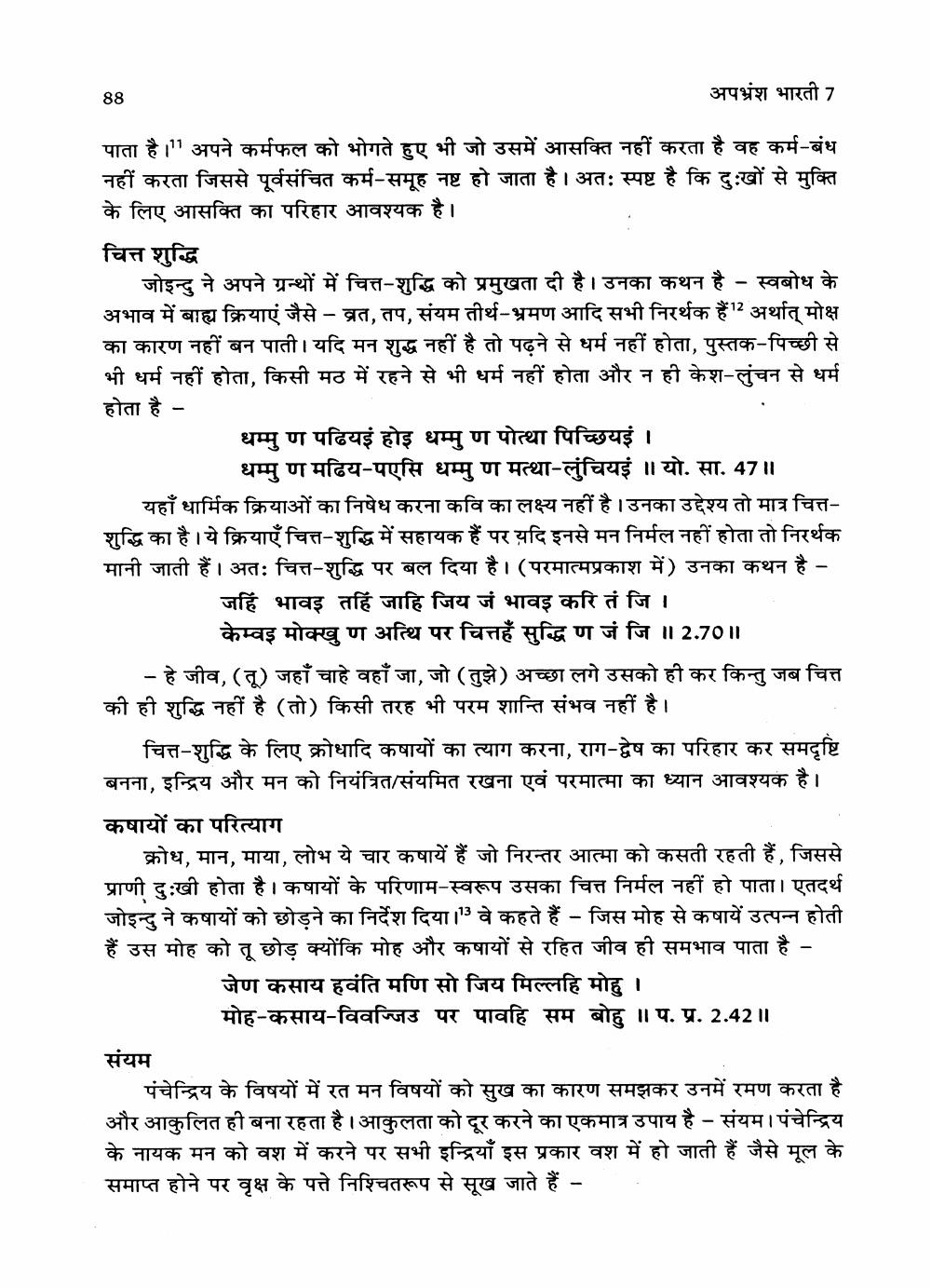________________
88
अपभ्रंश भारती7
पाता है। अपने कर्मफल को भोगते हुए भी जो उसमें आसक्ति नहीं करता है वह कर्म-बंध नहीं करता जिससे पूर्वसंचित कर्म-समूह नष्ट हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि दुःखों से मुक्ति के लिए आसक्ति का परिहार आवश्यक है। चित्त शुद्धि
जोइन्दु ने अपने ग्रन्थों में चित्त-शुद्धि को प्रमुखता दी है। उनका कथन है - स्वबोध के अभाव में बाह्य क्रियाएं जैसे - व्रत, तप, संयम तीर्थ-भ्रमण आदि सभी निरर्थक हैं12 अर्थात् मोक्ष का कारण नहीं बन पाती। यदि मन शुद्ध नहीं है तो पढ़ने से धर्म नहीं होता, पुस्तक-पिच्छी से भी धर्म नहीं होता, किसी मठ में रहने से भी धर्म नहीं होता और न ही केश-लुंचन से धर्म होता है -
धम्मु ण पढियइं होइ धम्मु ण पोत्था पिच्छियई ।
धम्मु ण मढिय-पएसि धम्मु ण मत्था-लुंचियइं ॥ यो. सा. 47॥ यहाँ धार्मिक क्रियाओं का निषेध करना कवि का लक्ष्य नहीं है। उनका उद्देश्य तो मात्र चित्तशुद्धि का है। ये क्रियाएँ चित्त-शुद्धि में सहायक हैं पर यदि इनसे मन निर्मल नहीं होता तो निरर्थक मानी जाती हैं। अत: चित्त-शुद्धि पर बल दिया है। (परमात्मप्रकाश में) उनका कथन है -
जहिं भावइ तहिं जाहि जिय जं भावइ करि तं जि ।
केम्वइ मोक्खु ण अत्थि पर चित्तहँ सुद्धि ण जं जि ॥ 2.70॥ - हे जीव, (तू) जहाँ चाहे वहाँ जा, जो (तुझे) अच्छा लगे उसको ही कर किन्तु जब चित्त की ही शुद्धि नहीं है (तो) किसी तरह भी परम शान्ति संभव नहीं है।
चित्त-शुद्धि के लिए क्रोधादि कषायों का त्याग करना, राग-द्वेष का परिहार कर समदृष्टि बनना, इन्द्रिय और मन को नियंत्रित/संयमित रखना एवं परमात्मा का ध्यान आवश्यक है। कषायों का परित्याग
क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषायें हैं जो निरन्तर आत्मा को कसती रहती हैं, जिससे प्राणी दु:खी होता है। कषायों के परिणाम-स्वरूप उसका चित्त निर्मल नहीं हो पाता। एतदर्थ जोइन्दु ने कषायों को छोड़ने का निर्देश दिया। वे कहते हैं - जिस मोह से कषायें उत्पन्न होती हैं उस मोह को तू छोड़ क्योंकि मोह और कषायों से रहित जीव ही समभाव पाता है -
जेण कसाय हवंति मणि सो जिय मिल्लहि मोहु ।
मोह-कसाय-विवज्जिउ पर पावहि सम बोहु ॥ प. प्र. 2.42॥ संयम ___पंचेन्द्रिय के विषयों में रत मन विषयों को सुख का कारण समझकर उनमें रमण करता है
और आकुलित ही बना रहता है । आकुलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है - संयम। पंचेन्द्रिय के नायक मन को वश में करने पर सभी इन्द्रियाँ इस प्रकार वश में हो जाती हैं जैसे मूल के समाप्त होने पर वृक्ष के पत्ते निश्चितरूप से सूख जाते हैं -