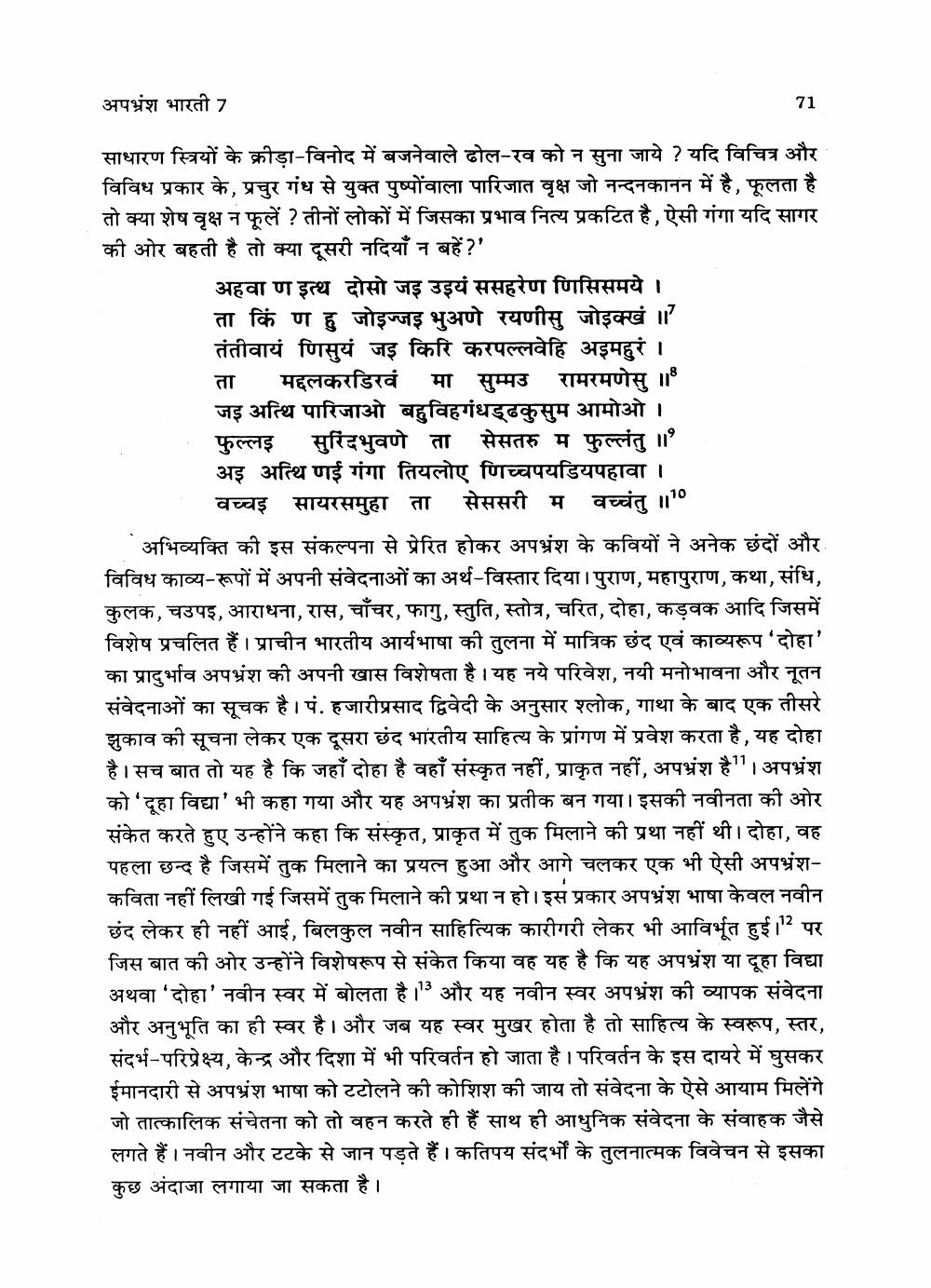________________
अपभ्रंश भारती 7
71
साधारण स्त्रियों के क्रीड़ा-विनोद में बजनेवाले ढोल-रव को न सुना जाये ? यदि विचित्र और विविध प्रकार के, प्रचुर गंध से युक्त पुष्पोंवाला पारिजात वृक्ष जो नन्दनकानन में है, फूलता है तो क्या शेष वृक्ष न फूलें ? तीनों लोकों में जिसका प्रभाव नित्य प्रकटित है, ऐसी गंगा यदि सागर की ओर बहती है तो क्या दूसरी नदियाँ न बहें?'
अहवा ण इत्थ दोसो जइ उइयं ससहरेण णिसिसमये । ता किं ण हु जोइज्जइ भुअणे रयणीसु जोइक्खं ।' तंतीवायं णिसुयं जइ किरि करपल्लवेहि अइमहुरं । ता मद्दलकरडिरवं मा सुम्मउ रामरमणेसु ॥ जइ अस्थि पारिजाओ बहुविहगंधड्ढकुसुम आमोओ। फुल्लइ सुरिंदभुवणे ता सेसतरु म फुल्लंतु ॥" अइ अस्थि णई गंगा तियलोए णिच्चपयडियपहावा ।
वच्चइ सायरसमुहा ता सेससरी म वच्चंतु ॥० अभिव्यक्ति की इस संकल्पना से प्रेरित होकर अपभ्रंश के कवियों ने अनेक छंदों और विविध काव्य-रूपों में अपनी संवेदनाओं का अर्थ-विस्तार दिया। पुराण, महापुराण, कथा, संधि, कुलक, चउपइ, आराधना, रास, चाँचर, फागु, स्तुति, स्तोत्र, चरित, दोहा, कड़वक आदि जिसमें विशेष प्रचलित हैं। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा की तुलना में मात्रिक छंद एवं काव्यरूप 'दोहा' का प्रादुर्भाव अपभ्रंश की अपनी खास विशेषता है। यह नये परिवेश, नयी मनोभावना और नूतन संवेदनाओं का सूचक है। पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्लोक, गाथा के बाद एक तीसरे झुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छंद भारतीय साहित्य के प्रांगण में प्रवेश करता है, यह दोहा है। सच बात तो यह है कि जहाँ दोहा है वहाँ संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, अपभ्रंश है । अपभ्रंश को 'दहा विद्या' भी कहा गया और यह अपभ्रंश का प्रतीक बन गया। इसकी नवीनता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत, प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा, वह पहला छन्द है जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चलकर एक भी ऐसी अपभ्रंशकविता नहीं लिखी गई जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा केवल नवीन छंद लेकर ही नहीं आई, बिलकुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर भी आविर्भूत हुई। पर जिस बात की ओर उन्होंने विशेषरूप से संकेत किया वह यह है कि यह अपभ्रंश या दूहा विद्या अथवा 'दोहा' नवीन स्वर में बोलता है। और यह नवीन स्वर अपभ्रंश की व्यापक संवेदना और अनुभूति का ही स्वर है। और जब यह स्वर मुखर होता है तो साहित्य के स्वरूप, स्तर, संदर्भ-परिप्रेक्ष्य, केन्द्र और दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के इस दायरे में घुसकर ईमानदारी से अपभ्रंश भाषा को टटोलने की कोशिश की जाय तो संवेदना के ऐसे आयाम मिलेंगे जो तात्कालिक संचेतना को तो वहन करते ही हैं साथ ही आधुनिक संवेदना के संवाहक जैसे लगते हैं। नवीन और टटके से जान पड़ते हैं । कतिपय संदर्भो के तुलनात्मक विवेचन से इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है।