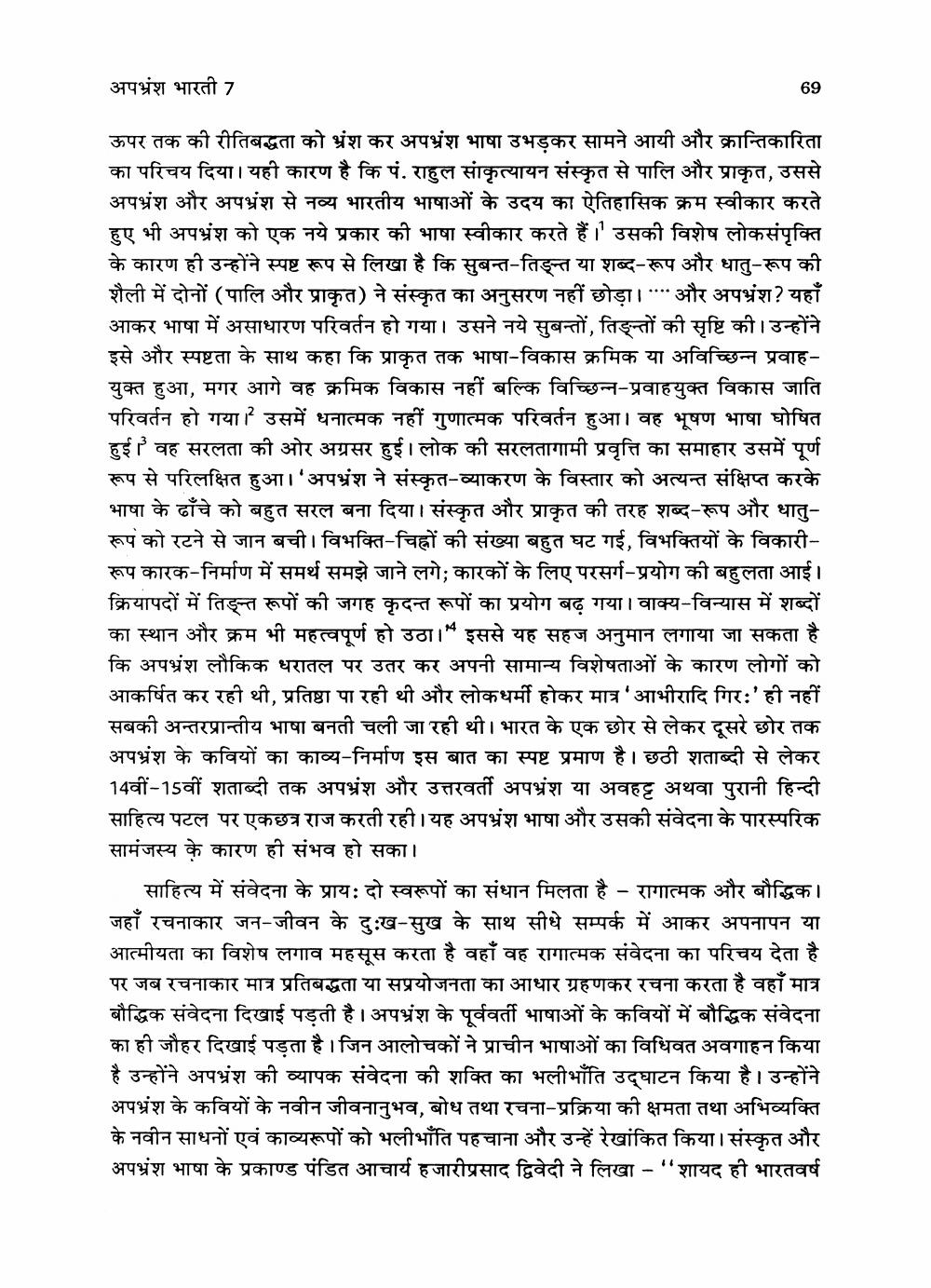________________
अपभ्रंश भारती 7
ऊपर तक की रीतिबद्धता को भ्रंश कर अपभ्रंश भाषा उभड़कर सामने आयी और क्रान्तिकारिता का परिचय दिया। यही कारण है कि पं. राहुल सांकृत्यायन संस्कृत से पालि और प्राकृत, उससे अपभ्रंश और अपभ्रंश से नव्य भारतीय भाषाओं के उदय का ऐतिहासिक क्रम स्वीकार करते हुए भी अपभ्रंश को एक नये प्रकार की भाषा स्वीकार करते हैं।' उसकी विशेष लोकसंपृक्ति के कारण ही उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबन्त - तिङ्न्त या शब्द-रूप और धातु रूप की शैली में दोनों (पालि और प्राकृत) ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा। और अपभ्रंश ? यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नये सुबन्तों, तिङ्न्तों की सृष्टि की। उन्होंने इसे और स्पष्टता के साथ कहा कि प्राकृत तक भाषा-विकास क्रमिक या अविच्छिन्न प्रवाहयुक्त हुआ, मगर आगे वह क्रमिक विकास नहीं बल्कि विच्छिन्न- प्रवाहयुक्त विकास जाति परिवर्तन हो गया। उसमें धनात्मक नहीं गुणात्मक परिवर्तन हुआ। वह भूषण भाषा घोषित हुई। वह सरलता की ओर अग्रसर हुई । लोक की सरलतागामी प्रवृत्ति का समाहार उसमें पूर्ण रूप से परिलक्षित हुआ । 'अपभ्रंश ने संस्कृत-व्याकरण के विस्तार को अत्यन्त संक्षिप्त करके भाषा के ढाँचे को बहुत सरल बना दिया। संस्कृत और प्राकृत की तरह शब्द-रूप और धातुरूपं को रटने से जान बची। विभक्ति-चिह्नों की संख्या बहुत घट गई, विभक्तियों के विकारीरूप कारक-निर्माण में समर्थ समझे जाने लगे; कारकों के लिए परसर्ग-प्रयोग की बहुलता आई । क्रियापदों में तिङ्न्त रूपों की जगह कृदन्त रूपों का प्रयोग बढ़ गया । वाक्य विन्यास में शब्दों का स्थान और क्रम भी महत्वपूर्ण हो उठा। इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश लौकिक धरातल पर उतर कर अपनी सामान्य विशेषताओं के कारण लोगों को आकर्षित कर रही थी, प्रतिष्ठा पा रही थी और लोकधर्मी होकर मात्र 'आभीरादि गिरः' ही नहीं सबकी अन्तरप्रान्तीय भाषा बनती चली जा रही थी। भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपभ्रंश के कवियों का काव्य-निर्माण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। छठी शताब्दी से लेकर 14वीं - 15वीं शताब्दी तक अपभ्रंश और उत्तरवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट अथवा पुरानी हिन्दी साहित्य पटल पर एकछत्र राज करती रही । यह अपभ्रंश भाषा और उसकी संवेदना के पारस्परिक सामंजस्य के कारण ही संभव हो सका ।
69
-
साहित्य में संवेदना के प्रायः दो स्वरूपों का संधान मिलता है रागात्मक और बौद्धिक । जहाँ रचनाकार जन-जीवन के दुःख-सुख के साथ सीधे सम्पर्क में आकर अपनापन या आत्मीयता का विशेष लगाव महसूस करता है वहाँ वह रागात्मक संवेदना का परिचय देता है पर जब रचनाकार मात्र प्रतिबद्धता या सप्रयोजनता का आधार ग्रहणकर रचना करता है वहाँ मात्र बौद्धिक संवेदना दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश के पूर्ववर्ती भाषाओं के कवियों में बौद्धिक संवेदना काही जौहर दिखाई पड़ता है। जिन आलोचकों ने प्राचीन भाषाओं का विधिवत अवगाहन किया है उन्होंने अपभ्रंश की व्यापक संवेदना की शक्ति का भलीभाँति उद्घाटन किया है। उन्होंने अपभ्रंश के कवियों के नवीन जीवनानुभव, बोध तथा रचना-प्रक्रिया की क्षमता तथा अभिव्यक्ति के नवीन साधनों एवं काव्यरूपों को भलीभाँति पहचाना और उन्हें रेखांकित किया। संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के प्रकाण्ड पंडित आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा
"
'शायद ही भारतवर्ष
-