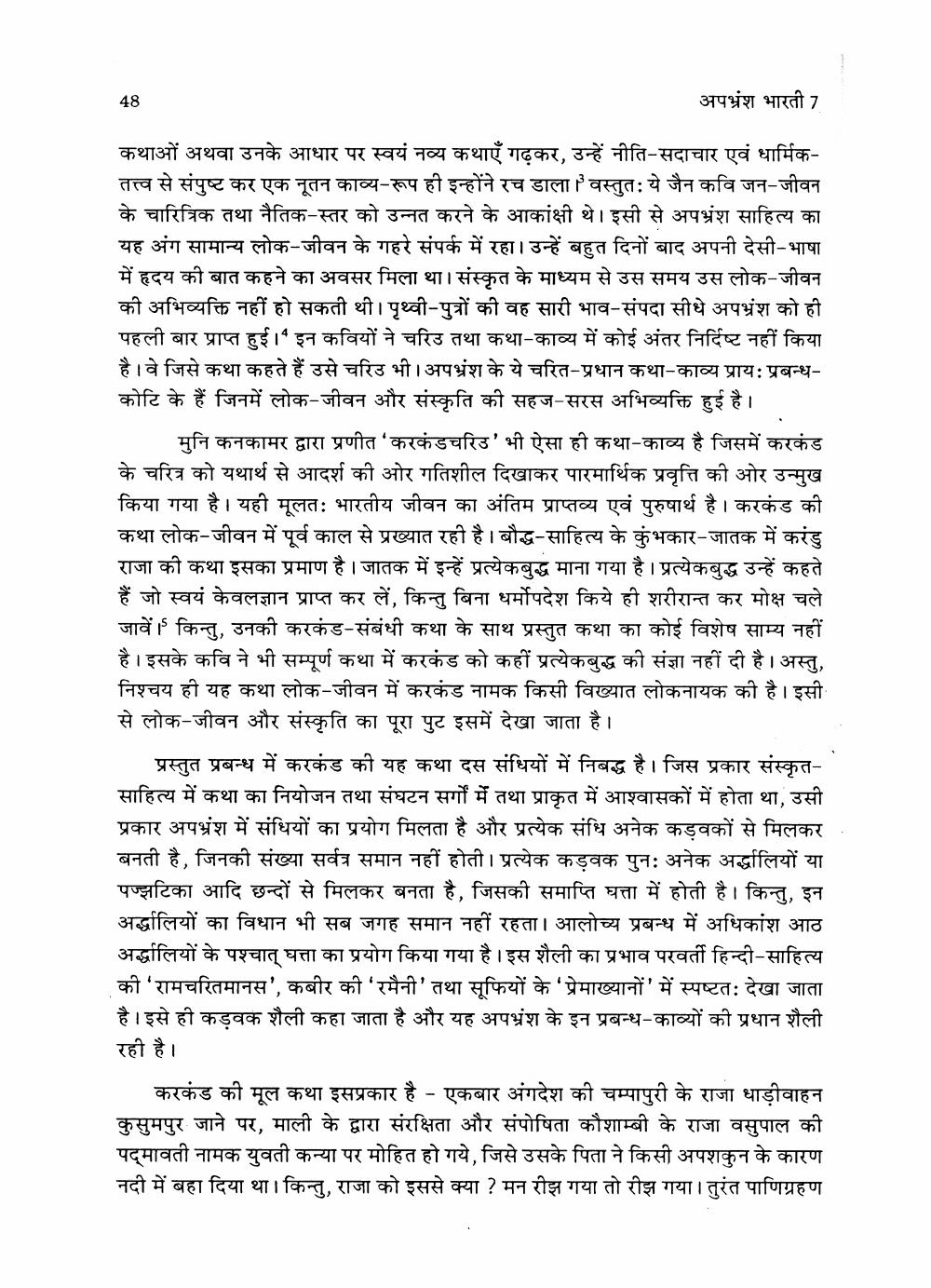________________
48
अपभ्रंश भारती7
कथाओं अथवा उनके आधार पर स्वयं नव्य कथाएँ गढ़कर, उन्हें नीति-सदाचार एवं धार्मिकतत्त्व से संपुष्ट कर एक नूतन काव्य-रूप ही इन्होंने रच डाला। वस्तुत: ये जैन कवि जन-जीवन के चारित्रिक तथा नैतिक-स्तर को उन्नत करने के आकांक्षी थे। इसी से अपभ्रंश साहित्य का यह अंग सामान्य लोक-जीवन के गहरे संपर्क में रहा। उन्हें बहुत दिनों बाद अपनी देसी-भाषा में हृदय की बात कहने का अवसर मिला था। संस्कृत के माध्यम से उस समय उस लोक-जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। पृथ्वी-पुत्रों की वह सारी भाव-संपदा सीधे अपभ्रंश को ही पहली बार प्राप्त हुई। इन कवियों ने चरिउ तथा कथा-काव्य में कोई अंतर निर्दिष्ट नहीं किया है। वे जिसे कथा कहते हैं उसे चरिउ भी। अपभ्रंश के ये चरित-प्रधान कथा-काव्य प्राय: प्रबन्धकोटि के हैं जिनमें लोक-जीवन और संस्कृति की सहज-सरस अभिव्यक्ति हुई है।
मुनि कनकामर द्वारा प्रणीत 'करकंडचरिउ' भी ऐसा ही कथा-काव्य है जिसमें करकंड के चरित्र को यथार्थ से आदर्श की ओर गतिशील दिखाकर पारमार्थिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख किया गया है। यही मूलतः भारतीय जीवन का अंतिम प्राप्तव्य एवं पुरुषार्थ है। करकंड की कथा लोक-जीवन में पूर्व काल से प्रख्यात रही है । बौद्ध-साहित्य के कुंभकार-जातक में करंडु राजा की कथा इसका प्रमाण है । जातक में इन्हें प्रत्येकबुद्ध माना गया है। प्रत्येकबुद्ध उन्हें कहते हैं जो स्वयं केवलज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु बिना धर्मोपदेश किये ही शरीरान्त कर मोक्ष चले जावें। किन्तु, उनकी करकंड-संबंधी कथा के साथ प्रस्तुत कथा का कोई विशेष साम्य नहीं है। इसके कवि ने भी सम्पूर्ण कथा में करकंड को कहीं प्रत्येकबुद्ध की संज्ञा नहीं दी है। अस्तु, निश्चय ही यह कथा लोक-जीवन में करकंड नामक किसी विख्यात लोकनायक की है। इसी से लोक-जीवन और संस्कृति का पूरा पुट इसमें देखा जाता है।
प्रस्तुत प्रबन्ध में करकंड की यह कथा दस संधियों में निबद्ध है। जिस प्रकार संस्कृतसाहित्य में कथा का नियोजन तथा संघटन सर्गों में तथा प्राकृत में आश्वासकों में होता था, उसी प्रकार अपभ्रंश में संधियों का प्रयोग मिलता है और प्रत्येक संधि अनेक कड़वकों से मिलकर बनती है, जिनकी संख्या सर्वत्र समान नहीं होती। प्रत्येक कड़वक पुनः अनेक अर्धालियों या पज्झटिका आदि छन्दों से मिलकर बनता है, जिसकी समाप्ति घत्ता में होती है। किन्तु, इन अर्धालियों का विधान भी सब जगह समान नहीं रहता। आलोच्य प्रबन्ध में अधिकांश आठ अर्धालियों के पश्चात् घत्ता का प्रयोग किया गया है । इस शैली का प्रभाव परवर्ती हिन्दी-साहित्य की 'रामचरितमानस', कबीर की 'रमैनी' तथा सूफियों के 'प्रेमाख्यानों' में स्पष्टतः देखा जाता है। इसे ही कड़वक शैली कहा जाता है और यह अपभ्रंश के इन प्रबन्ध-काव्यों की प्रधान शैली रही है।
करकंड की मूल कथा इसप्रकार है - एकबार अंगदेश की चम्पापुरी के राजा धाड़ीवाहन कुसुमपुर जाने पर, माली के द्वारा संरक्षिता और संपोषिता कौशाम्बी के राजा वसुपाल की पद्मावती नामक युवती कन्या पर मोहित हो गये, जिसे उसके पिता ने किसी अपशकुन के कारण नदी में बहा दिया था। किन्तु, राजा को इससे क्या ? मन रीझ गया तो रीझ गया। तुरंत पाणिग्रहण