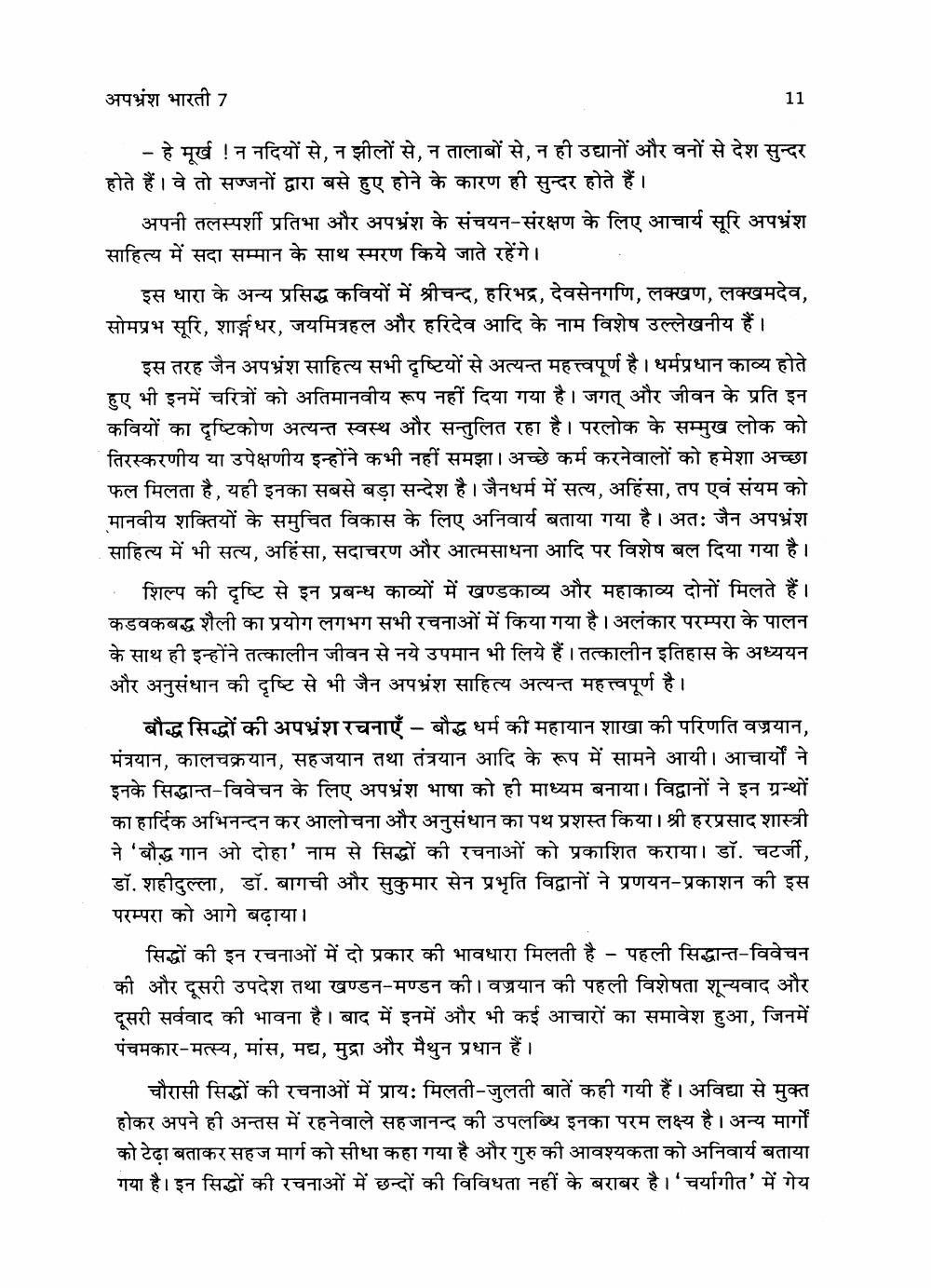________________
अपभ्रंश भारती 7
11
- हे मूर्ख ! न नदियों से, न झीलों से, न तालाबों से, न ही उद्यानों और वनों से देश सुन्दर होते हैं। वे तो सज्जनों द्वारा बसे हुए होने के कारण ही सुन्दर होते हैं।
अपनी तलस्पर्शी प्रतिभा और अपभ्रंश के संचयन-संरक्षण के लिए आचार्य सूरि अपभ्रंश साहित्य में सदा सम्मान के साथ स्मरण किये जाते रहेंगे।
इस धारा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में श्रीचन्द, हरिभद्र, देवसेनगणि, लक्खण, लक्खमदेव, सोमप्रभ सूरि, शार्ङ्गधर, जयमित्रहल और हरिदेव आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ___ इस तरह जैन अपभ्रंश साहित्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। धर्मप्रधान काव्य होते हुए भी इनमें चरित्रों को अतिमानवीय रूप नहीं दिया गया है। जगत् और जीवन के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण अत्यन्त स्वस्थ और सन्तुलित रहा है। परलोक के सम्मुख लोक को तिरस्करणीय या उपेक्षणीय इन्होंने कभी नहीं समझा। अच्छे कर्म करनेवालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है, यही इनका सबसे बड़ा सन्देश है। जैनधर्म में सत्य, अहिंसा, तप एवं संयम को मानवीय शक्तियों के समुचित विकास के लिए अनिवार्य बताया गया है। अतः जैन अपभ्रंश साहित्य में भी सत्य, अहिंसा, सदाचरण और आत्मसाधना आदि पर विशेष बल दिया गया है। . शिल्प की दृष्टि से इन प्रबन्ध काव्यों में खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों मिलते हैं। कडवकबद्ध शैली का प्रयोग लगभग सभी रचनाओं में किया गया है। अलंकार परम्परा के पालन के साथ ही इन्होंने तत्कालीन जीवन से नये उपमान भी लिये हैं । तत्कालीन इतिहास के अध्ययन और अनुसंधान की दृष्टि से भी जैन अपभ्रंश साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
बौद्ध सिद्धों की अपभ्रंश रचनाएँ - बौद्ध धर्म की महायान शाखा की परिणति वज्रयान, मंत्रयान, कालचक्रयान, सहजयान तथा तंत्रयान आदि के रूप में सामने आयी। आचार्यों ने इनके सिद्धान्त-विवेचन के लिए अपभ्रंश भाषा को ही माध्यम बनाया। विद्वानों ने इन ग्रन्थों का हार्दिक अभिनन्दन कर आलोचना और अनुसंधान का पथ प्रशस्त किया। श्री हरप्रसाद शास्त्री ने 'बौद्ध गान ओ दोहा' नाम से सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित कराया। डॉ. चटर्जी, डॉ. शहीदुल्ला, डॉ. बागची और सुकुमार सेन प्रभृति विद्वानों ने प्रणयन-प्रकाशन की इस परम्परा को आगे बढ़ाया।
सिद्धों की इन रचनाओं में दो प्रकार की भावधारा मिलती है - पहली सिद्धान्त-विवेचन की और दूसरी उपदेश तथा खण्डन-मण्डन की। वज्रयान की पहली विशेषता शून्यवाद और दूसरी सर्ववाद की भावना है। बाद में इनमें और भी कई आचारों का समावेश हुआ, जिनमें पंचमकार-मत्स्य, मांस, मद्य, मुद्रा और मैथुन प्रधान हैं।
चौरासी सिद्धों की रचनाओं में प्रायः मिलती-जुलती बातें कही गयी हैं। अविद्या से मुक्त होकर अपने ही अन्तस में रहनेवाले सहजानन्द की उपलब्धि इनका परम लक्ष्य है। अन्य मार्गों को टेढ़ा बताकर सहज मार्ग को सीधा कहा गया है और गुरु की आवश्यकता को अनिवार्य बताया गया है। इन सिद्धों की रचनाओं में छन्दों की विविधता नहीं के बराबर है। 'चर्यागीत' में गेय