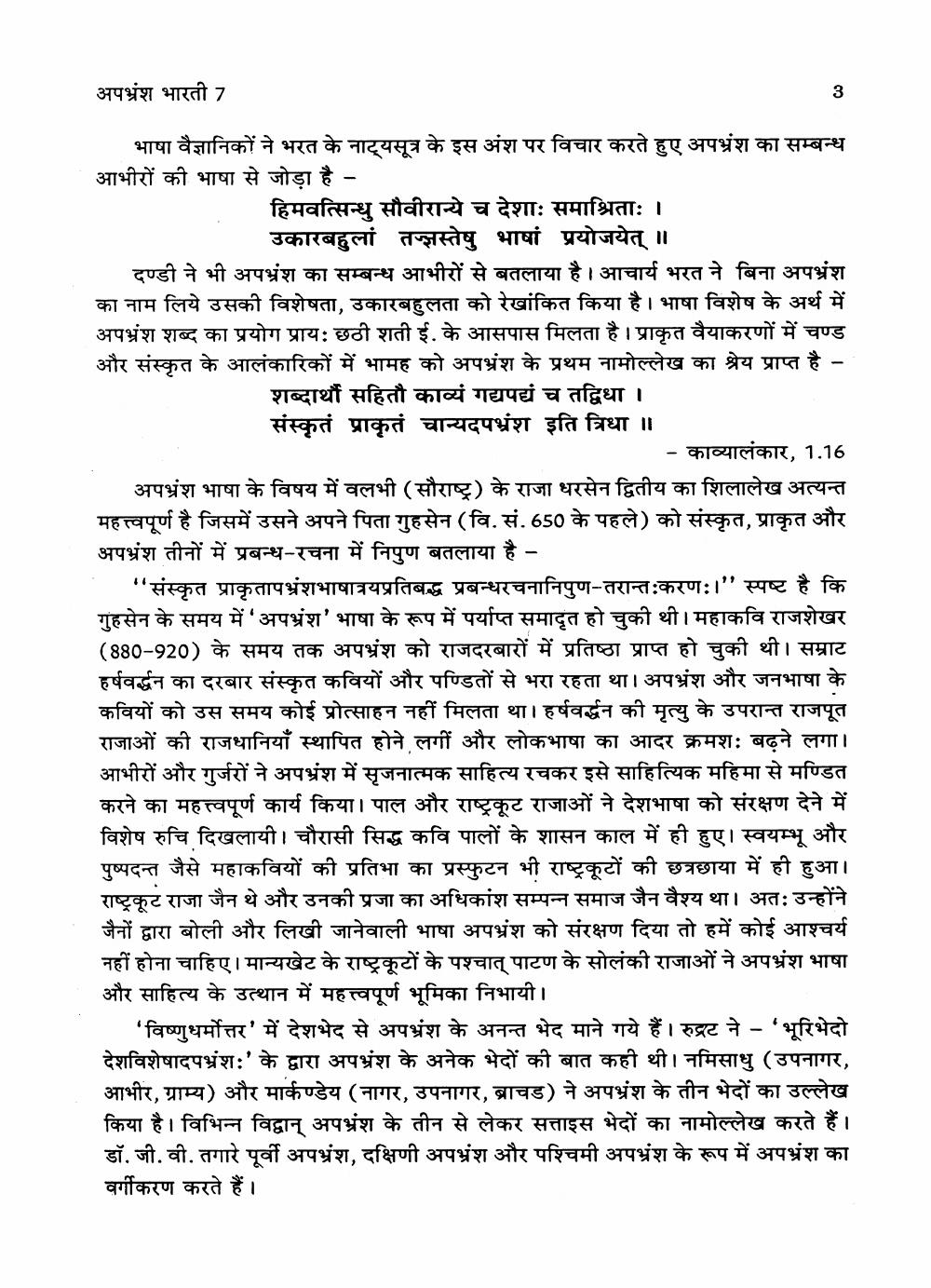________________
अपभ्रंश भारती 7
भाषा वैज्ञानिकों ने भरत के नाट्यसूत्र के इस अंश पर विचार करते हुए अपभ्रंश का सम्बन्ध आभीरों की भाषा से जोड़ा है -
हिमवत्सिन्धु सौवीरान्ये च देशाः समाश्रिताः ।
उकारबहुलां तज्ज्ञस्तेषु भाषां प्रयोजयेत् ॥ दण्डी ने भी अपभ्रंश का सम्बन्ध आभीरों से बतलाया है। आचार्य भरत ने बिना अपभ्रंश का नाम लिये उसकी विशेषता, उकारबहलता को रेखांकित किया है। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः छठी शती ई. के आसपास मिलता है। प्राकृत वैयाकरणों में चण्ड और संस्कृत के आलंकारिकों में भामह को अपभ्रंश के प्रथम नामोल्लेख का श्रेय प्राप्त है
शब्दार्थी सहितौ काव्यं गद्यपद्यं च तद्विधा । संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा ॥
- काव्यालंकार, 1.16 अपभ्रंश भाषा के विषय में वलभी (सौराष्ट्र) के राजा धरसेन द्वितीय का शिलालेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन (वि.सं. 650 के पहले) को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों में प्रबन्ध-रचना में निपुण बतलाया है - __ "संस्कृत प्राकृतापभ्रंशभाषात्रयप्रतिबद्ध प्रबन्धरचनानिपुण-तरान्तःकरणः।" स्पष्ट है कि गहसेन के समय में अपभ्रंश' भाषा के रूप में पर्याप्त समादत हो चकी थी। महाकवि राजशेखर (880-920) के समय तक अपभ्रंश को राजदरबारों में प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। सम्राट हर्षवर्द्धन का दरबार संस्कृत कवियों और पण्डितों से भरा रहता था। अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। हर्षवर्द्धन की मृत्यु के उपरान्त राजपूत राजाओं की राजधानियाँ स्थापित होने लगी और लोकभाषा का आदर क्रमशः बढ़ने लगा। आभीरों और गुर्जरों ने अपभ्रंश में सृजनात्मक साहित्य रचकर इसे साहित्यिक महिमा से मण्डित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने देशभाषा को संरक्षण देने में विशेष रुचि दिखलायी। चौरासी सिद्ध कवि पालों के शासन काल में ही हुए। स्वयम्भू और पुष्पदन्त जैसे महाकवियों की प्रतिभा का प्रस्फुटन भी राष्ट्रकूटों की छत्रछाया में ही हुआ। राष्ट्रकूट राजा जैन थे और उनकी प्रजा का अधिकांश सम्पन्न समाज जैन वैश्य था। अत: उन्होंने जैनों द्वारा बोली और लिखी जानेवाली भाषा अपभ्रंश को संरक्षण दिया तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के पश्चात् पाटण के सोलंकी राजाओं ने अपभ्रंश भाषा और साहित्य के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। ___ 'विष्णुधर्मोत्तर' में देशभेद से अपभ्रंश के अनन्त भेद माने गये हैं। रुद्रट ने – 'भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः' के द्वारा अपभ्रंश के अनेक भेदों की बात कही थी। नमिसाधु (उपनागर, आभीर, ग्राम्य) और मार्कण्डेय (नागर, उपनागर, ब्राचड) ने अपभ्रंश के तीन भेदों का उल्लेख किया है। विभिन्न विद्वान् अपभ्रंश के तीन से लेकर सत्ताइस भेदों का नामोल्लेख करते हैं। डॉ. जी. वी. तगारे पूर्वी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश के रूप में अपभ्रंश का वर्गीकरण करते हैं।