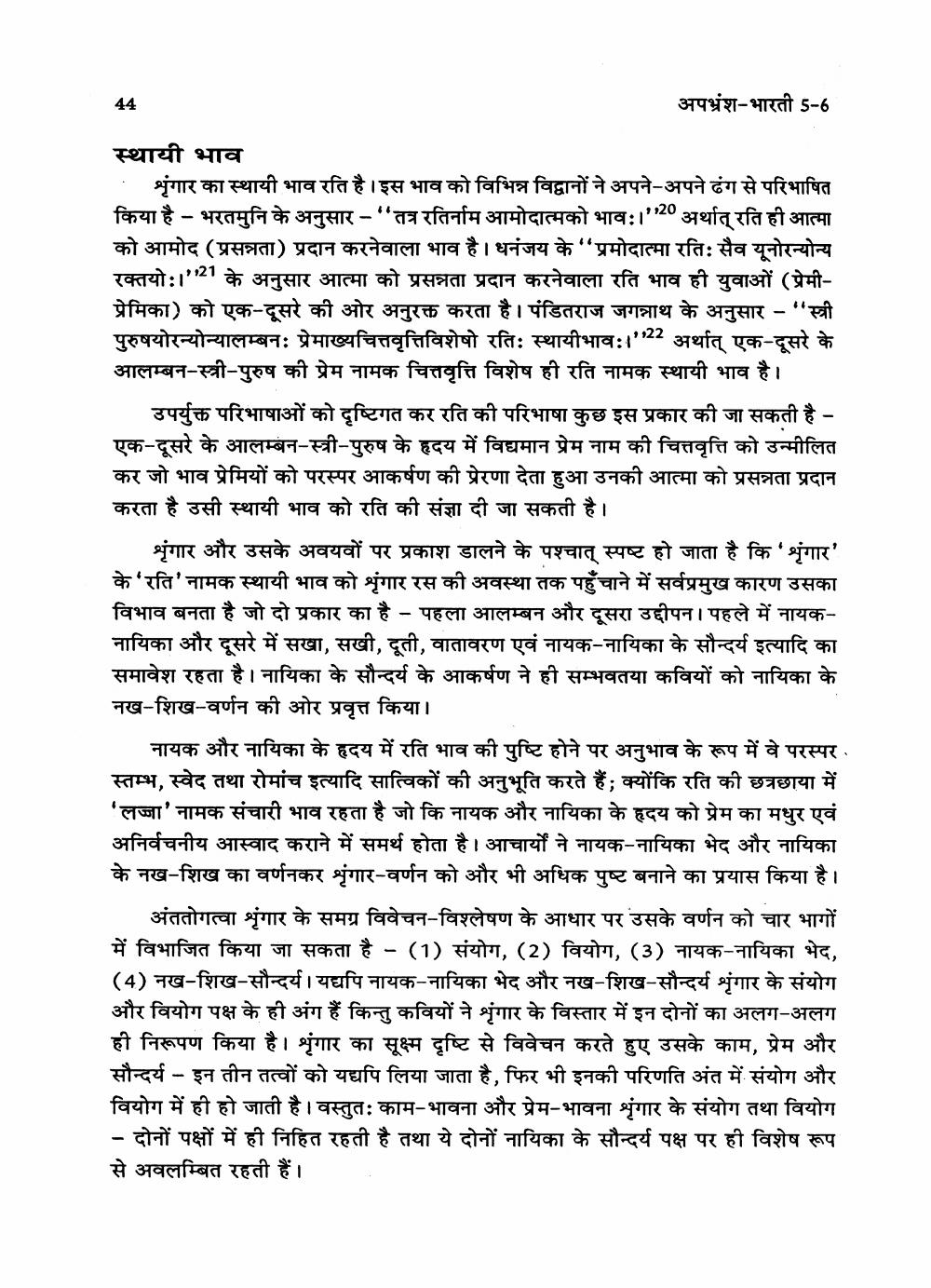________________
अपभ्रंश-भारती 5-6
स्थायी भाव - श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। इस भाव को विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है - भरतमुनि के अनुसार - "तत्र रति म आमोदात्मको भावः।।20 अर्थात् ति ही आत्मा को आमोद (प्रसन्नता) प्रदान करनेवाला भाव है। धनंजय के "प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्य रक्तयोः। 21 के अनुसार आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करनेवाला रति भाव ही युवाओं (प्रेमीप्रेमिका) को एक-दूसरे की ओर अनुरक्त करता है। पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार - "स्त्री पुरुषयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यचित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायीभावः। 22 अर्थात् एक-दूसरे के आलम्बन-स्त्री-पुरुष की प्रेम नामक चित्तवृत्ति विशेष ही रति नामक स्थायी भाव है। ___ उपर्युक्त परिभाषाओं को दृष्टिगत कर रति की परिभाषा कुछ इस प्रकार की जा सकती है - एक-दूसरे के आलम्बन-स्त्री-पुरुष के हृदय में विद्यमान प्रेम नाम की चित्तवृत्ति को उन्मीलित कर जो भाव प्रेमियों को परस्पर आकर्षण की प्रेरणा देता हुआ उनकी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करता है उसी स्थायी भाव को रति की संज्ञा दी जा सकती है।
श्रृंगार और उसके अवयवों पर प्रकाश डालने के पश्चात् स्पष्ट हो जाता है कि 'शृंगार' के 'रति' नामक स्थायी भाव को श्रृंगार रस की अवस्था तक पहुँचाने में सर्वप्रमुख कारण उसका विभाव बनता है जो दो प्रकार का है - पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन । पहले में नायकनायिका और दूसरे में सखा, सखी, दूती, वातावरण एवं नायक-नायिका के सौन्दर्य इत्यादि का समावेश रहता है। नायिका के सौन्दर्य के आकर्षण ने ही सम्भवतया कवियों को नायिका के नख-शिख-वर्णन की ओर प्रवृत्त किया।
नायक और नायिका के हृदय में रति भाव की पुष्टि होने पर अनुभाव के रूप में वे परस्पर . स्तम्भ, स्वेद तथा रोमांच इत्यादि सात्विकों की अनुभूति करते हैं; क्योंकि रति की छत्रछाया में 'लज्जा' नामक संचारी भाव रहता है जो कि नायक और नायिका के हृदय को प्रेम का मधुर एवं अनिर्वचनीय आस्वाद कराने में समर्थ होता है। आचार्यों ने नायक-नायिका भेद और नायिका के नख-शिख का वर्णनकर शृंगार-वर्णन को और भी अधिक पुष्ट बनाने का प्रयास किया है। ___ अंततोगत्वा श्रृंगार के समग्र विवेचन-विश्लेषण के आधार पर उसके वर्णन को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है - (1) संयोग, (2) वियोग, (3) नायक-नायिका भेद, (4) नख-शिख-सौन्दर्य । यद्यपि नायक-नायिका भेद और नख-शिख-सौन्दर्य श्रृंगार के संयोग
और वियोग पक्ष के ही अंग हैं किन्तु कवियों ने श्रृंगार के विस्तार में इन दोनों का अलग-अलग ही निरूपण किया है। श्रृंगार का सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करते हुए उसके काम, प्रेम और सौन्दर्य - इन तीन तत्वों को यद्यपि लिया जाता है, फिर भी इनकी परिणति अंत में संयोग और वियोग में ही हो जाती है। वस्तुतः काम-भावना और प्रेम-भावना श्रृंगार के संयोग तथा वियोग - दोनों पक्षों में ही निहित रहती है तथा ये दोनों नायिका के सौन्दर्य पक्ष पर ही विशेष रूप से अवलम्बित रहती हैं।