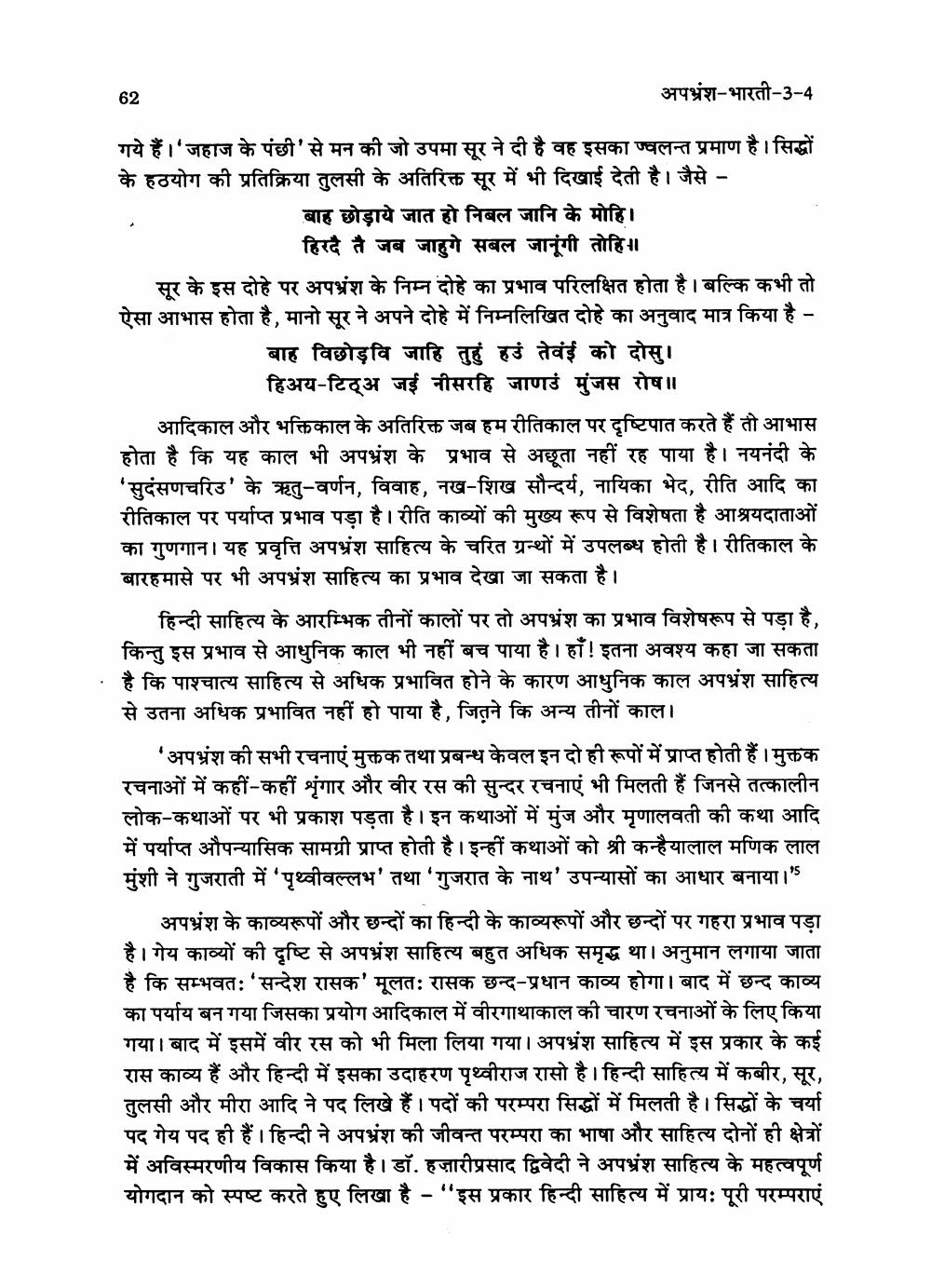________________
अपभ्रंश - भारती - 3-4
गये हैं।'जहाज के पंछी' से मन की जो उपमा सूर ने दी है वह इसका ज्वलन्त प्रमाण है। सिद्धों के हठयोग की प्रतिक्रिया तुलसी के अतिरिक्त सूर में भी दिखाई देती है । जैसे
62
बाह छोड़ाये जात हो निबल जानि के मोहि । हिरदै तै जब जाहुगे सबल जानूंगी तोहि ॥
-
सूर के इस दोहे पर अपभ्रंश के निम्न दोहे का प्रभाव परिलक्षित होता है। बल्कि कभी तो ऐसा आभास होता है, मानो सूर ने अपने दोहे में निम्नलिखित दोहे का अनुवाद मात्र किया है - बाह विछोड़वि जाहि तुहुं हउं तेवंई को दोसु । हिअय-टिट्अ जई नीसरहि जाणउं मुंजस रोष ॥
आदिकाल और भक्तिकाल के अतिरिक्त जब हम रीतिकाल पर दृष्टिपात करते हैं तो आभास होता है कि यह काल भी अपभ्रंश के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया है। नयनंदी के 'सुदंसणचरिउ' के ऋतु वर्णन, विवाह, नख-शिख सौन्दर्य, नायिका भेद, रीति आदि का रीतिकाल पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। रीति काव्यों की मुख्य रूप से विशेषता है आश्रयदाताओं का गुणगान। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश साहित्य के चरित ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। रीतिकाल के बारहमासे पर भी अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है।
हिन्दी साहित्य के आरम्भिक तीनों कालों पर तो अपभ्रंश का प्रभाव विशेषरूप से पड़ा है, किन्तु इस प्रभाव से आधुनिक काल भी नहीं बच पाया है। हाँ ! इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पाश्चात्य साहित्य से अधिक प्रभावित होने के कारण आधुनिक काल अपभ्रंश साहित्य से उतना अधिक प्रभावित नहीं हो पाया है, जितने कि अन्य तीनों काल ।
'अपभ्रंश की सभी रचनाएं मुक्तक तथा प्रबन्ध केवल इन दो ही रूपों में प्राप्त होती हैं। मुक्तक रचनाओं में कहीं-कहीं शृंगार और वीर रस की सुन्दर रचनाएं भी मिलती हैं जिनसे तत्कालीन लोक-कथाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इन कथाओं में मुंज और मृणालवती की कथा आदि में पर्याप्त औपन्यासिक सामग्री प्राप्त होती है। इन्हीं कथाओं को श्री कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी ने गुजराती में 'पृथ्वीवल्लभ' तथा 'गुजरात के नाथ' उपन्यासों का आधार बनाया।'
$5
अपभ्रंश के काव्यरूपों और छन्दों का हिन्दी के काव्यरूपों और छन्दों पर गहरा प्रभाव पड़ा है । गेय काव्यों की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य बहुत अधिक समृद्ध था। अनुमान लगाया जाता है कि सम्भवत: ‘सन्देश रासक' मूलतः रासक छन्द- प्रधान काव्य होगा। बाद में छन्द काव्य का पर्याय बन गया जिसका प्रयोग आदिकाल में वीरगाथाकाल की चारण रचनाओं के लिए किया गया। बाद में इसमें वीर रस को भी मिला लिया गया। अपभ्रंश साहित्य में इस प्रकार के कई रास काव्य हैं और हिन्दी में इसका उदाहरण पृथ्वीराज रासो है । हिन्दी साहित्य में कबीर, सूर, तुलसी और मीरा आदि ने पद लिखे हैं। पदों की परम्परा सिद्धों में मिलती है । सिद्धों के चर्या पद गेय पद ही हैं। हिन्दी ने अपभ्रंश की जीवन्त परम्परा का भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अविस्मरणीय विकास किया है। डॉ. हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करते हुए लिखा है। 'इस प्रकार हिन्दी साहित्य में प्रायः पूरी परम्पराएं
"