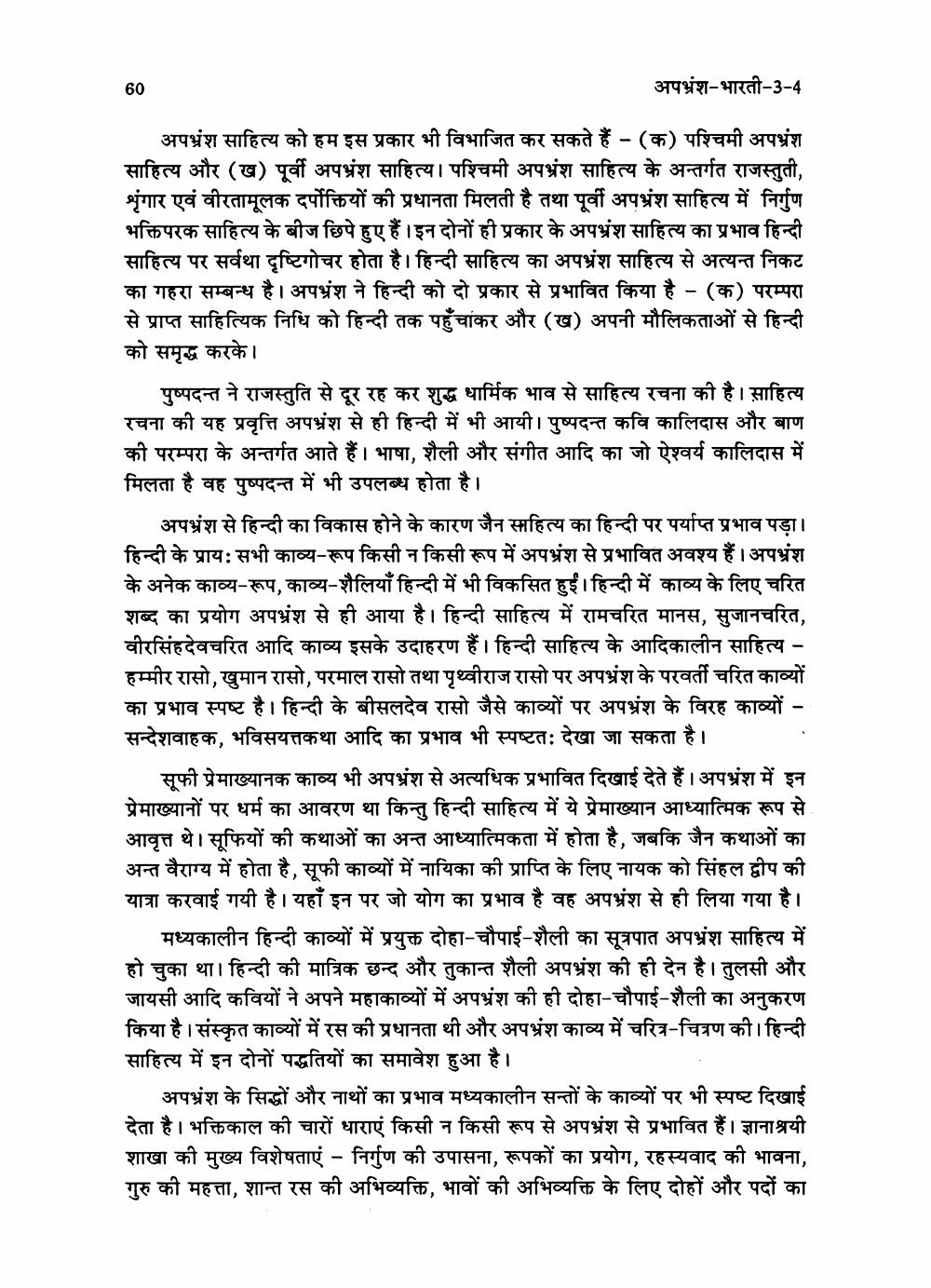________________
60
अपभ्रंश-भारती-3-4
__अपभ्रंश साहित्य को हम इस प्रकार भी विभाजित कर सकते हैं - (क) पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य और (ख) पूर्वी अपभ्रंश साहित्य। पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य के अन्तर्गत राजस्तुती, शृंगार एवं वीरतामूलक दर्पोक्तियों की प्रधानता मिलती है तथा पूर्वी अपभ्रंश साहित्य में निर्गुण भक्तिपरक साहित्य के बीज छिपे हुए हैं। इन दोनों ही प्रकार के अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर सर्वथा दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी साहित्य का अपभ्रंश साहित्य से अत्यन्त निकट का गहरा सम्बन्ध है। अपभ्रंश ने हिन्दी को दो प्रकार से प्रभावित किया है - (क) परम्परा से प्राप्त साहित्यिक निधि को हिन्दी तक पहुँचाकर और (ख) अपनी मौलिकताओं से हिन्दी को समृद्ध करके। ___ पुष्पदन्त ने राजस्तुति से दूर रह कर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की है। साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही हिन्दी में भी आयी। पुष्पदन्त कवि कालिदास और बाण
की परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। भाषा, शैली और संगीत आदि का जो ऐश्वर्य कालिदास में मिलता है वह पुष्पदन्त में भी उपलब्ध होता है।
अपभ्रंश से हिन्दी का विकास होने के कारण जैन साहित्य का हिन्दी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हिन्दी के प्रायः सभी काव्य-रूप किसी न किसी रूप में अपभ्रंश से प्रभावित अवश्य हैं। अपभ्रंश के अनेक काव्य-रूप, काव्य-शैलियाँ हिन्दी में भी विकसित हुई। हिन्दी में काव्य के लिए चरित शब्द का प्रयोग अपभ्रंश से ही आया है। हिन्दी साहित्य में रामचरित मानस, सुजानचरित, वीरसिंहदेवचरित आदि काव्य इसके उदाहरण हैं। हिन्दी साहित्य के आदिकालीन साहित्य - हम्मीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो तथा पृथ्वीराज रासो पर अपभ्रंश के परवर्ती चरित काव्यों का प्रभाव स्पष्ट है। हिन्दी के बीसलदेव रासो जैसे काव्यों पर अपभ्रंश के विरह काव्यों - सन्देशवाहक, भविसयत्तकथा आदि का प्रभाव भी स्पष्टतः देखा जा सकता है।
सूफी प्रेमाख्यानक काव्य भी अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। अपभ्रंश में इन प्रेमाख्यानों पर धर्म का आवरण था किन्तु हिन्दी साहित्य में ये प्रेमाख्यान आध्यात्मिक रूप से आवृत्त थे। सूफियों की कथाओं का अन्त आध्यात्मिकता में होता है, जबकि जैन कथाओं का अन्त वैराग्य में होता है, सूफी काव्यों में नायिका की प्राप्ति के लिए नायक को सिंहल द्वीप की यात्रा करवाई गयी है। यहाँ इन पर जो योग का प्रभाव है वह अपभ्रंश से ही लिया गया है। ___ मध्यकालीन हिन्दी काव्यों में प्रयुक्त दोहा-चौपाई-शैली का सूत्रपात अपभ्रंश साहित्य में हो चुका था। हिन्दी की मात्रिक छन्द और तुकान्त शैली अपभ्रंश की ही देन है। तुलसी और जायसी आदि कवियों ने अपने महाकाव्यों में अपभ्रंश की ही दोहा-चौपाई-शैली का अनुकरण किया है। संस्कृत काव्यों में रस की प्रधानता थी और अपभ्रंश काव्य में चरित्र-चित्रण की। हिन्दी साहित्य में इन दोनों पद्धतियों का समावेश हुआ है। ____ अपभ्रंश के सिद्धों और नाथों का प्रभाव मध्यकालीन सन्तों के काव्यों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। भक्तिकाल की चारों धाराएं किसी न किसी रूप से अपभ्रंश से प्रभावित हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा की मुख्य विशेषताएं - निर्गुण की उपासना, रूपकों का प्रयोग, रहस्यवाद की भावना, गुरु की महत्ता, शान्त रस की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति के लिए दोहों और पदों का