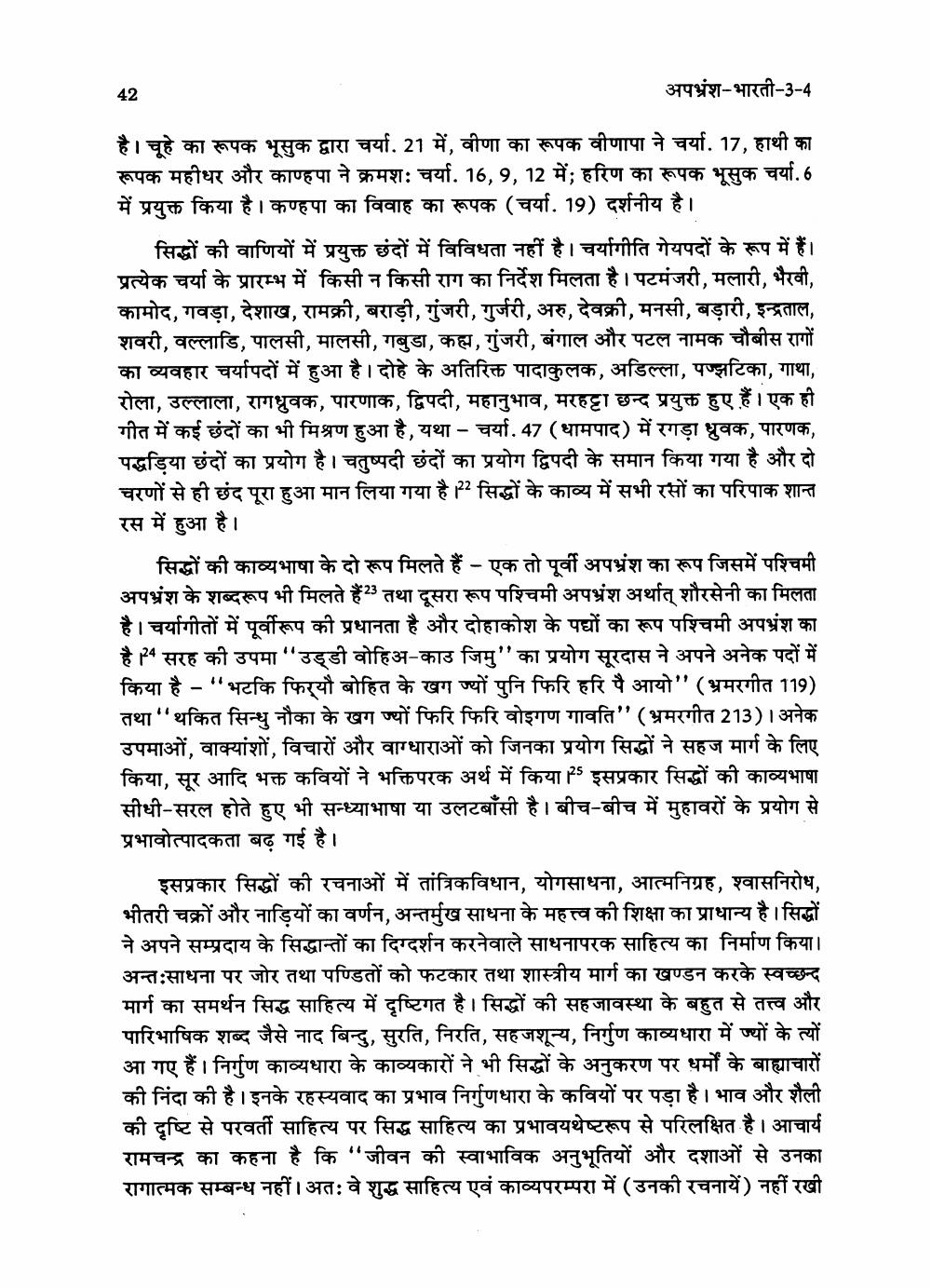________________
अपभ्रंश - भारती - 3-4
है। चूहे का रूपक भूसुक द्वारा चर्या. 21 में, वीणा का रूपक वीणापा ने चर्या. 17, हाथी का रूपक महीधर और काण्हपा ने क्रमशः चर्या. 16, 9, 12 में; हरिण का रूपक भूसुक चर्या. 6 में प्रयुक्त किया है। कण्हपा का विवाह का रूपक (चर्या. 19) दर्शनीय है ।
42
सिद्धों की वाणियों में प्रयुक्त छंदों में विविधता नहीं है। चर्यागीति गेयपदों के रूप में हैं। प्रत्येक चर्या के प्रारम्भ में किसी न किसी राग का निर्देश मिलता है। पटमंजरी, मलारी, भैरवी, कामोद, गवड़ा, देशाख, रामक्री, बराड़ी, गुंजरी, गुर्जरी, अरु, देवक्री, मनसी, बड़ारी, इन्द्रताल, शवरी, वल्लाडि, पालसी, मालसी, गबुडा, कल, गुंजरी, बंगाल और पटल नामक चौबीस रागों का व्यवहार चर्यापदों में हुआ है। दोहे के अतिरिक्त पादाकुलक, अडिल्ला, पज्झटिका, गाथा, रोला, उल्लाला रागध्रुवक, पारणाक, द्विपदी, महानुभाव, मरहट्टा छन्द प्रयुक्त हुए हैं। एक ही गीत में कई छंदों का भी मिश्रण हुआ है, यथा- चर्या. 47 (धामपाद) में रगड़ा ध्रुवक, पारणक, पद्धड़िया छंदों का प्रयोग है । चतुष्पदी छंदों का प्रयोग द्विपदी के समान किया गया है और दो चरणों से ही छंद पूरा हुआ मान लिया गया है। 22 सिद्धों के काव्य में सभी रसों का परिपाक शान्त रस में हुआ है 1
सिद्धों की काव्य भाषा के दो रूप मिलते हैं - एक तो पूर्वी अपभ्रंश का रूप जिसमें पश्चिमी अपभ्रंश के शब्दरूप भी मिलते हैं 23 तथा दूसरा रूप पश्चिमी अपभ्रंश अर्थात् शौरसेनी का मिलता है । चर्यागीतों में पूर्वी रूप की प्रधानता है और दोहाकोश के पद्यों का रूप पश्चिमी अपभ्रंश का है। 24 सरह की उपमा "उड्डी वोहिअ-काउ जिमु" का प्रयोग सूरदास ने अपने अनेक पदों में किया है - " भटकि फिर्यौ बोहित के खग ज्यों पुनि फिरि हरि पै आयो" (भ्रमरगीत 119 ) तथा" थकित सिन्धु नौका के खग ज्यों फिरि फिरि वोइगण गावति" (भ्रमरगीत 213 ) । अनेक उपमाओं, वाक्यांशों, विचारों और वाग्धाराओं को जिनका प्रयोग सिद्धों ने सहज मार्ग के लिए किया, सूर आदि भक्त कवियों ने भक्तिपरक अर्थ में किया।" इसप्रकार सिद्धों की काव्यभाषा सीधी-सरल होते हुए भी सन्ध्याभाषा या उलटबाँसी है। बीच-बीच में मुहावरों के प्रयोग से प्रभावोत्पादकता बढ़ गई है।
इसप्रकार सिद्धों की रचनाओं में तांत्रिकविधान, योगसाधना, आत्मनिग्रह, श्वासनिरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों का वर्णन, अन्तर्मुख साधना के महत्त्व की शिक्षा का प्राधान्य है। सिद्धों ने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन करनेवाले साधनापरक साहित्य का निर्माण किया। अन्तःसाधना पर जोर तथा पण्डितों को फटकार तथा शास्त्रीय मार्ग का खण्डन करके स्वच्छन्द मार्ग का समर्थन सिद्ध साहित्य में दृष्टिगत है । सिद्धों की सहजावस्था के बहुत से तत्त्व और पारिभाषिक शब्द जैसे नाद बिन्दु, सुरति, निरति, सहजशून्य, निर्गुण काव्यधारा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। निर्गुण काव्यधारा के काव्यकारों ने भी सिद्धों के अनुकरण पर धर्मों के बाह्याचारों की निंदा की है। इनके रहस्यवाद का प्रभाव निर्गुणधारा के कवियों पर पड़ा है। भाव और शैली की दृष्टि से परवर्ती साहित्य पर सिद्ध साहित्य का प्रभावयथेष्टरूप से परिलक्षित है। आचार्य रामचन्द्र का कहना है कि "जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका रागात्मक सम्बन्ध नहीं । अतः वे शुद्ध साहित्य एवं काव्यपरम्परा में (उनकी रचनायें) नहीं रखी