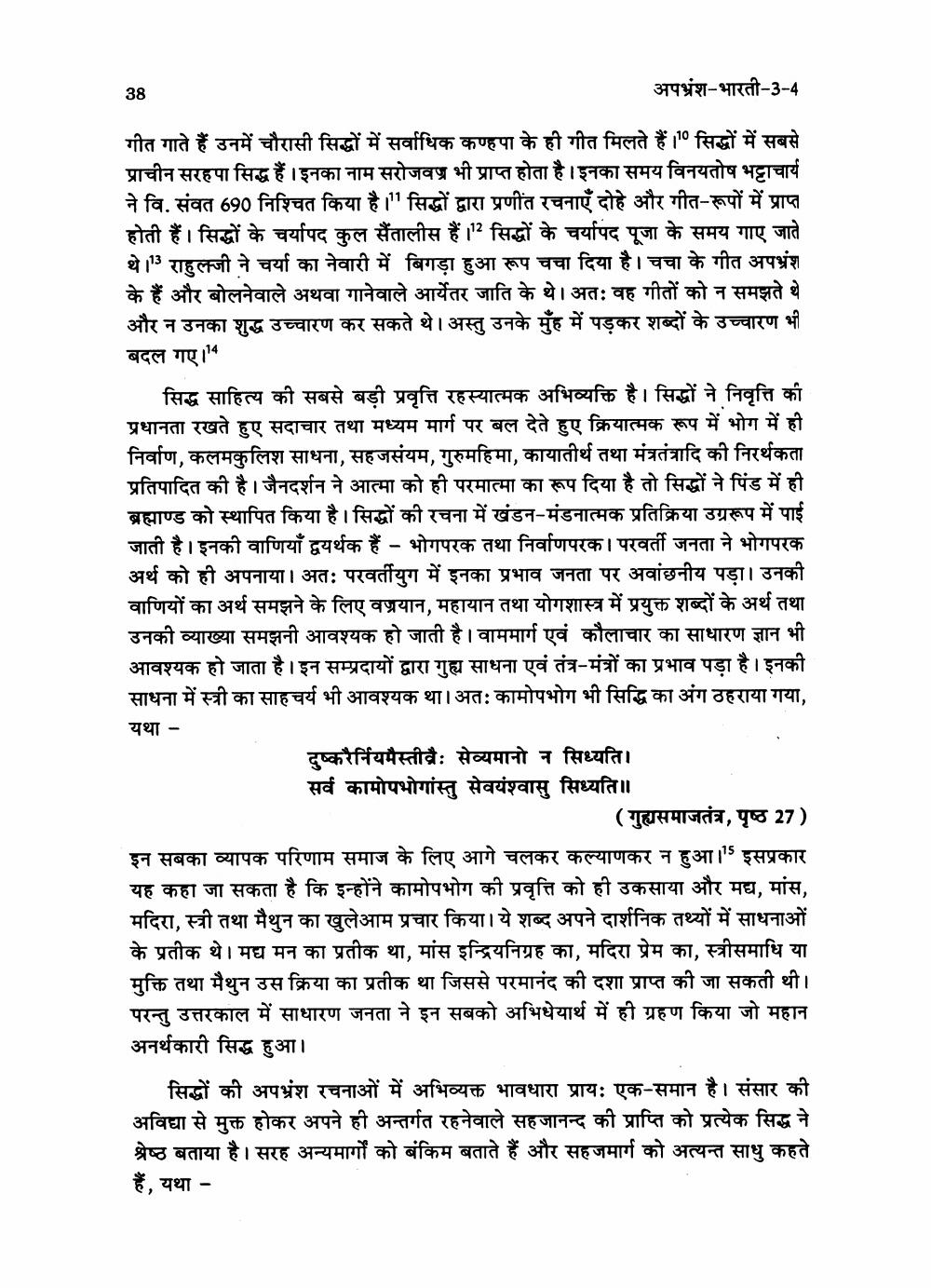________________
38
अपभ्रंश-भारती-3-4
गीत गाते हैं उनमें चौरासी सिद्धों में सर्वाधिक कण्हपा के ही गीत मिलते हैं। सिद्धों में सबसे प्राचीन सरहपा सिद्ध हैं। इनका नाम सरोजवन भी प्राप्त होता है। इनका समय विनयतोष भट्टाचार्य ने वि. संवत 690 निश्चित किया है।" सिद्धों द्वारा प्रणीत रचनाएँ दोहे और गीत-रूपों में प्राप्त होती हैं। सिद्धों के चर्यापद कुल सैंतालीस हैं। सिद्धों के चर्यापद पूजा के समय गाए जाते थे। राहुलजी ने चर्या का नेवारी में बिगड़ा हुआ रूप चचा दिया है। चचा के गीत अपभ्रंश के हैं और बोलनेवाले अथवा गानेवाले आर्येतर जाति के थे। अत: वह गीतों को न समझते थे और न उनका शुद्ध उच्चारण कर सकते थे। अस्तु उनके मुँह में पड़कर शब्दों के उच्चारण भी बदल गए।
सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है। सिद्धों ने निवृत्ति की प्रधानता रखते हुए सदाचार तथा मध्यम मार्ग पर बल देते हुए क्रियात्मक रूप में भोग में ही निर्वाण, कलमकुलिश साधना, सहजसंयम, गुरुमहिमा, कायातीर्थ तथा मंत्रतंत्रादि की निरर्थकता प्रतिपादित की है। जैनदर्शन ने आत्मा को ही परमात्मा का रूप दिया है तो सिद्धों ने पिंड में ही ब्रह्माण्ड को स्थापित किया है। सिद्धों की रचना में खंडन-मंडनात्मक प्रतिक्रिया उग्ररूप में पाई जाती है। इनकी वाणियाँ द्वयर्थक हैं - भोगपरक तथा निर्वाणपरक। परवर्ती जनता ने भोगपरक अर्थ को ही अपनाया। अतः परवर्तीयुग में इनका प्रभाव जनता पर अवांछनीय पड़ा। उनकी वाणियों का अर्थ समझने के लिए वज्रयान, महायान तथा योगशास्त्र में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ तथा उनकी व्याख्या समझनी आवश्यक हो जाती है। वाममार्ग एवं कौलाचार का साधारण ज्ञान भी आवश्यक हो जाता है। इन सम्प्रदायों द्वारा गुह्य साधना एवं तंत्र-मंत्रों का प्रभाव पड़ा है। इनकी साधना में स्त्री का साहचर्य भी आवश्यक था। अत: कामोपभोग भी सिद्धि का अंग ठहराया गया, यथा -
दुष्करैर्नियमैस्तीत्रैः सेव्यमानो न सिध्यति। सर्व कामोपभोगांस्तु सेवयंश्वासु सिध्यति॥
(गुह्यसमाजतंत्र, पृष्ठ 27) इन सबका व्यापक परिणाम समाज के लिए आगे चलकर कल्याणकर न हुआ। इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कामोपभोग की प्रवृत्ति को ही उकसाया और मद्य, मांस, मदिरा, स्त्री तथा मैथुन का खुलेआम प्रचार किया। ये शब्द अपने दार्शनिक तथ्यों में साधनाओं के प्रतीक थे। मध मन का प्रतीक था, मांस इन्द्रियनिग्रह का, मदिरा प्रेम का, स्त्रीसमाधि या मुक्ति तथा मैथुन उस क्रिया का प्रतीक था जिससे परमानंद की दशा प्राप्त की जा सकती थी। परन्तु उत्तरकाल में साधारण जनता ने इन सबको अभिधेयार्थ में ही ग्रहण किया जो महान अनर्थकारी सिद्ध हुआ।
सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं में अभिव्यक्त भावधारा प्रायः एक-समान है। संसार की अविद्या से मुक्त होकर अपने ही अन्तर्गत रहनेवाले सहजानन्द की प्राप्ति को प्रत्येक सिद्ध ने श्रेष्ठ बताया है। सरह अन्यमार्गों को बंकिम बताते हैं और सहजमार्ग को अत्यन्त साधु कहते हैं, यथा -