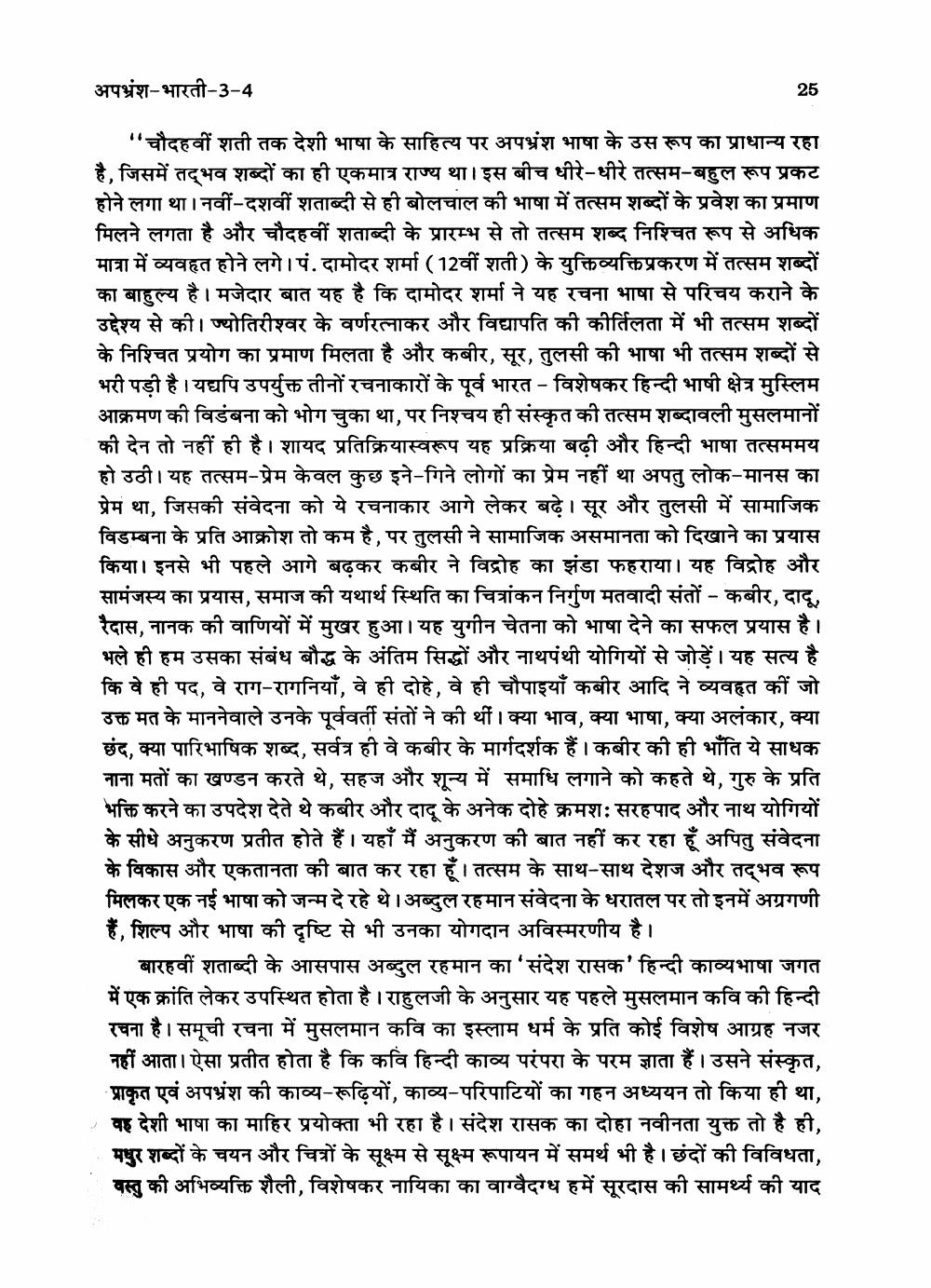________________
अपभ्रंश-भारती-3-4
25
"चौदहवीं शती तक देशी भाषा के साहित्य पर अपभ्रंश भाषा के उस रूप का प्राधान्य रहा है, जिसमें तद्भव शब्दों का ही एकमात्र राज्य था। इस बीच धीरे-धीरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। नवीं-दशवीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण मिलने लगता है और चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप से अधिक मात्रा में व्यवहृत होने लगे। पं.दामोदर शर्मा (12वीं शती) के युक्तिव्यक्तिप्रकरण में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। मजेदार बात यह है कि दामोदर शर्मा ने यह रचना भाषा से परिचय कराने के उद्देश्य से की। ज्योतिरीश्वर के वर्णरत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता में भी तत्सम शब्दों के निश्चित प्रयोग का प्रमाण मिलता है और कबीर, सूर, तुलसी की भाषा भी तत्सम शब्दों से भरी पड़ी है। यद्यपि उपर्युक्त तीनों रचनाकारों के पूर्व भारत - विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण की विडंबना को भोग चुका था, पर निश्चय ही संस्कृत की तत्सम शब्दावली मुसलमानों की देन तो नहीं ही है। शायद प्रतिक्रियास्वरूप यह प्रक्रिया बढ़ी और हिन्दी भाषा तत्सममय हो उठी। यह तत्सम-प्रेम केवल कछ इने-गिने लोगों का प्रेम नहीं था अपत लोक-मानस का प्रेम था, जिसकी संवेदना को ये रचनाकार आगे लेकर बढ़े। सूर और तुलसी में सामाजिक विडम्बना के प्रति आक्रोश तो कम है, पर तुलसी ने सामाजिक असमानता को दिखाने का प्रयास किया। इनसे भी पहले आगे बढ़कर कबीर ने विद्रोह का झंडा फहराया। यह विद्रोह और सामंजस्य का प्रयास, समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रांकन निर्गुण मतवादी संतों- कबीर, दादू, रैदास, नानक की वाणियों में मुखर हुआ। यह युगीन चेतना को भाषा देने का सफल प्रयास है। भले ही हम उसका संबंध बौद्ध के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों से जोड़ें। यह सत्य है कि वे ही पद, वे राग-रागनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहृत की जो उक्त मत के माननेवाले उनके पूर्ववर्ती संतों ने की थीं। क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र ही वे कबीर के मार्गदर्शक हैं। कबीर की ही भाँति ये साधक नाना मतों का खण्डन करते थे, सहज और शून्य में समाधि लगाने को कहते थे, गुरु के प्रति भक्ति करने का उपदेश देते थे कबीर और दादू के अनेक दोहे क्रमशः सरहपाद और नाथ योगियों के सीधे अनुकरण प्रतीत होते हैं। यहाँ मैं अनुकरण की बात नहीं कर रहा हूँ अपितु संवेदना के विकास और एकतानता की बात कर रहा हूँ। तत्सम के साथ-साथ देशज और तद्भव रूप मिलकर एक नई भाषा को जन्म दे रहे थे। अब्दुल रहमान संवेदना के धरातल पर तो इनमें अग्रगणी हैं, शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। ___ बारहवीं शताब्दी के आसपास अब्दुल रहमान का 'संदेश रासक' हिन्दी काव्यभाषा जगत में एक क्रांति लेकर उपस्थित होता है। राहुलजी के अनुसार यह पहले मुसलमान कवि की हिन्दी रचना है। समूची रचना में मुसलमान कवि का इस्लाम धर्म के प्रति कोई विशेष आग्रह नजर नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि हिन्दी काव्य परंपरा के परम ज्ञाता हैं। उसने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की काव्य-रूढ़ियों, काव्य-परिपाटियों का गहन अध्ययन तो किया ही था, , वह देशी भाषा का माहिर प्रयोक्ता भी रहा है। संदेश रासक का दोहा नवीनता युक्त तो है ही, - मधुर शब्दों के चयन और चित्रों के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपायन में समर्थ भी है। छंदों की विविधता,
वस्तु की अभिव्यक्ति शैली, विशेषकर नायिका का वाग्वैदग्ध हमें सूरदास की सामर्थ्य की याद