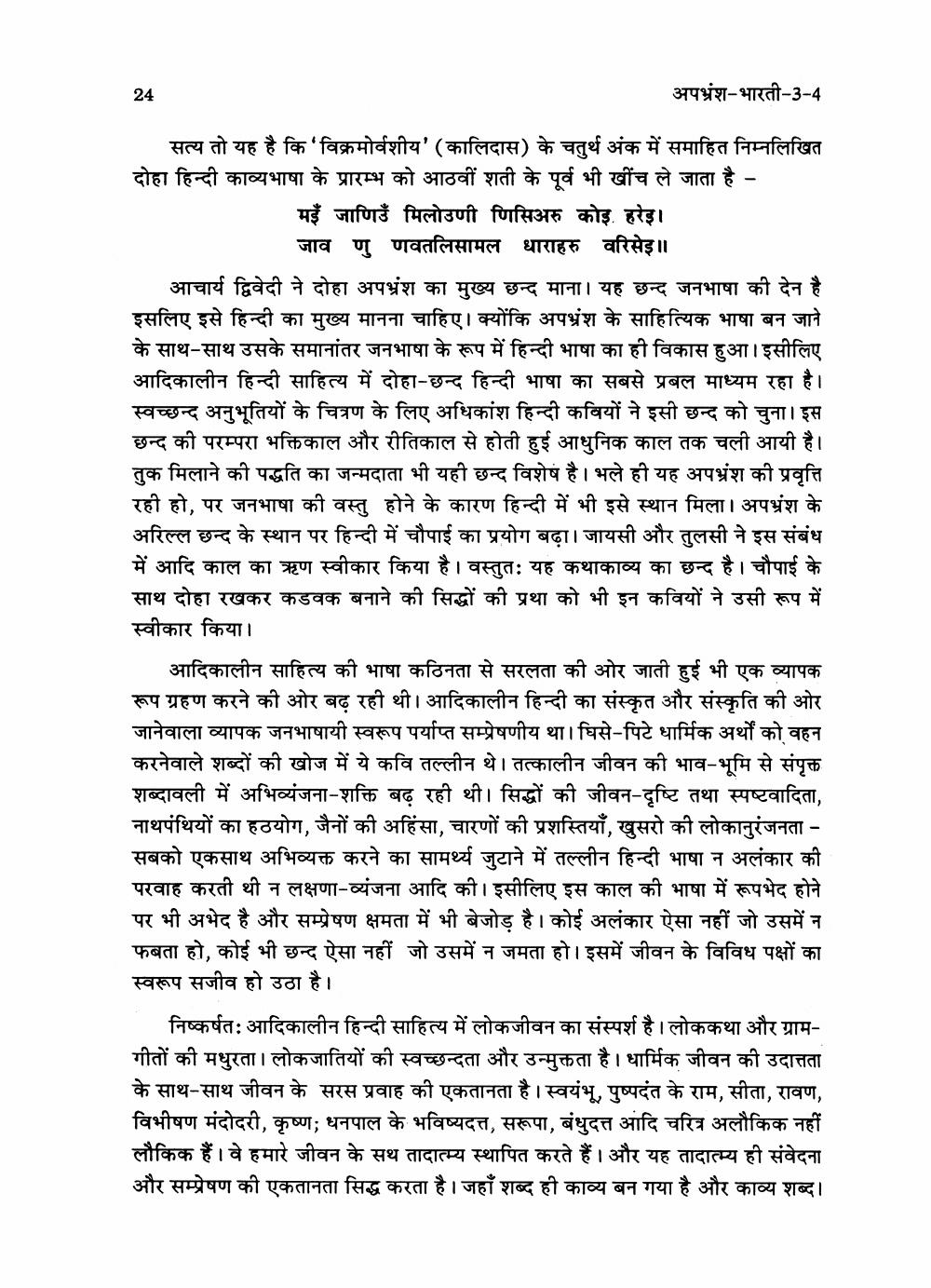________________
अपभ्रंश - भारती - 3-4
सत्य तो यह है कि 'विक्रमोर्वशीय' (कालिदास) के चतुर्थ अंक में समाहित निम्नलिखित दोहा हिन्दी काव्यभाषा के प्रारम्भ को आठवीं शती के पूर्व भी खींच ले जाता है - मइँ जाणिउँ मिलोउणी णिसिअरु कोइ हरेइ । जाव णु णवतलिसामल धाराहरु वरिसेइ ॥
24
आचार्य द्विवेदी ने दोहा अपभ्रंश का मुख्य छन्द माना । यह छन्द जनभाषा की देन है। इसलिए इसे हिन्दी का मुख्य मानना चाहिए। क्योंकि अपभ्रंश के साहित्यिक भाषा बन जाने के साथ-साथ उसके समानांतर जनभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का ही विकास हुआ। इसीलिए आदिकालीन हिन्दी साहित्य में दोहा - छन्द हिन्दी भाषा का सबसे प्रबल माध्यम रहा है। स्वच्छन्द अनुभूतियों के चित्रण के लिए अधिकांश हिन्दी कवियों ने इसी छन्द को चुना। इस छन्द की परम्परा भक्तिकाल और रीतिकाल से होती हुई आधुनिक काल तक चली आयी है । तुक मिलाने की पद्धति का जन्मदाता भी यही छन्द विशेष है। भले ही यह अपभ्रंश की प्रवृत्ति रही हो, पर जनभाषा की वस्तु होने के कारण हिन्दी में भी इसे स्थान मिला। अपभ्रंश के अरिल्ल छन्द के स्थान पर हिन्दी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। जायसी और तुलसी ने इस संबंध में आदि काल का ऋण स्वीकार किया है। वस्तुतः यह कथाकाव्य का छन्द है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कडवक बनाने की सिद्धों की प्रथा को भी इन कवियों ने उसी रूप में स्वीकार किया ।
आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई भी एक व्यापक रूप ग्रहण करने की ओर बढ़ रही थी। आदिकालीन हिन्दी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जानेवाला व्यापक जनभाषायी स्वरूप पर्याप्त सम्प्रेषणीय था । घिसे-पिटे धार्मिक अर्थों को वहन करनेवाले शब्दों की खोज में ये कवि तल्लीन थे। तत्कालीन जीवन की भाव-भूमि से संपृक्त शब्दावली में अभिव्यंजना - शक्ति बढ़ रही थी। सिद्धों की जीवन-दृष्टि तथा स्पष्टवादिता, नाथपंथियों का हठयोग, जैनों की अहिंसा, चारणों की प्रशस्तियाँ, खुसरो की लोकानुरंजनता सबको एकसाथ अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य जुटाने में तल्लीन हिन्दी भाषा न अलंकार की परवाह करती थी न लक्षणा-व्यंजना आदि की । इसीलिए इस काल की भाषा में रूपभेद होने पर भी अभेद है और सम्प्रेषण क्षमता में भी बेजोड़ है । कोई अलंकार ऐसा नहीं जो उसमें न फबता हो, कोई भी छन्द ऐसा नहीं जो उसमें न जमता हो। इसमें जीवन के विविध पक्षों का स्वरूप सजीव हो उठा है।
निष्कर्षत: आदिकालीन हिन्दी साहित्य में लोकजीवन का संस्पर्श है। लोककथा और ग्रामगीतों की मधुरता । लोकजातियों की स्वच्छन्दता और उन्मुक्तता है। धार्मिक जीवन की उदात्तता के साथ-साथ जीवन के सरस प्रवाह की एकतानता है। स्वयंभू, पुष्पदंत के राम, सीता, रावण, विभीषण मंदोदरी, कृष्ण; धनपाल के भविष्यदत्त, सरूपा, बंधुदत्त आदि चरित्र अलौकिक नहीं लौकिक हैं। वे हमारे जीवन के सथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। और यह तादात्म्य ही संवेदना और सम्प्रेषण की एकतानता सिद्ध करता है। जहाँ शब्द ही काव्य बन गया है और काव्य शब्द ।