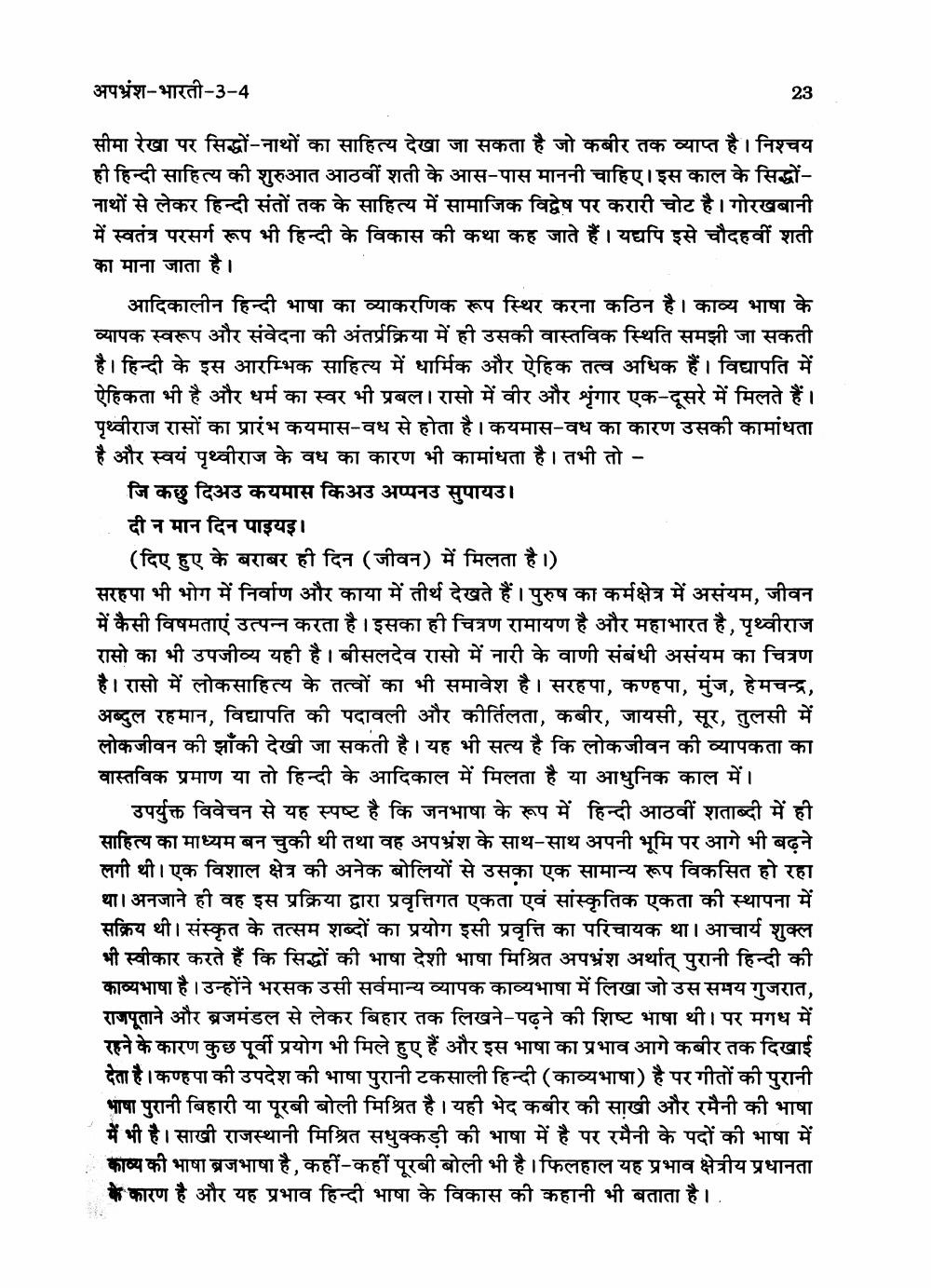________________
अपभ्रंश - भारती - 3-4
सीमा रेखा पर सिद्धों-नाथों का साहित्य देखा जा सकता है जो कबीर तक व्याप्त है। निश्चय ही हिन्दी साहित्य की शुरुआत आठवीं शती के आस-पास माननी चाहिए। इस काल के सिद्धोंनाथों से लेकर हिन्दी संतों तक के साहित्य में सामाजिक विद्वेष पर करारी चोट है। गोरखबानी में स्वतंत्र परसर्ग रूप भी हिन्दी के विकास की कथा कह जाते हैं। यद्यपि इसे चौदहवीं शती का माना जाता है।
23
आदिकालीन हिन्दी भाषा का व्याकरणिक रूप स्थिर करना कठिन है । काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर्प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है । हिन्दी के इस आरम्भिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक तत्व अधिक हैं । विद्यापति में ऐहिकता भी है और धर्म का स्वर भी प्रबल । रासो में वीर और शृंगार एक-दूसरे में मिलते हैं । पृथ्वीराज रासों का प्रारंभ कयमास- वध से होता है । कयमास - वध का कारण उसकी कामांधता है और स्वयं पृथ्वीराज के वध का कारण भी कामांधता है। तभी तो
जि कछु दिअउ कयमास किअउ अप्पनउ सुपायउ।
दी न मान दिन पाइयइ ।
(दिए हुए के बराबर ही दिन (जीवन) में मिलता है ।)
-
सरहपा भी भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। पुरुष का कर्मक्षेत्र में असंयम, जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इसका ही चित्रण रामायण है और महाभारत है, पृथ्वीराज रासो का भी उपजीव्य यही है । बीसलदेव रासो में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है । रासो में लोकसाहित्य के तत्वों का भी समावेश है। सरहपा, कण्हपा, मुंज, हेमचन्द्र, अब्दुल रहमान, विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी में लोकजीवन की झाँकी देखी जा सकती है। यह भी सत्य है कि लोकजीवन की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो हिन्दी के आदिकाल में मिलता है या आधुनिक काल I
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनभाषा के रूप में हिन्दी आठवीं शताब्दी में ही साहित्य का माध्यम बन चुकी थी तथा वह अपभ्रंश के साथ-साथ अपनी भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी थी। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था। अनजाने ही वह इस प्रक्रिया द्वारा प्रवृत्तिगत एकता एवं सांस्कृतिक एकता की स्थापना में सक्रिय थी। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इसी प्रवृत्ति का परिचायक था । आचार्य शुक्ल भी स्वीकार करते हैं कि सिद्धों की भाषा देशी भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात् पुरानी हिन्दी की काव्यभाषा है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्यभाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं और इस भाषा का प्रभाव आगे कबीर तक दिखाई देता है। कहा की उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिन्दी (काव्यभाषा) है पर गीतों की पुरानी भाषा पुरानी बिहारी या पूरबी बोली मिश्रित है। यही भेद कबीर की साखी और रमैनी की भाषा मैं भी है। सखी राजस्थानी मिश्रित सधुक्कड़ी की भाषा में है पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रजभाषा है, कहीं-कहीं पूरबी बोली भी है। फिलहाल यह प्रभाव क्षेत्रीय प्रधानता के कारण है और यह प्रभाव हिन्दी भाषा के विकास की कहानी भी बताता है । .