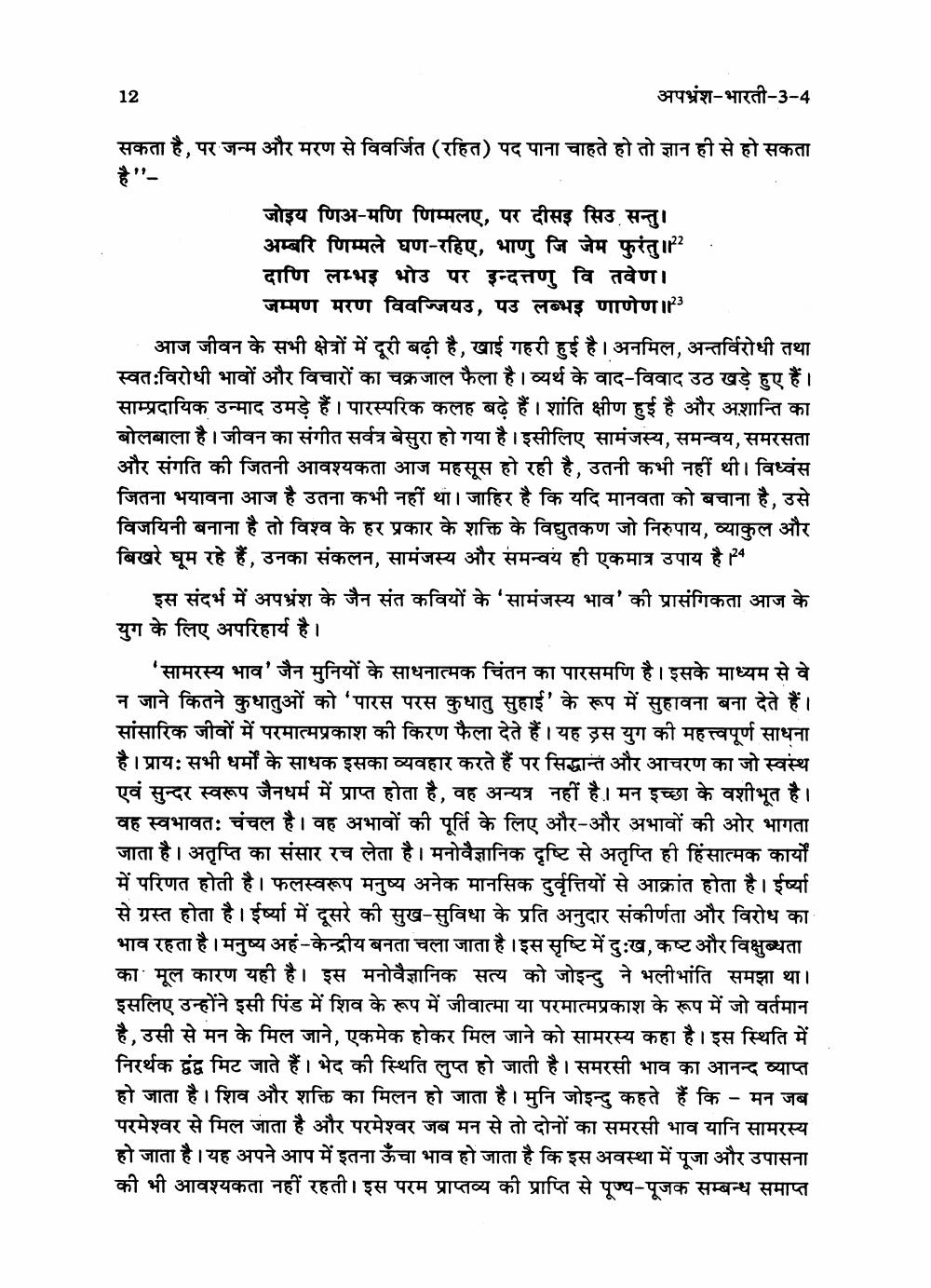________________
12
अपभ्रंश-भारती-3-4 सकता है, पर जन्म और मरण से विवर्जित (रहित) पद पाना चाहते हो तो ज्ञान ही से हो सकता
जोइय णिअ-मणि णिम्मलए, पर दीसइ सिउ सन्तु। अम्बरि णिम्मले घण-रहिए, भाणु जि जेम फुरंतु . दाणि लम्भइ भोउ पर इन्दत्तणु वि तवेण।
जम्मण मरण विवज्जियउ, पउ लब्भइ णाणेण आज जीवन के सभी क्षेत्रों में दूरी बढ़ी है, खाई गहरी हुई है। अनमिल, अन्तर्विरोधी तथा स्वत:विरोधी भावों और विचारों का चक्रजाल फैला है। व्यर्थ के वाद-विवाद उठ खड़े हुए हैं। साम्प्रदायिक उन्माद उमड़े हैं। पारस्परिक कलह बढ़े हैं। शांति क्षीण हुई है और अशान्ति का बोलबाला है। जीवन का संगीत सर्वत्र बेसुरा हो गया है। इसीलिए सामंजस्य, समन्वय, समरसता
और संगति की जितनी आवश्यकता आज महसूस हो रही है, उतनी कभी नहीं थी। विध्वंस जितना भयावना आज है उतना कभी नहीं था। जाहिर है कि यदि मानवता को बचाना है, उसे विजयिनी बनाना है तो विश्व के हर प्रकार के शक्ति के विद्युतकण जो निरुपाय, व्याकुल और बिखरे घूम रहे हैं, उनका संकलन, सामंजस्य और समन्वय ही एकमात्र उपाय है 4
इस संदर्भ में अपभ्रंश के जैन संत कवियों के 'सामंजस्य भाव' की प्रासंगिकता आज के युग के लिए अपरिहार्य है। _ 'सामरस्य भाव' जैन मुनियों के साधनात्मक चिंतन का पारसमणि है। इसके माध्यम से वे न जाने कितने कुधातुओं को 'पारस परस कुधातु सुहाई' के रूप में सुहावना बना देते हैं। सांसारिक जीवों में परमात्मप्रकाश की किरण फैला देते हैं। यह उस युग की महत्त्वपूर्ण साधना है। प्रायः सभी धर्मों के साधक इसका व्यवहार करते हैं पर सिद्धान्त और आचरण का जो स्वस्थ एवं सुन्दर स्वरूप जैनधर्म में प्राप्त होता है, वह अन्यत्र नहीं है। मन इच्छा के वशीभूत है। वह स्वभावतः चंचल है। वह अभावों की पूर्ति के लिए और-और अभावों की ओर भागता जाता है। अतृप्ति का संसार रच लेता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अतृप्ति ही हिंसात्मक कार्यों में परिणत होती है। फलस्वरूप मनुष्य अनेक मानसिक दुर्वृत्तियों से आक्रांत होता है। ईर्ष्या से ग्रस्त होता है। ईर्ष्या में दूसरे की सुख-सुविधा के प्रति अनुदार संकीर्णता और विरोध का भाव रहता है। मनुष्य अहं-केन्द्रीय बनता चला जाता है । इस सृष्टि में दुःख, कष्ट और विक्षुब्धता का मूल कारण यही है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को जोइन्द ने भलीभांति समझा था। इसलिए उन्होंने इसी पिंड में शिव के रूप में जीवात्मा या परमात्मप्रकाश के रूप में जो वर्तमान है, उसी से मन के मिल जाने, एकमेक होकर मिल जाने को सामरस्य कहा है। इस स्थिति में निरर्थक द्वंद्व मिट जाते हैं। भेद की स्थिति लुप्त हो जाती है। समरसी भाव का आनन्द व्याप्त हो जाता है। शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। मुनि जोइन्दु कहते हैं कि - मन जब परमेश्वर से मिल जाता है और परमेश्वर जब मन से तो दोनों का समरसी भाव यानि सामरस्य हो जाता है। यह अपने आप में इतना ऊँचा भाव हो जाता है कि इस अवस्था में पूजा और उपासना की भी आवश्यकता नहीं रहती। इस परम प्राप्तव्य की प्राप्ति से पूण्य-पूजक सम्बन्ध समाप्त