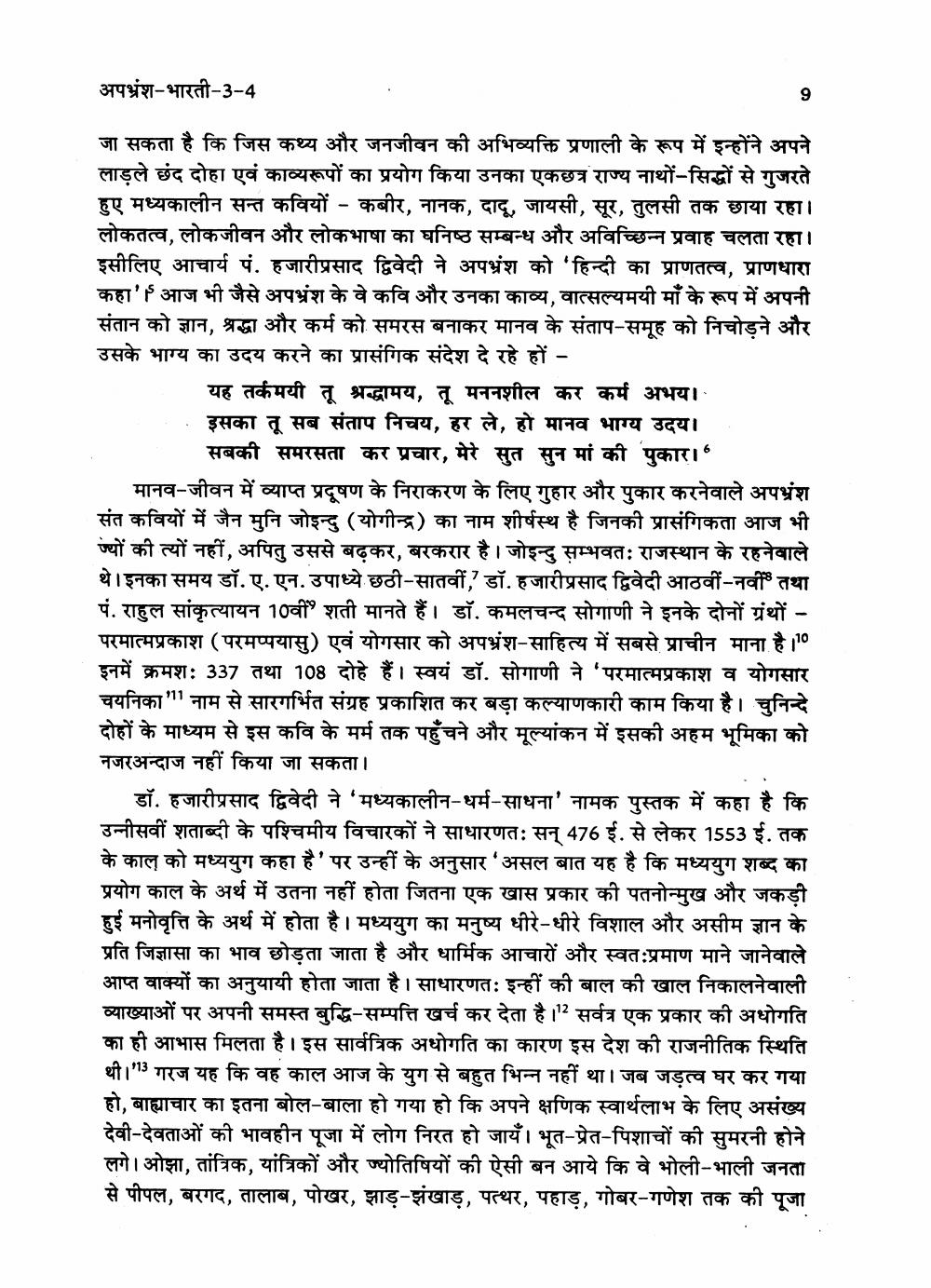________________
अपभ्रंश-भारती-3-4
जा सकता है कि जिस कथ्य और जनजीवन की अभिव्यक्ति प्रणाली के रूप में इन्होंने अपने लाड़ले छंद दोहा एवं काव्यरूपों का प्रयोग किया उनका एकछत्र राज्य नाथों-सिद्धों से गुजरते हुए मध्यकालीन सन्त कवियों - कबीर, नानक, दादू, जायसी, सूर, तुलसी तक छाया रहा। लोकतत्व, लोकजीवन और लोकभाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध और अविच्छिन्न प्रवाह चलता रहा। इसीलिए आचार्य पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को 'हिन्दी का प्राणतत्व, प्राणधारा कहा' आज भी जैसे अपभ्रंश के वे कवि और उनका काव्य, वात्सल्यमयी माँ के रूप में अपनी संतान को ज्ञान, श्रद्धा और कर्म को समरस बनाकर मानव के संताप-समूह को निचोड़ने और उसके भाग्य का उदय करने का प्रासंगिक संदेश दे रहे हों -
यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय। . इसका तू सब संताप निचय, हर ले, हो मानव भाग्य उदय।
सबकी समरसता कर प्रचार, मेरे सुत सुन मां की पुकार।' मानव-जीवन में व्याप्त प्रदूषण के निराकरण के लिए गुहार और पुकार करनेवाले अपभ्रंश संत कवियों में जैन मुनि जोइन्दु (योगीन्द्र) का नाम शीर्षस्थ है जिनकी प्रासंगिकता आज भी ज्यों की त्यों नहीं, अपितु उससे बढ़कर, बरकरार है। जोइन्दु सम्भवतः राजस्थान के रहनेवाले थे। इनका समय डॉ. ए. एन. उपाध्ये छठी-सातवीं, डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी आठवीं-नवीं तथा पं. राहुल सांकृत्यायन 10वीं शती मानते हैं। डॉ. कमलचन्द सोगाणी ने इनके दोनों ग्रंथों - परमात्मप्रकाश (परमप्पयासु) एवं योगसार को अपभ्रंश-साहित्य में सबसे प्राचीन माना है। इनमें क्रमशः 337 तथा 108 दोहे हैं। स्वयं डॉ. सोगाणी ने 'परमात्मप्रकाश व योगसार चयनिका" नाम से सारगर्भित संग्रह प्रकाशित कर बड़ा कल्याणकारी काम किया है। चुनिन्दे दोहों के माध्यम से इस कवि के मर्म तक पहुँचने और मूल्यांकन में इसकी अहम भूमिका को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। ___ डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'मध्यकालीन-धर्म-साधना' नामक पुस्तक में कहा है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चिमीय विचारकों ने साधारणतः सन् 476 ई. से लेकर 1553 ई. तक के काल को मध्ययुग कहा है' पर उन्हीं के अनुसार 'असल बात यह है कि मध्ययुग शब्द का प्रयोग काल के अर्थ में उतना नहीं होता जितना एक खास प्रकार की पतनोन्मुख और जकड़ी हुई मनोवृत्ति के अर्थ में होता है। मध्ययुग का मनुष्य धीरे-धीरे विशाल और असीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का भाव छोड़ता जाता है और धार्मिक आचारों और स्वत:प्रमाण माने जानेवाले आप्त वाक्यों का अनुयायी होता जाता है। साधारणतः इन्हीं की बाल की खाल निकालनेवाली व्याख्याओं पर अपनी समस्त बुद्धि-सम्पत्ति खर्च कर देता है। सर्वत्र एक प्रकार की अधोगति का ही आभास मिलता है। इस सार्वत्रिक अधोगति का कारण इस देश की राजनीतिक स्थिति थी।" गरज यह कि वह काल आज के युग से बहुत भिन्न नहीं था। जब जड़त्व घर कर गया हो, बाह्याचार का इतना बोल-बाला हो गया हो कि अपने क्षणिक स्वार्थलाभ के लिए असंख्य देवी-देवताओं की भावहीन पूजा में लोग निरत हो जायँ। भूत-प्रेत-पिशाचों की सुमरनी होने लगे। ओझा, तांत्रिक, यांत्रिकों और ज्योतिषियों की ऐसी बन आये कि वे भोली-भाली जनता से पीपल, बरगद, तालाब, पोखर, झाड़-झंखाड़, पत्थर, पहाड़, गोबर-गणेश तक की पूजा