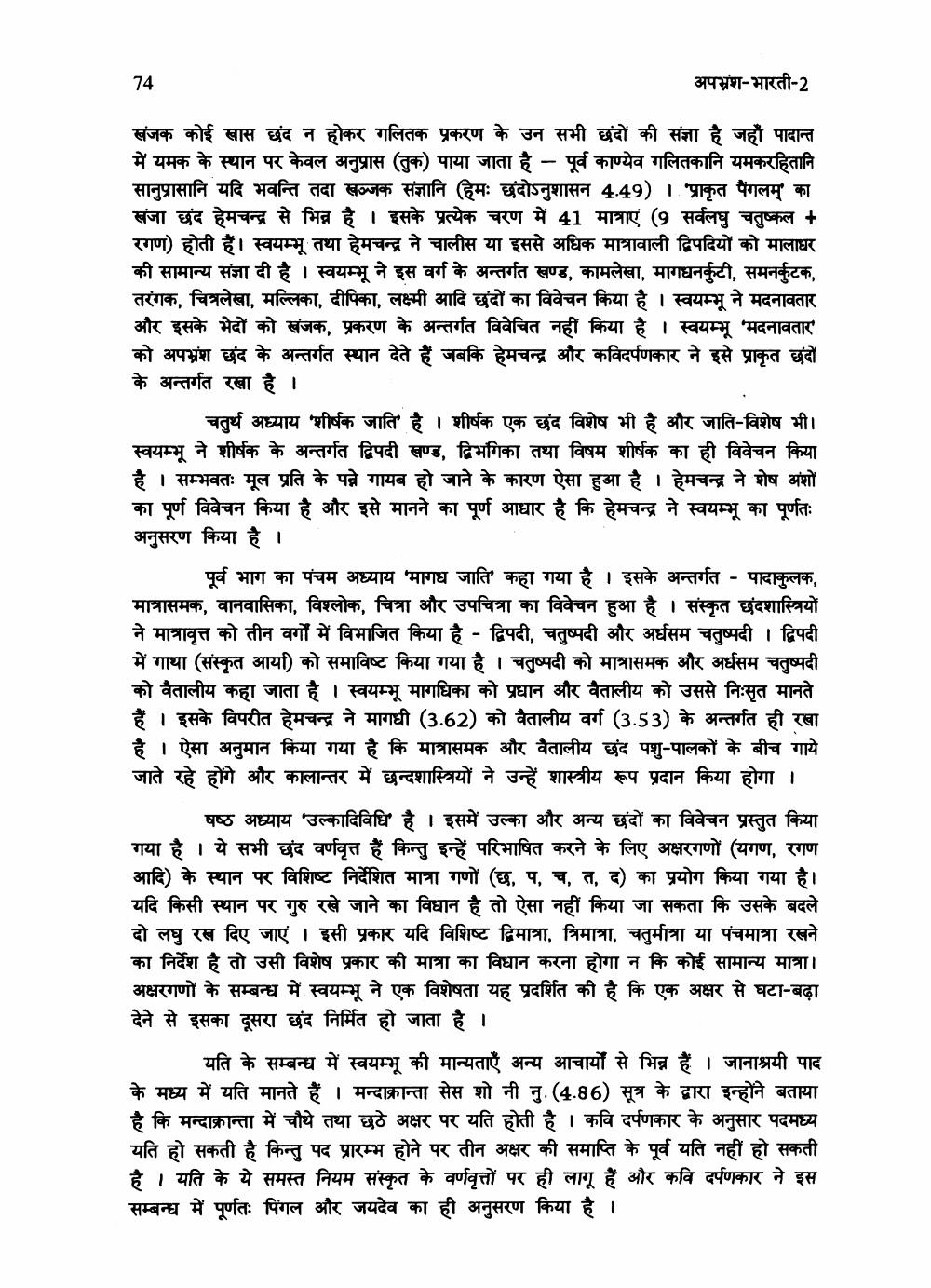________________
74
अपभ्रंश-भारती-2
खंजक कोई खास छंद न होकर गलितक प्रकरण के उन सभी छंदों की संज्ञा है जहाँ पादान्त में यमक के स्थान पर केवल अनुप्रास (तुक) पाया जाता है - पूर्व काण्येव गलितकानि यमकरहितानि सानुप्रासानि यदि भवन्ति तदा खञ्जक संज्ञानि हिमः छदोऽनुशासन 4.49) । 'प्राकृत पैगलम् का खंजा छंद हेमचन्द्र से भिन्न है । इसके प्रत्येक चरण में 41 मात्राएं (७ सर्वलघु चतुष्कल + रगण) होती हैं। स्वयम्भू तथा हेमचन्द्र ने चालीस या इससे अधिक मात्रावाली द्विपदियों को मालाधर की सामान्य संज्ञा दी है । स्वयम्भू ने इस वर्ग के अन्तर्गत खण्ड, कामलेखा, मागधनकुटी, समनकुंटक, तरंगक, चित्रलेखा, मल्लिका, दीपिका, लक्ष्मी आदि छंदों का विवेचन किया है । स्वयम्भू ने मदनावतार और इसके भेदों को खंजक, प्रकरण के अन्तर्गत विवेचित नहीं किया है । स्वयम्भू 'मदनावतार' को अपभ्रंश छंद के अन्तर्गत स्थान देते हैं जबकि हेमचन्द्र और कविदर्पणकार ने इसे प्राकृत छंदों के अन्तर्गत रखा है।
चतुर्थ अध्याय 'शीर्षक जाति है । शीर्षक एक छंद विशेष भी है और जाति-विशेष भी। स्वयम्भू ने शीर्षक के अन्तर्गत द्विपदी खण्ड, द्विभगिका तथा विषम शीर्षक का ही विवेचन किया है । सम्भवतः मूल प्रति के पन्ने गायब हो जाने के कारण ऐसा हुआ है । हेमचन्द्र ने शेष अंशों का पूर्ण विवेचन किया है और इसे मानने का पूर्ण आधार है कि हेमचन्द्र ने स्वयम्भू का पूर्णतः अनुसरण किया है ।
पूर्व भाग का पंचम अध्याय 'मागध जाति' कहा गया है । इसके अन्तर्गत - पादाकुलक, मात्रासमक, वानवासिका, विश्लोक, चित्रा और उपचित्रा का विवेचन हुआ है । संस्कृत छंदशास्त्रियों ने मात्रावृत्त को तीन वर्गों में विभाजित किया है - द्विपदी, चतुष्पदी और अर्धसम चतुष्पदी । द्विपदी में गाथा (संस्कृत आया) को समाविष्ट किया गया है । चतुष्पदी को मात्रासमक और अर्धसम चतुष्पदी को वैतालीय कहा जाता है । स्वयम्भू मागधिका को प्रधान और वैतालीय को उससे निःसृत मानते हैं । इसके विपरीत हेमचन्द्र ने मागधी (3.62) को वैतालीय वर्ग (3.53) के अन्तर्गत ही रखा है । ऐसा अनुमान किया गया है कि मात्रासमक और वैतालीय छंद पशु-पालकों के बीच गाये जाते रहे होंगे और कालान्तर में छन्दशास्त्रियों ने उन्हें शास्त्रीय रूप प्रदान किया होगा ।
षष्ठ अध्याय 'उल्कादिविधि है । इसमें उल्का और अन्य छंदों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ये सभी छंद वर्णवृत्त हैं किन्तु इन्हें परिभाषित करने के लिए अक्षरगणों (यगण, रगण आदि) के स्थान पर विशिष्ट निर्देशित मात्रा गणों (छ, प, च, त, द) का प्रयोग किया गया है। यदि किसी स्थान पर गुरु रखे जाने का विधान है तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसके बदले दो लघु रख दिए जाएं । इसी प्रकार यदि विशिष्ट द्विमात्रा, त्रिमात्रा, चतुर्मात्रा या पंचमात्रा रखने का निर्देश है तो उसी विशेष प्रकार की मात्रा का विधान करना होगा न कि कोई सामान्य मात्रा। अक्षरगणों के सम्बन्ध में स्वयम्भ ने एक विशेषता यह प्रदर्शित की है कि एक अक्षर से घटादेने से इसका दूसरा छंद निर्मित हो जाता है ।
यति के सम्बन्ध में स्वयम्भू की मान्यताएँ अन्य आचार्यों से भिन्न हैं । जानाश्रयी पाद के मध्य में यति मानते हैं । मन्दाक्रान्ता सेस शो नी नु. (4.86) सूत्र के द्वारा इन्होंने बताया है कि मन्दाक्रान्ता में चौथे तथा छठे अक्षर पर यति होती है । कवि दर्पणकार के अनुसार पदमध्य यति हो सकती है किन्तु पद प्रारम्भ होने पर तीन अक्षर की समाप्ति के पूर्व यति नहीं हो सकती है । यति के ये समस्त नियम संस्कृत के वर्णवृत्तों पर ही लागू हैं और कवि दर्पणकार ने इस सम्बन्ध में पूर्णतः पिंगल और जयदेव का ही अनुसरण किया है ।