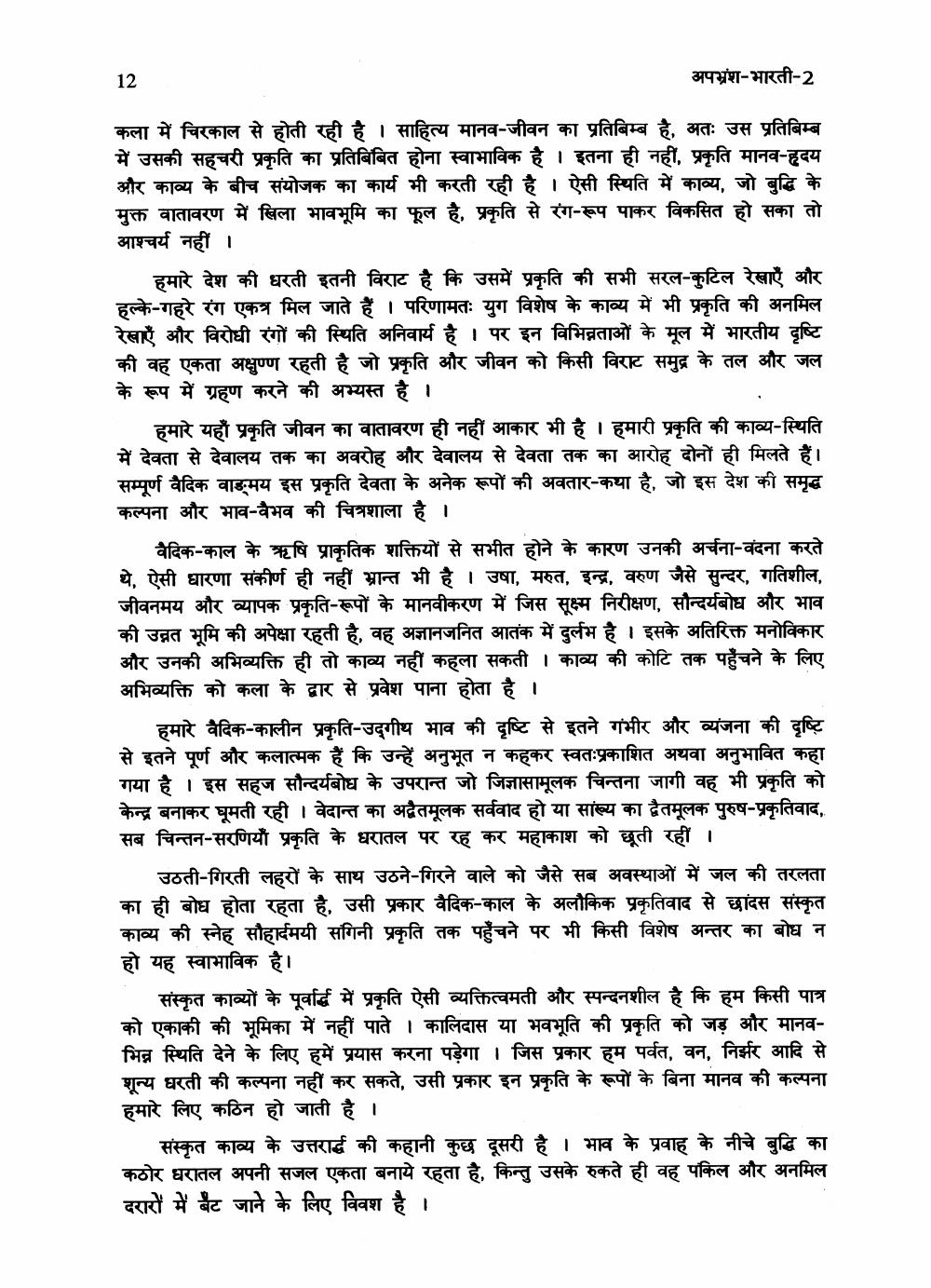________________
अपभ्रंश - भारती-2
कला में चिरकाल से होती रही है । साहित्य मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है, अतः उस प्रतिबिम्ब में उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिंबित होना स्वाभाविक है । इतना ही नहीं, प्रकृति मानव हृदय और काव्य के बीच संयोजक का कार्य भी करती रही है । ऐसी स्थिति में काव्य, जो बुद्धि के मुक्त वातावरण में खिला भावभूमि का फूल है, प्रकृति से रंग-रूप पाकर विकसित हो सका तो आश्चर्य नहीं ।
12
हमारे देश की धरती इतनी विराट है कि उसमें प्रकृति की सभी सरल-कुटिल रेखाएँ और हल्के - गहरे रंग एकत्र मिल जाते हैं । परिणामतः युग विशेष के काव्य में भी प्रकृति की अनमिल रेखाएँ और विरोधी रंगों की स्थिति अनिवार्य है । पर इन विभिन्नताओं के मूल में भारतीय दृष्टि की वह एकता अक्षुण्ण रहती है जो प्रकृति और जीवन को किसी विराट समुद्र के तल और जल के रूप में ग्रहण करने की अभ्यस्त है ।
हमारे यहाँ प्रकृति जीवन का वातावरण ही नहीं आकार भी है । हमारी प्रकृति की काव्य-स्थिति में देवता से देवालय तक का अवरोह और देवालय से देवता तक का आरोह दोनों ही मिलते हैं। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय इस प्रकृति देवता के अनेक रूपों की अवतार कथा है, जो इस देश की समृद्ध कल्पना और भाव- वैभव की चित्रशाला है ।
वैदिक काल के ऋषि प्राकृतिक शक्तियों से सभीत होने के कारण उनकी अर्चना - वंदना करते थे, ऐसी धारणा संकीर्ण ही नहीं भ्रान्त भी है । उषा, मरुत, इन्द्र, वरुण जैसे सुन्दर, गतिशील, जीवनमय और व्यापक प्रकृति रूपों के मानवीकरण में जिस सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्यबोध और भाव की उन्नत भूमि की अपेक्षा रहती है, वह अज्ञानजनित आतंक में दुर्लभ है । इसके अतिरिक्त मनोविकार और उनकी अभिव्यक्ति ही तो काव्य नहीं कहला सकती । काव्य की कोटि तक पहुँचने के लिए अभिव्यक्ति को कला के द्वार से प्रवेश पाना होता है ।
हमारे वैदिक-कालीन प्रकृति- उद्गीथ भाव की दृष्टि से इतने गंभीर और व्यंजना की दृष्टि से इतने पूर्ण और कलात्मक हैं कि उन्हें अनुभूत न कहकर स्वतः प्रकाशित अथवा अनुभावित कहा गया है । इस सहज सौन्दर्यबोध के उपरान्त जो जिज्ञासामूलक चिन्तना जागी वह भी प्रकृति को
द्र बनाकर घूमती रही । वेदान्त का अद्वैतमूलक सर्ववाद हो या सांख्य का द्वैतमूलक पुरुष प्रकृतिवाद, सब चिन्तन-सरणियाँ प्रकृति के धरातल पर रह कर महाकाश को छूती रहीं ।
उठती- गिरती लहरों के साथ उठने-गिरने वाले को जैसे सब अवस्थाओं में जल की तरलता का ही बोध होता रहता है, उसी प्रकार वैदिक काल के अलौकिक प्रकृतिवाद से छांदस संस्कृत काव्य की स्नेह सौहार्दमयी संगिनी प्रकृति तक पहुँचने पर भी किसी विशेष अन्तर का बोध न हो यह स्वाभाविक है ।
संस्कृत काव्यों के पूर्वार्द्ध में प्रकृति ऐसी व्यक्तित्वमती और स्पन्दनशील है कि हम किसी पात्र को एकाकी की भूमिका में नहीं पाते । कालिदास या भवभूति की प्रकृति को जड़ और मानवभिन्न स्थिति देने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा । जिस प्रकार हम पर्वत, वन, निर्झर आदि से शून्य धरती की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार इन प्रकृति के रूपों के बिना मानव की कल्पना हमारे लिए कठिन हो जाती है ।
संस्कृत काव्य के उत्तरार्द्ध की कहानी कुछ दूसरी है । भाव के प्रवाह के नीचे बुद्धि का कठोर धरातल अपनी सजल एकता बनाये रहता है, किन्तु उसके रुकते ही वह पंकिल और अनमिल दरारों में बैट जाने के लिए विवश है ।