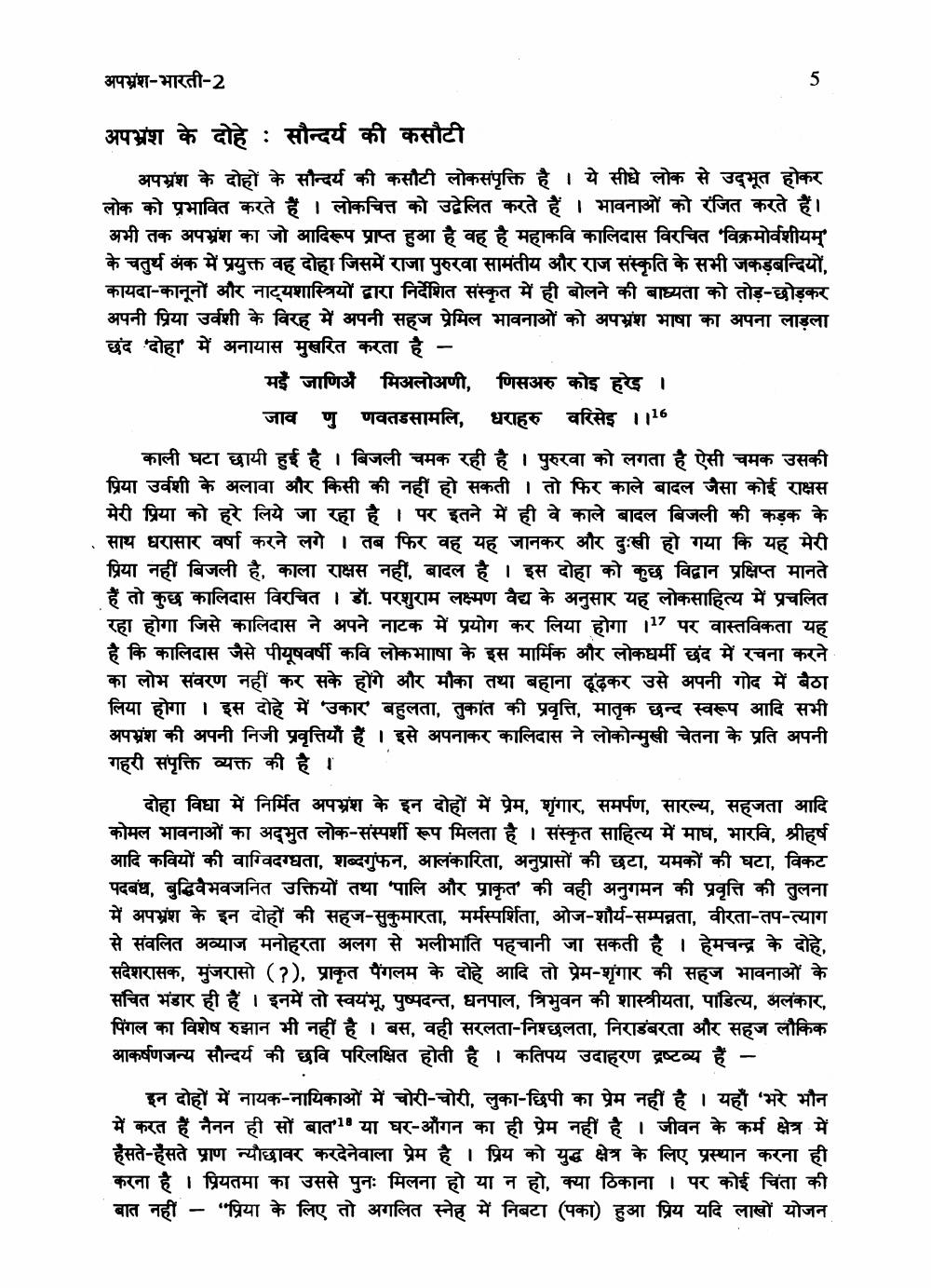________________
अपभ्रंश - भारती-2
अपभ्रंश के दोहे : सौन्दर्य की कसौटी
अपभ्रंश के दोहों के सौन्दर्य की कसौटी लोकसंपृक्ति है । ये सीधे लोक से उद्भूत होकर लोक को प्रभावित करते हैं । लोकचित्त को उद्वेलित करते हैं । भावनाओं को रंजित करते हैं। अभी तक अपभ्रंश का जो आदिरूप प्राप्त हुआ है वह है महाकवि कालिदास विरचित 'विक्रमोर्वशीयम्'
चतुर्थ अंक में प्रयुक्त वह दोहा जिसमें राजा पुरुरवा सामंतीय और राज संस्कृति के सभी जकड़बन्दियों, कायदा - कानूनों और नाट्यशास्त्रियों द्वारा निर्देशित संस्कृत में ही बोलने की बाध्यता को तोड़-छोड़कर अपनी प्रिया उर्वशी के विरह में अपनी सहज प्रेमिल भावनाओं को अपभ्रंश भाषा का अपना लाड़ला छंद 'दोहा' में अनायास मुखरित करता है
मईं जाणि मिअलोअणी, णिसअरु कोइ हरेइ । जाव णु णवतडसामलि, धराहरु वरिसेइ 1116
5
काली घटा छायी हुई है। बिजली चमक रही है । पुरुरवा को लगता है ऐसी चमक उसकी प्रिया उर्वशी के अलावा और किसी की नहीं हो सकती । तो फिर काले बादल जैसा कोई राक्षस मेरी प्रिया को हरे लिये जा रहा है । पर इतने में ही वे काले बादल बिजली की कड़क के साथ धरासार वर्षा करने लगे । तब फिर वह यह जानकर और दुःखी हो गया कि यह मेरी प्रिया नहीं बिजली है, काला राक्षस नहीं, बादल है । इस दोहा को कुछ विद्वान प्रक्षिप्त मानते 1. हैं तो कुछ कालिदास विरचित । डॉ. परशुराम लक्ष्मण वैद्य के अनुसार यह लोकसाहित्य में प्रचलित रहा होगा जिसे कालिदास ने अपने नाटक में प्रयोग कर लिया होगा । 17 पर वास्तविकता यह है कि कालिदास जैसे पीयूषवर्षी कवि लोकभाषा के इस मार्मिक और लोकधर्मी छंद में रचना करने का लोभ संवरण नहीं कर सके होंगे और मौका तथा बहाना ढूंढ़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया होगा । इस दोहे में 'उकार' बहुलता, तुकांत की प्रवृत्ति, मातृक छन्द स्वरूप आदि सभी अपभ्रंश की अपनी निजी प्रवृत्तियाँ हैं । इसे अपनाकर कालिदास ने लोकोन्मुखी चेतना के प्रति अपनी गहरी संपृक्ति व्यक्त की है ।
दोहा विधा में निर्मित अपभ्रंश के इन दोहों में प्रेम, शृंगार, समर्पण, सारल्य, सहजता आदि कोमल भावनाओं का अद्भुत लोक-संस्पर्शी रूप मिलता है । संस्कृत साहित्य में माघ, भारवि, श्रीहर्ष आदि कवियों की वाग्विदग्धता, शब्दगुंफन, आलंकारिता, अनुप्रासों की छटा, यमकों की घटा, विकट पदबंध, बुद्धिवैभवजनित उक्तियों तथा 'पालि और प्राकृत' की वही अनुगमन की प्रवृत्ति की तुलना में अपभ्रंश के इन दोहों की सहज सुकुमारता, मर्मस्पर्शिता, ओज - शौर्य - सम्पन्नता, वीरता - तप-त्याग से संवलित अव्याज मनोहरता अलग से भलीभांति पहचानी जा सकती है । हेमचन्द्र के दोहे, संदेशरासक, मुंजरासो (?), प्राकृत पैंगलम के दोहे आदि तो प्रेम-शृंगार की सहज भावनाओं के सचित भंडार ही हैं । इनमें तो स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, त्रिभुवन की शास्त्रीयता, पांडित्य, अलंकार, पिंगल का विशेष रुझान भी नहीं है । बस, वही सरलता - निश्छलता, निराडंबरता और सहज लौकिक आकर्षणजन्य सौन्दर्य की छवि परिलक्षित होती है । कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं
इन दोहों में नायक-नायिकाओं में चोरी-चोरी, लुका-छिपी का प्रेम नहीं है । यहाँ 'भरे भौन में करत हैं नैनन ही सों बात' 1" या घर-आँगन का ही प्रेम नहीं है । जीवन के कर्म क्षेत्र में हँसते-हँसते प्राण न्यौछावर करदेनेवाला प्रेम है । प्रिय को युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना ही करना है । प्रियतमा का उससे पुनः मिलना हो या न हो, क्या ठिकाना । पर कोई चिंता की M "प्रिया के लिए तो अगलित स्नेह में निबटा (पका) हुआ प्रिय यदि लाखों योजन