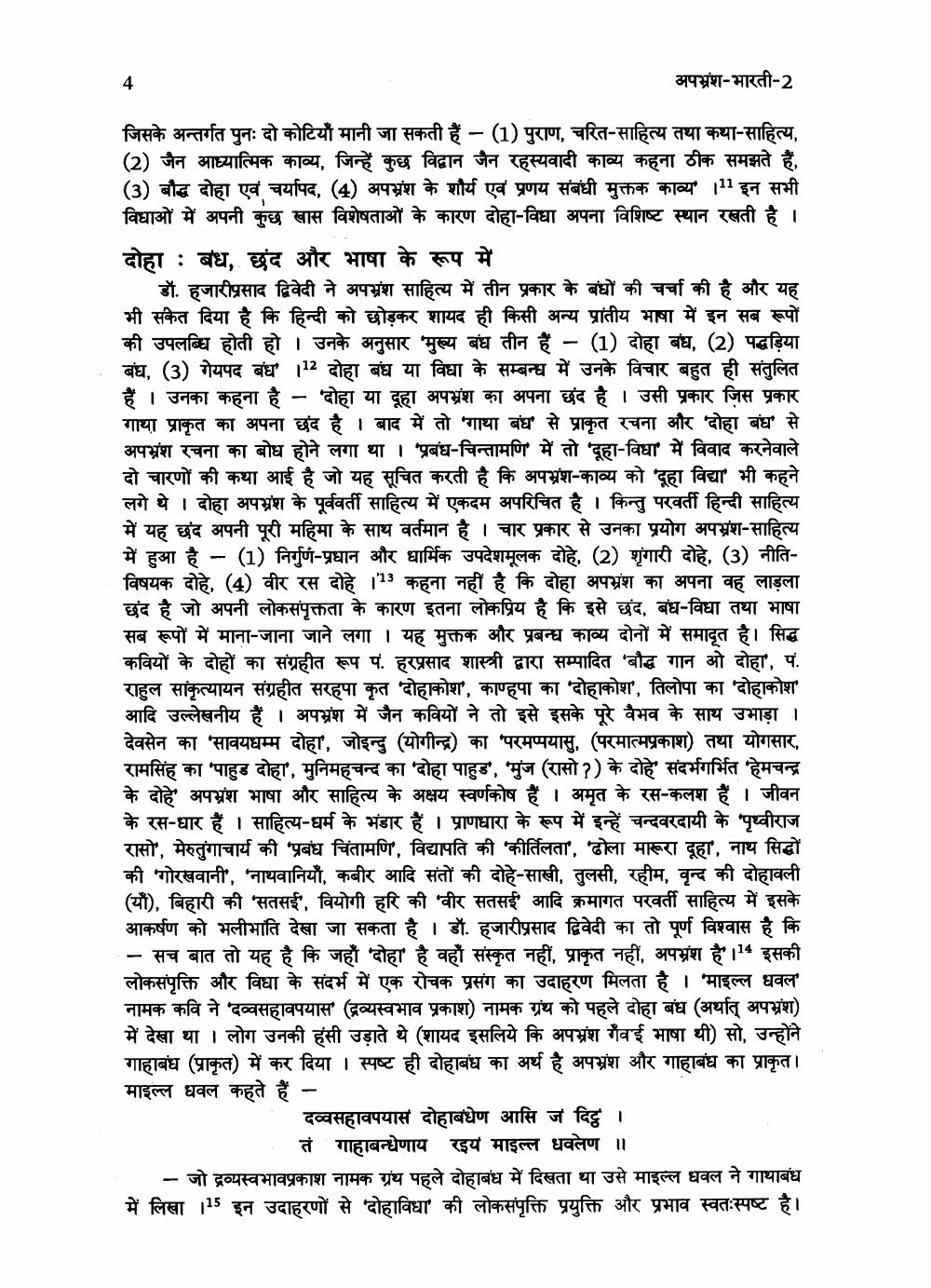________________
अपभ्रंश-भारती-2
जिसके अन्तर्गत पुनः दो कोटियाँ मानी जा सकती हैं - (1) पुराण, चरित-साहित्य तथा कथा-साहित्य, (2) जैन आध्यात्मिक काव्य, जिन्हें कुछ विद्वान जैन रहस्यवादी काव्य कहना ठीक समझते हैं, (3) बौद्ध दोहा एवं चर्यापद, (4) अपभ्रंश के शौर्य एवं प्रणय संबंधी मुक्तक काव्य' ।11 इन सभी विधाओं में अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण दोहा-विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है । दोहा : बंध, छंद और भाषा के रूप में
डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य में तीन प्रकार के बंधों की चर्चा की है और यह भी संकेत दिया है कि हिन्दी को छोड़कर शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा में इन सब रूपों की उपलब्धि होती हो । उनके अनुसार 'मुख्य बंध तीन हैं - (1) दोहा बंध, (2) पद्धड़िया बंध, (3) गेयपद बंध' ।12 दोहा बंध या विद्या के सम्बन्ध में उनके विचार बहुत ही संतुलित हैं । उनका कहना है - 'दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है । उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है । बाद में तो 'गाथा बंध' से प्राकृत रचना और 'दोहा बंध' से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा था । 'प्रबंध-चिन्तामणि' में तो 'दूहा-विधा' में विवाद करनेवाले दो चारणों की कथा आई है जो यह सूचित करती है कि अपभ्रंश-काव्य को 'दूहा विद्या' भी कहने लगे थे । दोहा अपभ्रंश के पूर्ववर्ती साहित्य में एकदम अपरिचित है । किन्तु परवर्ती हिन्दी साहित्य में यह छंद अपनी पूरी महिमा के साथ वर्तमान है । चार प्रकार से उनका प्रयोग अपभ्रंश-साहि में हुआ है - (1) निर्गुणं-प्रधान और धार्मिक उपदेशमूलक दोहे, (2) शृंगारी दोहे, (3) नीतिविषयक दोहे, (4) वीर रस दोहे ।13 कहना नहीं है कि दोहा अपभ्रंश का अपना वह लाड़ला छंद है जो अपनी लोकसंपृक्तता के कारण इतना लोकप्रिय है कि इसे छंद, बंध-विधा तथा भाषा सब रूपों में माना-जाना जाने लगा । यह मुक्तक और प्रबन्ध काव्य दोनों में समादृत है। सिद्ध कवियों के दोहों का संग्रहीत रूप पं. हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित 'बौद्ध गान ओ दोहा', पं. राहुल सांकृत्यायन संग्रहीत सरहपा कृत 'दोहाकोश', काण्हपा का 'दोहाकोश', तिलोपा का 'दोहाकोश' आदि उल्लेखनीय हैं । अपभ्रंश में जैन कवियों ने तो इसे इसके पूरे वैभव के साथ उभाड़ा । देवसेन का 'सावयधम्म दोहा', जोइन्दु (योगीन्द्र) का 'परमप्पयासु, (परमात्मप्रकाश) तथा योगसार, रामसिंह का 'पाहुड दोहा', मुनिमहचन्द का 'दोहा पाहुड', 'मुंज (रासो ?) के दोहे' संदर्भगर्भित 'हेमचन्द्र के दोहे' अपभ्रंश भाषा और साहित्य के अक्षय स्वर्णकोष हैं । अमृत के रस-कलश हैं । जीवन के रस-धार हैं । साहित्य-धर्म के भंडार हैं । प्राणधारा के रूप में इन्हें चन्दवरदायी के 'पृथ्वीराज रासो', मेरुतुंगाचार्य की 'प्रबंध चिंतामणि', विद्यापति की 'कीर्तिलता', 'ढोला मारूरा दूहा', नाथ सिद्धों की 'गोरखवानी', 'नाथवानियाँ, कबीर आदि संतों की दोहे-साखी, तुलसी, रहीम, वृन्द की दोहावली (याँ), बिहारी की 'सतसई, वियोगी हरि की 'वीर सतसई आदि क्रमागत परवर्ती साहित्य में इसके आकर्षण को भलीभाति देखा जा सकता है । डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का तो पूर्ण विश्वास है कि - सच बात तो यह है कि जहाँ 'दोहा' है वहाँ संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, अपभ्रंश है। इसकी लोकसंपृक्ति और विधा के संदर्भ में एक रोचक प्रसंग का उदाहरण मिलता है । 'माइल्ल धवल' नामक कवि ने 'दव्वसहावपयास' (द्रव्यस्वभाव प्रकाश) नामक ग्रंथ को पहले दोहा बंध (अर्थात् अपभ्रंश) में देखा था । लोग उनकी हंसी उड़ाते थे (शायद इसलिये कि अपभ्रंश गवई भाषा थी) सो, उन्होंने गाहाबंध (प्राकृत) में कर दिया । स्पष्ट ही दोहाबंध का अर्थ है अपभ्रंश और गाहाबंध का प्राकृत। माइल्ल धवल कहते हैं -
दव्वसहावपयास दोहाबंधेण आसि ज दिन ।
तं गाहाबन्धेणाय रइय माइल्ल धवलण ॥ - जो द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक ग्रंथ पहले दोहाबंध में दिखता था उसे माइल्ल धवल ने गाथाबंध में लिखा ।15 इन उदाहरणों से 'दोहाविधा' की लोकसंपृक्ति प्रयुक्ति और प्रभाव स्वतःस्पष्ट है।