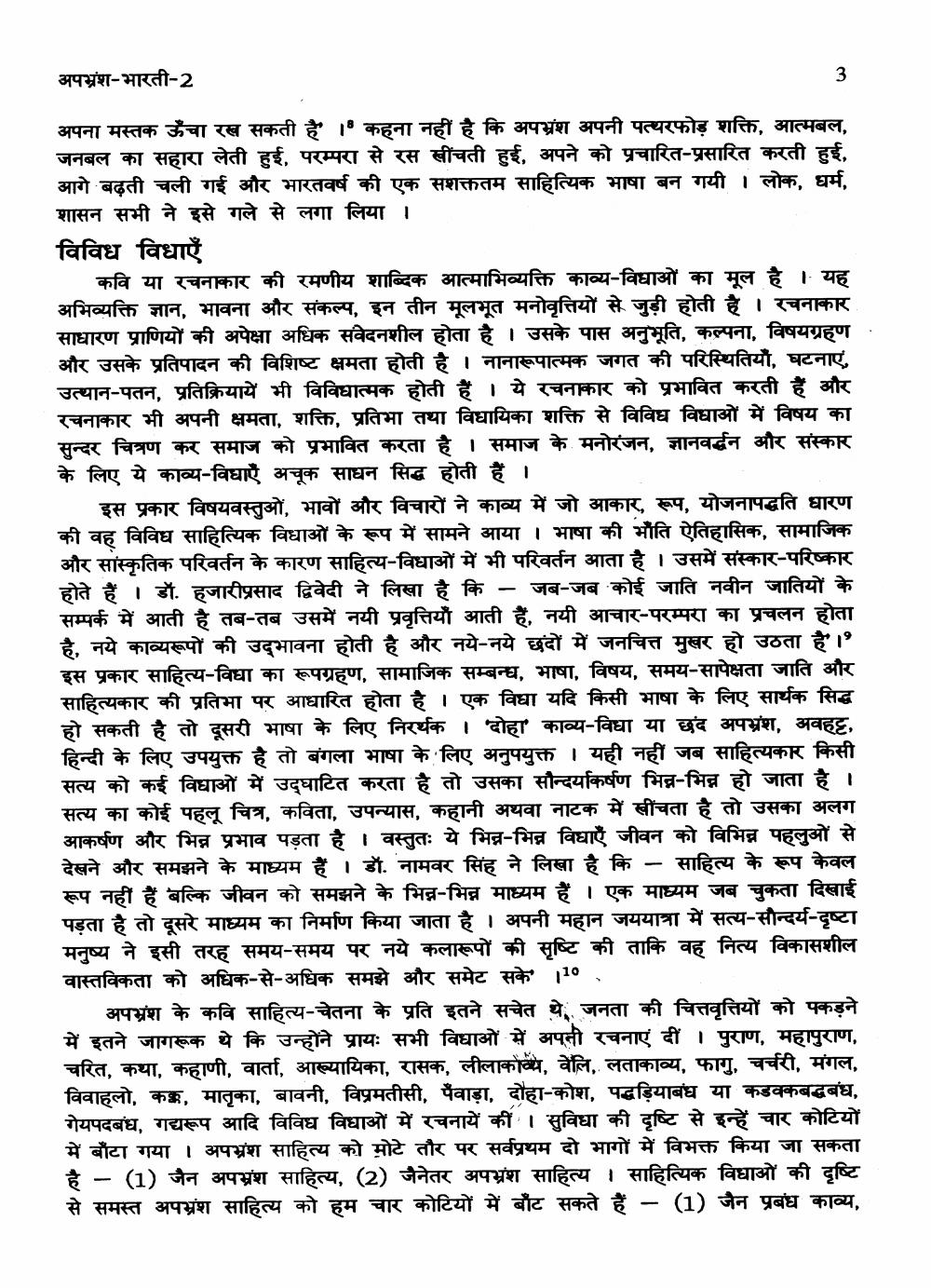________________
अपभ्रंश-भारती-2
अपना मस्तक ऊँचा रख सकती है । कहना नहीं है कि अपभ्रंश अपनी पत्थरफोड़ शक्ति, आत्मबल, जनबल का सहारा लेती हुई, परम्परा से रस खींचती हुई, अपने को प्रचारित-प्रसारित करती हुई, आगे बढ़ती चली गई और भारतवर्ष की एक सशक्ततम साहित्यिक भाषा बन गयी । लोक, धर्म, शासन सभी ने इसे गले से लगा लिया । विविध विधाएँ
कवि या रचनाकार की रमणीय शाब्दिक आत्माभिव्यक्ति काव्य-विधाओं का मूल है । यह अभिव्यक्ति ज्ञान, भावना और संकल्प, इन तीन मूलभूत मनोवृत्तियों से जुड़ी होती है । रचनाकार साधारण प्राणियों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है । उसके पास अनुभति, व और उसके प्रतिपादन की विशिष्ट क्षमता होती है । नानारूपात्मक जगत की परिस्थितियाँ, घटनाएं, उत्थान-पतन, प्रतिक्रियायें भी विविधात्मक होती हैं । ये रचनाकार को प्रभावित करती हैं और रचनाकार भी अपनी क्षमता, शक्ति, प्रतिभा तथा विधायिका शक्ति से विविध विधाओं में विषय का सुन्दर चित्रण कर समाज को प्रभावित करता है । समाज के मनोरंजन, ज्ञानवर्द्धन और संस्कार के लिए ये काव्य-विधाएँ अचूक साधन सिद्ध होती हैं ।
इस प्रकार विषयवस्तुओं, भावों और विचारों ने काव्य में जो आकार, रूप, योजनापद्धति धारण की वह विविध साहित्यिक विधाओं के रूप में सामने आया । भाषा की भाँति ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण साहित्य-विधाओं में भी परिवर्तन आता है । उसमें संस्कार-परिष्कार होते हैं । डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि - जब-जब कोई जाति नवीन जातियों के सम्पर्क में आती है तब-तब उसमें नयी प्रवृत्तियाँ आती हैं, नयी आचार-परम्परा का प्रचलन होता है, नये काव्यरूपों की उद्भावना होती है और नये-नये छंदों में जनचित्त मुखर हो उठता है।' इस प्रकार साहित्य-विधा का रूपग्रहण, सामाजिक सम्बन्ध, भाषा, विषय, समय-सापेक्षता जाति और साहित्यकार की प्रतिभा पर आधारित होता है । एक विधा यदि किसी भाषा के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है तो दूसरी भाषा के लिए निरर्थक । 'दोहा काव्य-विधा या छंद अपभ्रंश, अवहट्ट, हिन्दी के लिए उपयुक्त है तो बंगला भाषा के लिए अनुपयुक्त । यही नहीं जब साहित्यकार किसी सत्य को कई विधाओं में उद्घाटित करता है तो उसका सौन्दर्याकर्षण भिन्न-भिन्न हो जाता है । सत्य का कोई पहलू चित्र, कविता, उपन्यास, कहानी अथवा नाटक में खींचता है तो उसका अलग आकर्षण और भिन्न प्रभाव पड़ता है । वस्तुतः ये भिन्न-भिन्न विधाएँ जीवन को विभिन्न पहलुओं से देखने और समझने के माध्यम हैं । डॉ. नामवर सिंह ने लिखा है कि - साहित्य के रूप केवल रूप नहीं हैं बल्कि जीवन को समझने के भिन्न-भिन्न माध्यम हैं । एक माध्यम जब चुकता दिखाई पड़ता है तो दूसरे माध्यम का निर्माण किया जाता है । अपनी महान जययात्रा में सत्य-सौन्दर्य-दृष्टा मनुष्य ने इसी तरह समय-समय पर नये कलारूपों की सृष्टि की ताकि वह नित्य विकासशील वास्तविकता को अधिक-से-अधिक समझे और समेट सके ।10. _अपभ्रंश के कवि साहित्य-चेतना के प्रति इतने सचेत थे, जनता की चित्तवृत्तियों को पकड़ने में इतने जागरूक थे कि उन्होंने प्रायः सभी विधाओं में अपनी रचनाएं दी । पुराण, महापुराण, चरित, कथा, कहाणी, वार्ता, आख्यायिका, रासक, लीलाकोव्य, वेलि, लताकाव्य, फागु, चर्चरी, मंगल, विवाहलो, कक्क, मातृका, बावनी, विप्रमतीसी, पँवाड़ा, दोहा-कोश, पद्धड़ियाबंध या कडक्कबद्धबंध, गेयपदबंध, गद्यरूप आदि विविध विधाओं में रचनायें की । सुविधा की दृष्टि से इन्हें चार कोटियों में बाँटा गया । अपभ्रंश साहित्य को मोटे तौर पर सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - (1) जैन अपभ्रंश साहित्य, (2) जैनेतर अपभ्रंश साहित्य । साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से समस्त अपभ्रंश साहित्य को हम चार कोटियों में बाँट सकते हैं - (1) जैन प्रबंध काव्य,