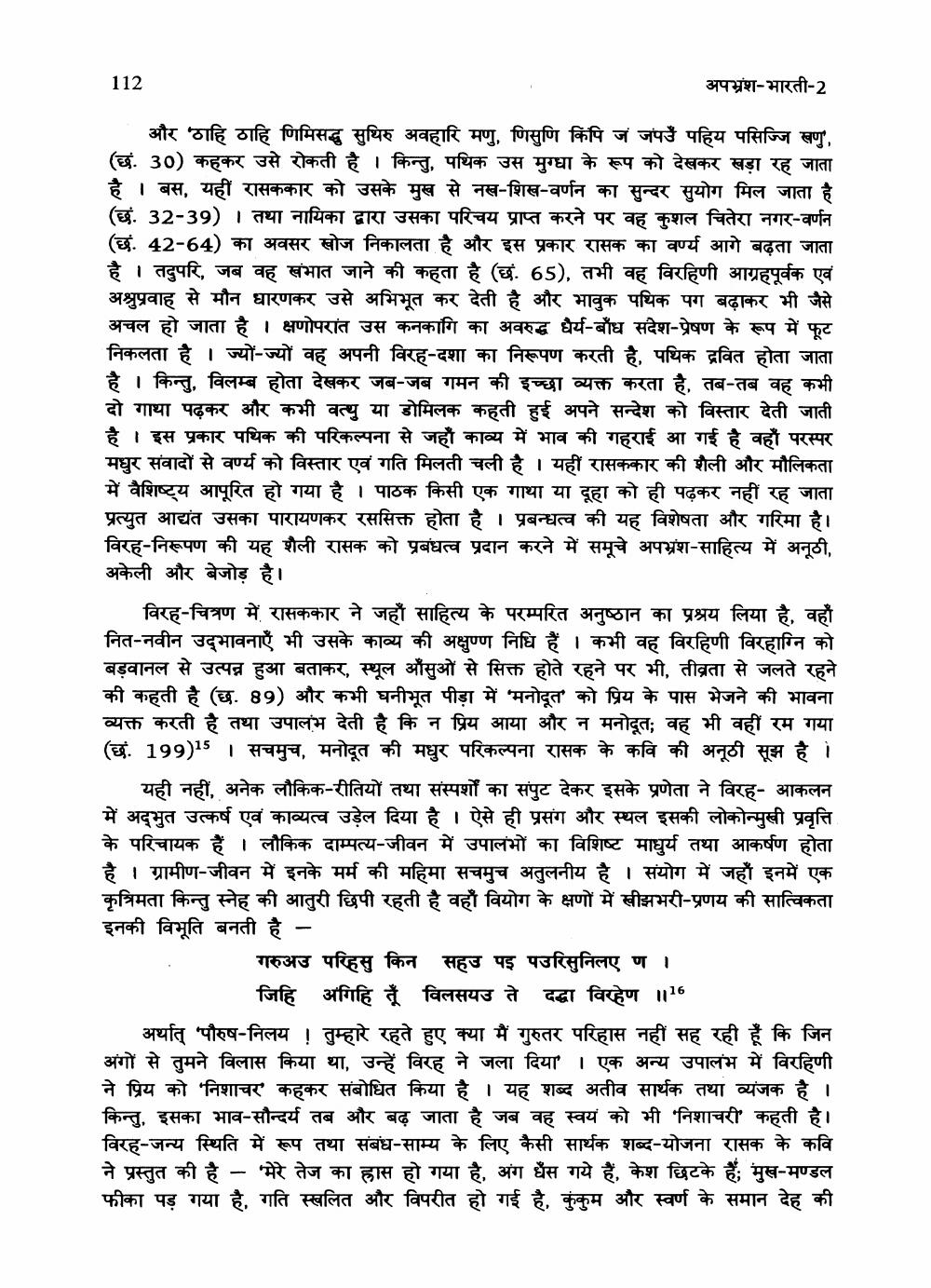________________
112
अपभ्रंश-भारती-2
____ और 'ठाहि ठाहि णिमिसद्ध सुथिरु अवहारि मणु, णिसुणि किंपि जं जपउँ पहिय पसिज्जि खणु, (छ. 30) कहकर उसे रोकती है । किन्तु, पथिक उस मुग्धा के रूप को देखकर खड़ा रह जाता है । बस, यहीं रासककार को उसके मुख से नख-शिख-वर्णन का सुन्दर सुयोग मिल जाता है (छ. 32-39) । तथा नायिका द्वारा उसका परिचय प्राप्त करने पर वह कुशल चितेरा नगर-वर्णन (छ. 42-64) का अवसर खोज निकालता है और इस प्रकार रासक का वर्ण्य आगे बढ़ता जाता है । तदुपरि, जब वह खंभात जाने की कहता है (छ. 65), तभी वह विरहिणी आग्रहपूर्वक एवं अश्रुप्रवाह से मौन धारणकर उसे अभिभूत कर देती है और भावुक पथिक पग बढ़ाकर भी जैसे अचल हो जाता है । क्षणोपरांत उस कनकागि का अवरुद्ध धैर्य-बाँध संदेश-प्रेषण के रूप में फट निकलता है । ज्यों-ज्यों वह अपनी विरह-दशा का निरूपण करती है, पथिक द्रवित होता जाता है । किन्तु, विलम्ब होता देखकर जब-जब गमन की इच्छा व्यक्त करता है, तब-तब वह कभी दो गाथा पढ़कर और कभी वत्थु या डोमिलक कहती हुई अपने सन्देश को विस्तार देती जाती है । इस प्रकार पथिक की परिकल्पना से जहाँ काव्य में भाव की गहराई आ गई है वहाँ परस्पर मधुर संवादों से वर्ण्य को विस्तार एवं गति मिलती चली है । यहीं रासककार की शैली और मौलिकता में वैशिष्ट्य आपूरित हो गया है । पाठक किसी एक गाथा या दूहा को ही पढ़कर नहीं रह जाता प्रत्युत आद्यंत उसका पारायणकर रससिक्त होता है । प्रबन्धत्व की यह विशेषता और गरिमा है। विरह-निरूपण की यह शैली रासक को प्रबंधत्व प्रदान करने में समूचे अपभ्रंश-साहित्य में अनूठी, अकेली और बेजोड़ है।
विरह-चित्रण में रासककार ने जहाँ साहित्य के परम्परित अनुष्ठान का प्रश्रय लिया है, वहाँ नित-नवीन उद्भावनाएँ भी उसके काव्य की अक्षुण्ण निधि हैं । कभी वह विरहिणी विरहाग्नि को बड़वानल से उत्पन्न हुआ बताकर, स्थूल आँसुओं से सिक्त होते रहने पर भी, तीव्रता से जलते रहने की कहती है (छ.89) और कभी घनीभूत पीड़ा में 'मनोदूत' को प्रिय के पास भेजने की भावना व्यक्त करती है तथा उपालंभ देती है कि न प्रिय आया और न मनोदूत; वह भी वहीं रम गया (छ. 199)15 । सचमुच, मनोदूत की मधुर परिकल्पना रासक के कवि की अनूठी सूझ है ।
यही नहीं, अनेक लौकिक-रीतियों तथा संस्पर्शों का संपुट देकर इसके प्रणेता ने विरह- आकलन में अद्भुत उत्कर्ष एवं काव्यत्व उड़ेल दिया है । ऐसे ही प्रसंग और स्थल इसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के परिचायक हैं । लौकिक दाम्पत्य-जीवन में उपालंभों का विशिष्ट माधुर्य तथा आकर्षण होता है । ग्रामीण-जीवन में इनके मर्म की महिमा सचमुच अतुलनीय है । संयोग में जहाँ इनमें एक कृत्रिमता किन्तु स्नेह की आतुरी छिपी रहती है वहाँ वियोग के क्षणों में खीझभरी-प्रणय की सात्विकता इनकी विभूति बनती है -
गरुअउ परिहसु किन सहउ पइ पउरिसुनिलए ण ।
जिहि अगिहि तूं विलसयउ ते दद्धा विरहेण ॥16 अर्थात् 'पौरुष-निलय । तुम्हारे रहते हुए क्या मैं गुरुतर परिहास नहीं सह रही हूँ कि जिन अंगों से तुमने विलास किया था, उन्हें विरह ने जला दिया' । एक अन्य उपालंभ में विरहिणी ने प्रिय को 'निशाचर' कहकर संबोधित किया है । यह शब्द अतीव सार्थक तथा व्यंजक है । किन्तु, इसका भाव-सौन्दर्य तब और बढ़ जाता है जब वह स्वयं को भी 'निशाचरी कहती है। विरह-जन्य स्थिति में रूप तथा संबंध-साम्य के लिए कैसी सार्थक शब्द-योजना रासक के कवि ने प्रस्तुत की है – 'मेरे तेज का ह्रास हो गया है, अंग फँस गये हैं, केश छिटके हैं; मुख-मण्डल फीका पड़ गया है. गति स्खलित और विपरीत हो गई है, कुंकुम और स्वर्ण के समान देह की