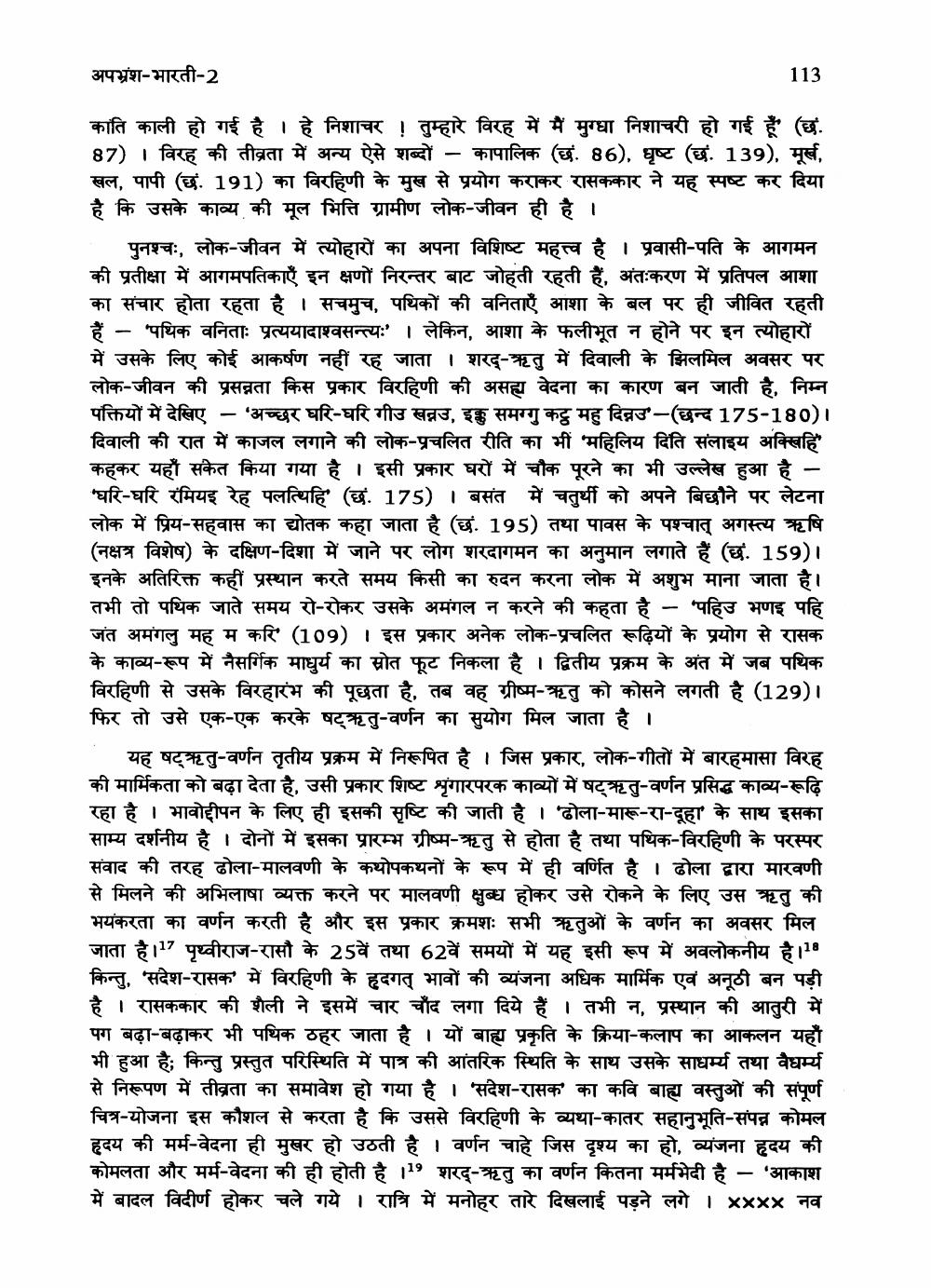________________
अपभ्रंश-भारती-2
113
कांति काली हो गई है । हे निशाचर । तुम्हारे विरह में मैं मुग्धा निशाचरी हो गई हूँ (छ. 87) । विरह की तीव्रता में अन्य ऐसे शब्दों - कापालिक (छ.86), धृष्ट (छ. 139), मूर्ख, खल, पापी (छं. 191) का विरहिणी के मुख से प्रयोग कराकर रासककार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके काव्य की मूल भित्ति ग्रामीण लोक-जीवन ही है ।
पुनश्चः, लोक-जीवन में त्योहारों का अपना विशिष्ट महत्त्व है । प्रवासी-पति के आगमन की प्रतीक्षा में आगमपतिकाएँ इन क्षणों निरन्तर बाट जोहती रहती हैं, अंतःकरण में प्रतिपल आशा का संचार होता रहता है । सचमुच, पथिकों की वनिताएँ आशा के बल पर ही जीवित रहती हैं - 'पथिक वनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः' । लेकिन, आशा के फलीभूत न होने पर इन त्योहारों में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता । शरद्-ऋतु में दिवाली के झिलमिल अवसर पर लोक-जीवन की प्रसन्नता किस प्रकार विरहिणी की असह्य वेदना का कारण बन जाती है, निम्न पक्तियों में देखिए - 'अच्छर घरि-घरि गीउ खन्नउ, इक्कु समग्गु कट्ठ महु दिन्नउ'-(छन्द 175-180)। दिवाली की रात में काजल लगाने की लोक-प्रचलित रीति का भी 'महिलिय दिति सलाइय अक्खिही कहकर यहाँ सकेत किया गया है। इसी प्रकार घरों में चौक परने का भी उल्लेख हआ है - 'घरि-घरि रंमियइ रेह पलस्थिहि' (छ. 175) । बसंत में चतुर्थी को अपने बिछौने पर लेटना लोक में प्रिय-सहवास का द्योतक कहा जाता है (छ. 195) तथा पावस के पश्चात् अगस्त्य ऋषि (नक्षत्र विशेष) के दक्षिण-दिशा में जाने पर लोग शरदागमन का अनुमान लगाते हैं (छ. 159)। इनके अतिरिक्त कहीं प्रस्थान करते समय किसी का रुदन करना लोक में अशुभ माना जाता है। तभी तो पथिक जाते समय रो-रोकर उसके अमंगल न करने की कहता है - 'पहिउ भणइ पहि जंत अमंगलु मह म करि' (109) । इस प्रकार अनेक लोक-प्रचलित रूढ़ियों के प्रयोग से रासक के काव्य-रूप में नैसर्गिक माधुर्य का स्रोत फूट निकला है । द्वितीय प्रक्रम के अंत में जब पथिक विरहिणी से उसके विरहारंभ की पूछता है, तब वह ग्रीष्म ऋतु को कोसने लगती है (129)। फिर तो उसे एक-एक करके षट्ऋतु-वर्णन का सुयोग मिल जाता है ।
यह षट्ऋतु-वर्णन तृतीय प्रक्रम में निरूपित है । जिस प्रकार, लोक-गीतों में बारहमासा विरह की मार्मिकता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार शिष्ट श्रृंगारपरक काव्यों में षट्ऋतु-वर्णन प्रसिद्ध काव्य-रूढ़ि रहा है । भावोद्दीपन के लिए ही इसकी सृष्टि की जाती है । 'ढोला-मारू-रा-दूहा' के साथ इसका साम्य दर्शनीय है । दोनों में इसका प्रारम्भ ग्रीष्म ऋतु से होता है तथा पथिक-विरहिणी के परस्पर संवाद की तरह ढोला-मालवणी के कथोपकथनों के रूप में ही वर्णित है । ढोला द्वारा मारवणी से मिलने की अभिलाषा व्यक्त करने पर मालवणी क्षुब्ध होकर उसे रोकने के लिए उस ऋतु की भयंकरता का वर्णन करती है और इस प्रकार क्रमशः सभी ऋतुओं के वर्णन का अवसर मिल जाता है।17 पृथ्वीराज-रासौ के 25वें तथा 62वें समयों में यह इसी रूप में अवलोकनीय है।। किन्तु, 'सदेश-रासक' में विरहिणी के हृदगत् भावों की व्यंजना अधिक मार्मिक एवं अनूठी बन पड़ी है । रासककार की शैली ने इसमें चार चाँद लगा दिये हैं । तभी न, प्रस्थान की आतुरी में पग बढ़ा-बढ़ाकर भी पथिक ठहर जाता है। यों बाह्य प्रकृति के क्रिया-कलाप का आकलन यहाँ भी हुआ है; किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति में पात्र की आंतरिक स्थिति के साथ उसके साधर्म्य तथा वैधर्म्य से निरूपण में तीव्रता का समावेश हो गया है । 'सदेश-रासक' का कवि बाह्य वस्तुओं की संपूर्ण चित्र-योजना इस कौशल से करता है कि उससे विरहिणी के व्यथा-कातर सहानुभूति-संपन्न कोमल हृदय की मर्म-वेदना ही मुखर हो उठती है । वर्णन चाहे जिस दृश्य का हो, व्यंजना हृदय की कोमलता और मर्म-वेदना की ही होती है ।" शरद्-ऋतु का वर्णन कितना मर्मभेदी है - 'आकाश में बादल विदीर्ण होकर चले गये । रात्रि में मनोहर तारे दिखलाई पड़ने लगे । xxxx नव