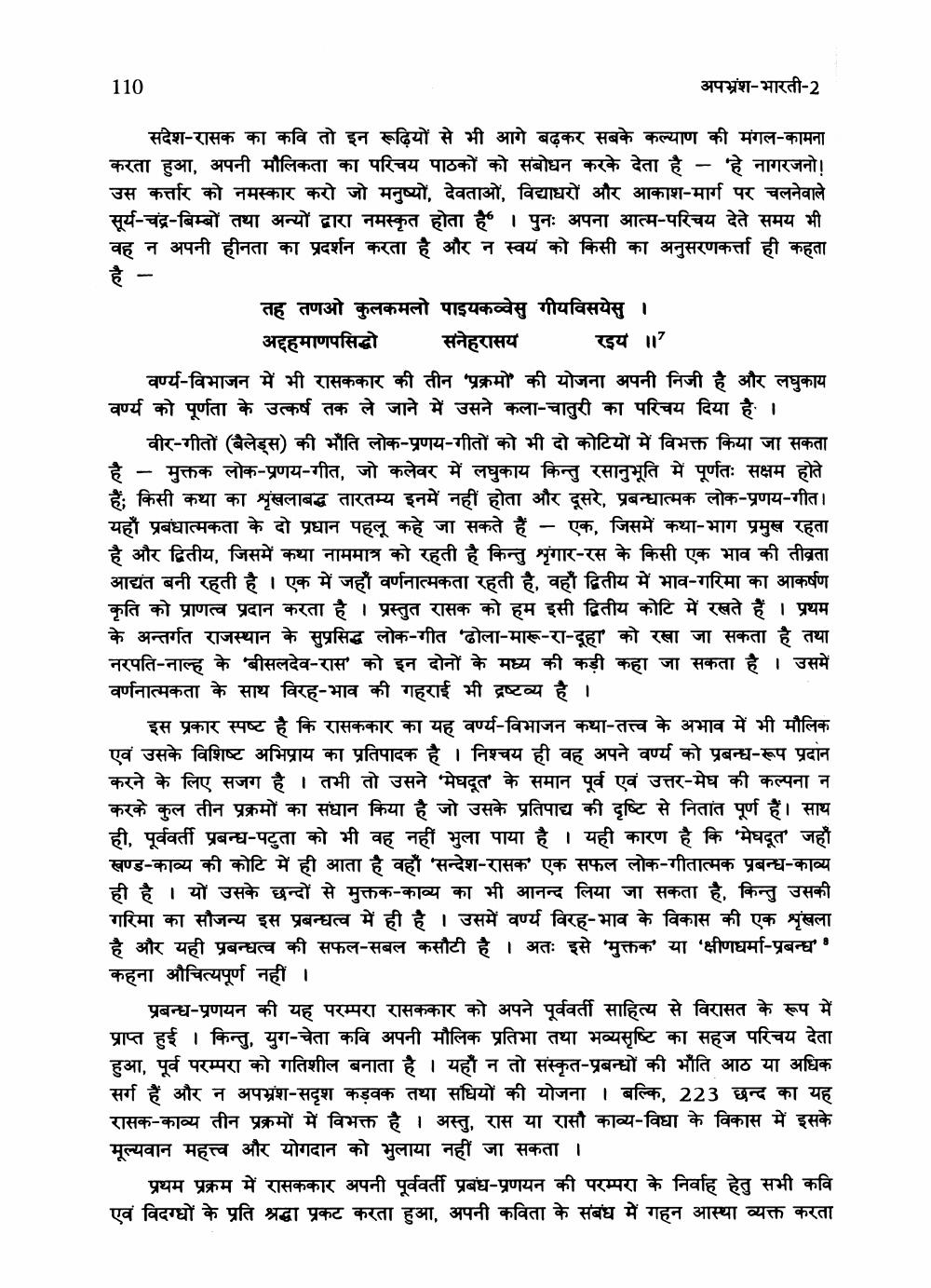________________
110
अपभ्रंश-भारती-2
सदेश-रासक का कवि तो इन रूढ़ियों से भी आगे बढ़कर सबके कल्याण की मंगल-कामना करता हुआ, अपनी मौलिकता का परिचय पाठकों को संबोधन करके देता है - 'हे नागरजनो। उस कार को नमस्कार करो जो मनुष्यों, देवताओं, विद्याधरों और आकाश-मार्ग पर चलनेवाले सूर्य-चंद्र-बिम्बों तथा अन्यों द्वारा नमस्कृत होता है । पुनः अपना आत्म-परिचय देते समय भी वह न अपनी हीनता का प्रदर्शन करता है और न स्वयं को किसी का अनुसरणकर्ता ही कहता
तह तणओ कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । अद्दहमाणपसिद्धो सनेहरासयं रइयं ॥
वर्ण्य-विभाजन में भी रासककार की तीन 'प्रक्रमों की योजना अपनी निजी है और लघुकाय वर्ण्य को पूर्णता के उत्कर्ष तक ले जाने में उसने कला-चातुरी का परिचय दिया है।
वीर-गीतों (बैलेड्स) की भाँति लोक-प्रणय-गीतों को भी दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है - मुक्तक लोक-प्रणय-गीत, जो कलेवर में लघुकाय किन्तु रसानुभूति में पूर्णतः सक्षम होते हैं; किसी कथा का श्रृंखलाबद्ध तारतम्य इनमें नहीं होता और दूसरे, प्रबन्धात्मक लोक-प्रणय-गीत। यहाँ प्रबंधात्मकता के दो प्रधान पहलू कहे जा सकते हैं - एक, जिसमें कथा-भाग प्रमुख रहता है और द्वितीय, जिसमें कथा नाममात्र को रहती है किन्तु श्रृंगार-रस के किसी एक भाव की तीव्रता आद्यंत बनी रहती है । एक में जहाँ वर्णनात्मकता रहती है, वहाँ द्वितीय में भाव-गरिमा का आकर्षण कृति को प्राणत्व प्रदान करता है । प्रस्तुत रासक को हम इसी द्वितीय कोटि में रखते हैं । प्रथम के अन्तर्गत राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक-गीत 'ढोला-मारू-रा-दूहा को रखा जा सकता है तथा नरपति-नाल्ह के 'बीसलदेव-रास' को इन दोनों के मध्य की कड़ी कहा जा सकता है । उसमें वर्णनात्मकता के साथ विरह-भाव की गहराई भी द्रष्टव्य है ।
इस प्रकार स्पष्ट है कि रासककार का यह वर्ण्य-विभाजन कथा-तत्त्व के अभाव में भी मौलिक एवं उसके विशिष्ट अभिप्राय का प्रतिपादक है । निश्चय ही वह अपने वर्ण्य को प्रबन्ध-रूप प्रदान करने के लिए सजग है । तभी तो उसने 'मेघदूत' के समान पूर्व एवं उत्तर-मेघ की कल्पना न करके कुल तीन प्रक्रमों का संधान किया है जो उसके प्रतिपाद्य की दृष्टि से नितांत पूर्ण हैं। साथ ही, पूर्ववर्ती प्रबन्ध-पटुता को भी वह नहीं भुला पाया है । यही कारण है कि 'मेघदूत' जहाँ खण्ड-काव्य की कोटि में ही आता है वहाँ 'सन्देश-रासक' एक सफल लोक-गीतात्मक प्रबन्ध-काव्य ही है । यों उसके छन्दों से मुक्तक-काव्य का भी आनन्द लिया जा सकता है, किन्तु उसकी गरिमा का सौजन्य इस प्रबन्धत्व में ही है । उसमें वर्ण्य विरह-भाव के विकास की एक श्रृंखला है और यही प्रबन्धत्व की सफल-सबल कसौटी है । अतः इसे 'मुक्तक' या 'क्षीणधम कहना औचित्यपूर्ण नहीं ।
प्रबन्ध-प्रणयन की यह परम्परा रासककार को अपने पूर्ववर्ती साहित्य से विरासत के रूप में प्राप्त हुई । किन्तु, युग-चेता कवि अपनी मौलिक प्रतिभा तथा भव्यसृष्टि का सहज परिचय देता हुआ, पूर्व परम्परा को गतिशील बनाता है । यहाँ न तो संस्कृत-प्रबन्धों की भाँति आठ या अधिक सर्ग हैं और न अपभ्रंश-सदृश कड़वक तथा संधियों की योजना । बल्कि, 223 छन्द का यह रासक-काव्य तीन प्रक्रमों में विभक्त है । अस्तु, रास या रासौ काव्य-विधा के विकास में इसके मूल्यवान महत्त्व और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता ।
प्रथम प्रक्रम में रासककार अपनी पूर्ववर्ती प्रबंध-प्रणयन की परम्परा के निर्वाह हेतु सभी कवि एवं विदग्धों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता हुआ, अपनी कविता के संबंध में गहन आस्था व्यक्त करता