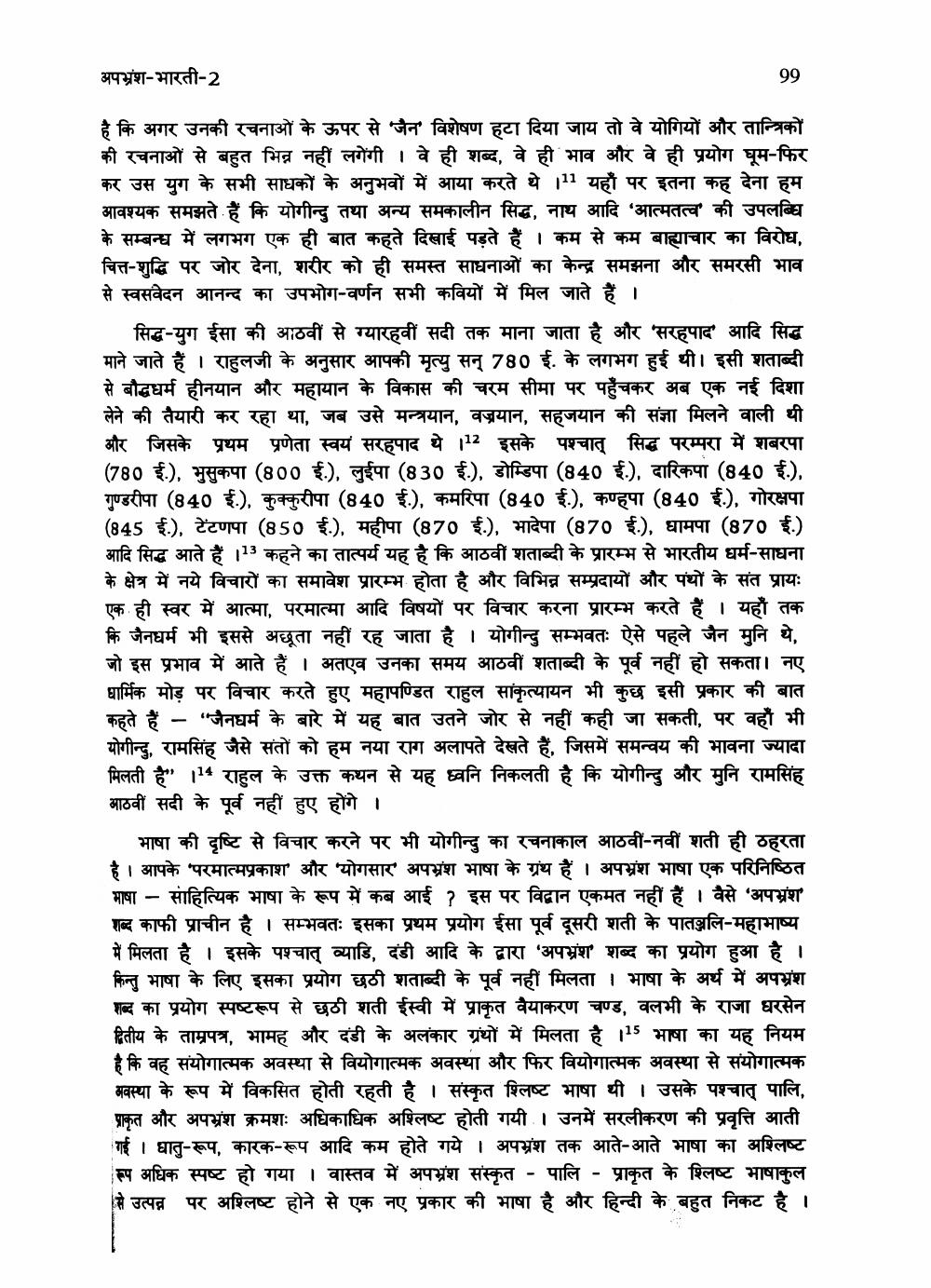________________
अपभ्रंश भारती-2
है कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से 'जैन' विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियों और तान्त्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी । वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम-फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभवों में आया करते थे । यहाँ पर इतना कह देना हम आवश्यक समझते हैं कि योगीन्दु तथा अन्य समकालीन सिद्ध, नाथ आदि 'आत्मतत्व' की उपलब्धि के सम्बन्ध में लगभग एक ही बात कहते दिखाई पड़ते हैं । कम से कम बाह्याचार का विरोध, चित्त शुद्धि पर जोर देना, शरीर को ही समस्त साधनाओं का केन्द्र समझना और समरसी भाव से स्वसंवेदन आनन्द का उपभोग वर्णन सभी कवियों में मिल जाते हैं ।
सिद्ध युग ईसा की आठवीं से ग्यारहवीं सदी तक माना जाता है और 'सरहपाद' आदि सिद्ध
-
माने जाते हैं । राहुलजी के अनुसार आपकी मृत्यु सन् 780 ई. के लगभग हुई थी। इसी शताब्दी से बौद्धधर्म हीनयान और महायान के विकास की चरम सीमा पर पहुँचकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मन्त्रयान, वज्रयान, सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी और जिसके प्रथम प्रणेता स्वयं सरहपाद थे । 12 इसके पश्चात् सिद्ध परम्परा में शबरपा (780 ई.), भुसुकपा (800 ई.), लुईपा (830 ई.), डोम्डिपा (840 ई.), दारिकपा ( 840 ई.), गुण्डरीपा (840 ई.), कुक्कुरीपा (840 ई.), कमरिपा ( 840 ई.), कण्हपा (840 ई.), गोरक्षपा (845 ई.), टेंटणपा (850 ई.), महीपा ( 870 ई.), भावेपा ( 870 ई.), धामपा (870 ई.) आदि सिद्ध आते हैं । 13 कहने का तात्पर्य यह है कि आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ से भारतीय धर्म-साधना के क्षेत्र में नये विचारों का समावेश प्रारम्भ होता है और विभिन्न सम्प्रदायों और पंथों के संत प्रायः एक ही स्वर में आत्मा परमात्मा आदि विषयों पर विचार करना प्रारम्भ करते हैं । यहाँ तक कि जैनधर्म भी इससे अछूता नहीं रह जाता है । योगीन्दु सम्भवतः ऐसे पहले जैन मुनि थे, जो इस प्रभाव में आते हैं । अतएव उनका समय आठवीं शताब्दी के पूर्व नहीं हो सकता। नए धार्मिक मोड़ पर विचार करते हुए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन भी कुछ इसी प्रकार की बात कहते हैं "जैनधर्म के बारे में यह बात उतने जोर से नहीं कही जा सकती, पर वहाँ भी योगीन्दु रामसिंह जैसे संतों को हम नया राग अलापते देखते हैं, जिसमें समन्वय की भावना ज्यादा मिलती है" 124 राहुल के उक्त कथन से यह ध्वनि निकलती है कि योगीन्दु और मुनि रामसिंह आठवीं सदी के पूर्व नहीं हुए होंगे ।
।
—
-
99
भाषा की दृष्टि से विचार करने पर भी योगीन्दु का रचनाकाल आठवीं नवीं शती ही ठहरता है। आपके 'परमात्मप्रकाश' और 'योगसार' अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ हैं। अपभ्रंश भाषा एक परिनिष्ठित भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में कब आई ? इस पर विद्वान एकमत नहीं हैं । वैसे 'अपभ्रंश' शब्द काफी प्राचीन है । सम्भवतः इसका प्रथम प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी शती के पातञ्जलि - महाभाष्य में मिलता है । इसके पश्चात् व्याडि, दंडी आदि के द्वारा 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग हुआ है । किन्तु भाषा के लिए इसका प्रयोग छठी शताब्दी के पूर्व नहीं मिलता। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग स्पष्टरूप से छठी शती ईस्वी में प्राकृत वैयाकरण चण्ड, वलभी के राजा धरसेन द्वितीय के ताम्रपत्र, भामह और दंडी के अलंकार ग्रंथों में मिलता है । 15 भाषा का यह नियम है कि वह संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था और फिर वियोगात्मक अवस्था से संयोगात्मक अवस्था के रूप में विकसित होती रहती है । संस्कृत श्लिष्ट भाषा थी । उसके पश्चात् पालि, प्राकृत और अपभ्रंश क्रमशः अधिकाधिक अश्लिष्ट होती गयी। उनमें सरलीकरण की प्रवृत्ति आती गई। धातु रूप, कारक रूप आदि कम होते गये। अपभ्रंश तक आते आते भाषा का अश्लिष्ट रूप अधिक स्पष्ट हो गया । वास्तव में अपभ्रंश संस्कृत पालि प्राकृत के श्लिष्ट भाषाकुल से उत्पन्न पर अश्लिष्ट होने से एक नए प्रकार की भाषा है और हिन्दी के बहुत निकट है ।
-
-