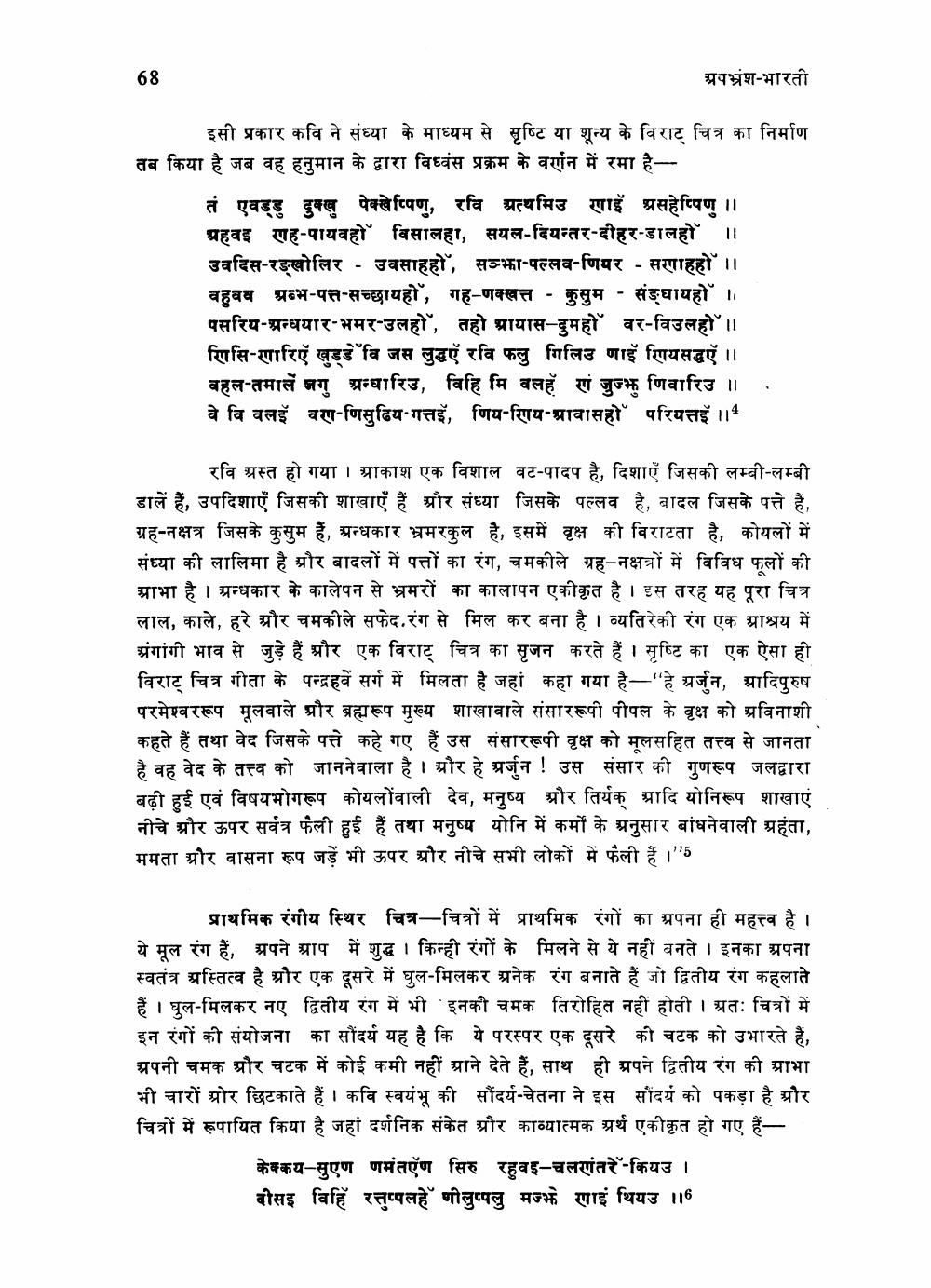________________
68
अपभ्रंश-भारती
इसी प्रकार कवि ने संध्या के माध्यम से सृष्टि या शून्य के विराट चित्र का निर्माण तब किया है जब वह हनुमान के द्वारा विध्वंस प्रक्रम के वर्णन में रमा है
तं एवड्डु दुक्खु पेक्षेप्पिणु, रवि अत्यमिउ पाइँ असहेप्पिणु ।। अहवइ गह-पायवहाँ विसालहा, सयल-दियन्तर-दीहर-डालहों ॥ उवदिस-रङ्खोलिर - उवसाहहों, सञ्झा-पल्लव-णियर - सरणाहहों ।। वहुवव अब्भ-पत्त-सच्छायहों, गह-णक्खत्त - कुसुम - संङ्घायहाँ ।। पसरिय-अन्धयार-भमर-उलहों, तहो प्रायास-दुमहों वर-विउलहों ।। णिसि-पारिऍ खुड्डेवि जस लुद्धएँ रवि फलु गिलिउ गाइ रिणयसद्धएँ । वहल-तमाले जगु अन्धारिउ, विहि मि वलहें एं जुज्झु णिवारिउ ॥ . वे वि वलइँ वरण-णिसुढिय गत्त, णिय-रिणय-प्रावासहों परियत्त ।।
रवि अस्त हो गया । अाकाश एक विशाल वट-पादप है, दिशाएँ जिसकी लम्बी-लम्बी डालें हैं, उपदिशाएँ जिसकी शाखाएँ हैं और संध्या जिसके पल्लव है, बादल जिसके पत्ते हैं, ग्रह-नक्षत्र जिसके कुसुम हैं, अन्धकार भ्रमरकुल है, इसमें वृक्ष की विराटता है, कोयलों में संध्या की लालिमा है और बादलों में पत्तों का रंग, चमकीले ग्रह-नक्षत्रों में विविध फूलों की आभा है। अन्धकार के कालेपन से भ्रमरों का कालापन एकीकृत है । इस तरह यह पूरा चित्र लाल, काले, हरे और चमकीले सफेद.रंग से मिल कर बना है । व्यतिरेकी रंग एक आश्रय में अंगांगी भाव से जुड़े हैं और एक विराट चित्र का सृजन करते हैं । सृष्टि का एक ऐसा ही विराट चित्र गीता के पन्द्रहवें सर्ग में मिलता है जहां कहा गया है—"हे अर्जुन, आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले और ब्रह्मरूप मुख्य शाखावाले संसाररूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसाररूपी वृक्ष को मूलसहित तत्त्व से जानता है वह वेद के तत्त्व को जाननेवाला है । और हे अर्जुन ! उस संसार की गुणरूप जलद्वारा बढी हई एवं विषयभोगरूप कोयलोंवाली देव, मनुष्य और तिर्यक प्रादि योनिरूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधनेवाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी ऊपर और नीचे सभी लोकों में फैली हैं।''5
प्राथमिक रंगीय स्थिर चित्र-चित्रों में प्राथमिक रंगों का अपना ही महत्त्व है । ये मूल रंग हैं, अपने आप में शुद्ध । किन्ही रंगों के मिलने से ये नहीं बनते । इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और एक दूसरे में घुल-मिलकर अनेक रंग बनाते हैं जो द्वितीय रंग कहलाते हैं । घुल-मिलकर नए द्वितीय रंग में भी इनकी चमक तिरोहित नहीं होती । अतः चित्रों में इन रंगों की संयोजना का सौंदर्य यह है कि ये परस्पर एक दूसरे की चटक को उभारते हैं, अपनी चमक और चटक में कोई कमी नहीं आने देते हैं, साथ ही अपने द्वितीय रंग की प्राभा भी चारों ओर छिटकाते हैं । कवि स्वयंभू की सौंदर्य-चेतना ने इस सौंदर्य को पकड़ा है और चित्रों में रूपायित किया है जहां दर्शनिक संकेत और काव्यात्मक अर्थ एकीकृत हो गए हैं
केक्कय-सुएण णमंतऍण सिरु रहुवइ-चलणंतरें-कियउ । वोसइ विहिं रत्तुप्पलहें गोलुप्पलु मज्झे गाई थियउ ।