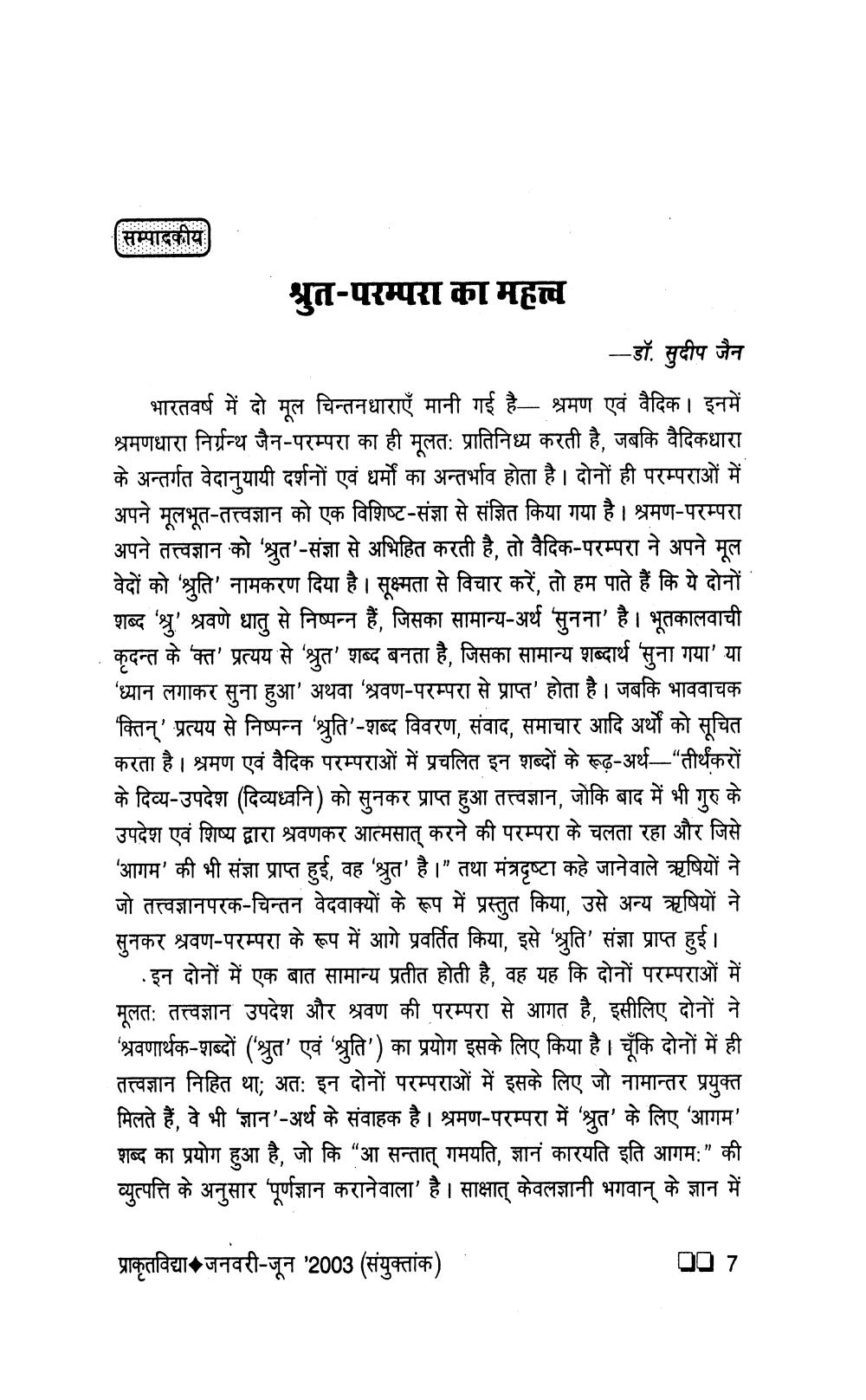________________
[सम्पादकीय
श्रुत-परम्परा का महत्व
-डॉ. सुदीप जैन भारतवर्ष में दो मूल चिन्तनधाराएँ मानी गई है— श्रमण एवं वैदिक। इनमें श्रमणधारा निर्ग्रन्थ जैन-परम्परा का ही मूलत: प्रातिनिध्य करती है, जबकि वैदिकधारा के अन्तर्गत वेदानुयायी दर्शनों एवं धर्मों का अन्तर्भाव होता है। दोनों ही परम्पराओं में अपने मूलभूत-तत्त्वज्ञान को एक विशिष्ट-संज्ञा से संज्ञित किया गया है। श्रमण-परम्परा अपने तत्त्वज्ञान को 'श्रुत'-संज्ञा से अभिहित करती है, तो वैदिक-परम्परा ने अपने मूल वेदों को 'श्रुति' नामकरण दिया है। सूक्ष्मता से विचार करें, तो हम पाते हैं कि ये दोनों शब्द 'श्रु' श्रवणे धातु से निष्पन्न हैं, जिसका सामान्य-अर्थ 'सुनना' है। भूतकालवाची कृदन्त के 'क्त' प्रत्यय से 'श्रुत' शब्द बनता है, जिसका सामान्य शब्दार्थ 'सुना गया' या 'ध्यान लगाकर सुना हुआ' अथवा 'श्रवण-परम्परा से प्राप्त' होता है। जबकि भाववाचक 'क्तिन्' प्रत्यय से निष्पन्न 'श्रुति'-शब्द विवरण, संवाद, समाचार आदि अर्थों को सूचित करता है। श्रमण एवं वैदिक परम्पराओं में प्रचलित इन शब्दों के रूढ़-अर्थ-“तीर्थंकरों के दिव्य-उपदेश (दिव्यध्वनि) को सुनकर प्राप्त हुआ तत्त्वज्ञान, जोकि बाद में भी गुरु के उपदेश एवं शिष्य द्वारा श्रवणकर आत्मसात् करने की परम्परा के चलता रहा और जिसे 'आगम' की भी संज्ञा प्राप्त हुई, वह 'श्रुत' है।" तथा मंत्रदृष्टा कहे जानेवाले ऋषियों ने जो तत्त्वज्ञानपरक-चिन्तन वेदवाक्यों के रूप में प्रस्तुत किया, उसे अन्य ऋषियों ने सुनकर श्रवण-परम्परा के रूप में आगे प्रवर्तित किया, इसे 'श्रुति' संज्ञा प्राप्त हुई।
. इन दोनों में एक बात सामान्य प्रतीत होती है, वह यह कि दोनों परम्पराओं में मूलत: तत्त्वज्ञान उपदेश और श्रवण की परम्परा से आगत है, इसीलिए दोनों ने 'श्रवणार्थक-शब्दों ('श्रुत' एवं 'श्रुति') का प्रयोग इसके लिए किया है। चूंकि दोनों में ही तत्त्वज्ञान निहित था; अत: इन दोनों परम्पराओं में इसके लिए जो नामान्तर प्रयुक्त मिलते हैं, वे भी 'ज्ञान'-अर्थ के संवाहक है। श्रमण-परम्परा में 'श्रुत' के लिए 'आगम' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि “आ सन्तात् गमयति, ज्ञानं कारयति इति आगम:” की व्युत्पत्ति के अनुसार 'पूर्णज्ञान करानेवाला' है। साक्षात् केवलज्ञानी भगवान् के ज्ञान में
प्राकृतविद्या जनवरी-जून '2003 (संयुक्तांक)
007