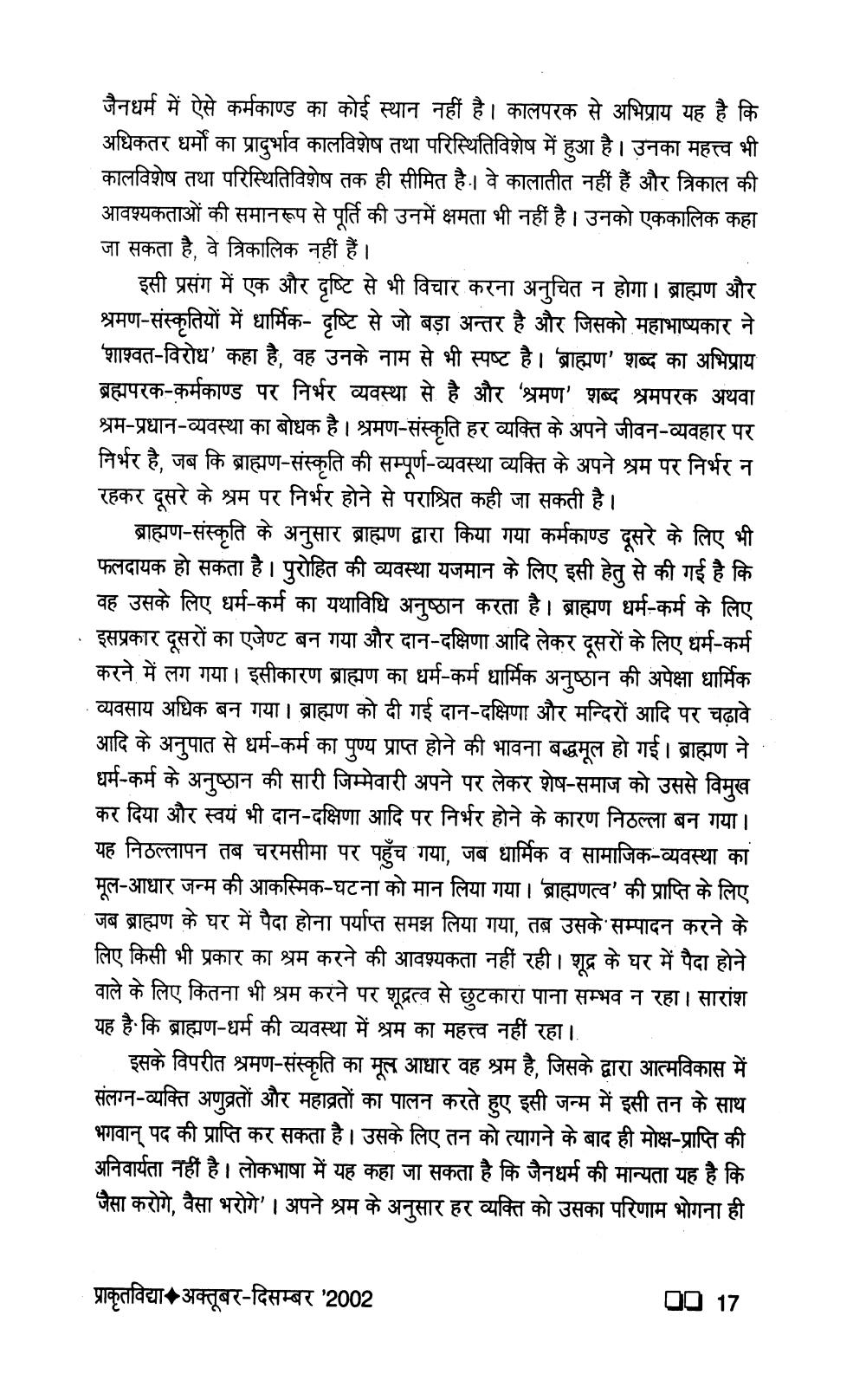________________
जैनधर्म में ऐसे कर्मकाण्ड का कोई स्थान नहीं है। कालपरक से अभिप्राय यह है कि अधिकतर धर्मों का प्रादुर्भाव कालविशेष तथा परिस्थितिविशेष में हुआ है। उनका महत्त्व भी कालविशेष तथा परिस्थितिविशेष तक ही सीमित है। वे कालातीत नहीं हैं और त्रिकाल की आवश्यकताओं की समानरूप से पूर्ति की उनमें क्षमता भी नहीं है। उनको एककालिक कहा जा सकता है, वे त्रिकालिक नहीं हैं।
इसी प्रसंग में एक और दृष्टि से भी विचार करना अनुचित न होगा। ब्राह्मण और श्रमण-संस्कृतियों में धार्मिक- दृष्टि से जो बड़ा अन्तर है और जिसको महाभाष्यकार ने 'शाश्वत-विरोध' कहा है, वह उनके नाम से भी स्पष्ट है। 'ब्राह्मण' शब्द का अभिप्राय ब्रह्मपरक-कर्मकाण्ड पर निर्भर व्यवस्था से है और 'श्रमण' शब्द श्रमपरक अथवा श्रम-प्रधान-व्यवस्था का बोधक है। श्रमण-संस्कृति हर व्यक्ति के अपने जीवन-व्यवहार पर निर्भर है, जब कि ब्राह्मण-संस्कृति की सम्पूर्ण-व्यवस्था व्यक्ति के अपने श्रम पर निर्भर न रहकर दूसरे के श्रम पर निर्भर होने से पराश्रित कही जा सकती है।
ब्राह्मण-संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण द्वारा किया गया कर्मकाण्ड दूसरे के लिए भी फलदायक हो सकता है। पुरोहित की व्यवस्था यजमान के लिए इसी हेतु से की गई है कि वह उसके लिए धर्म-कर्म का यथाविधि अनुष्ठान करता है। ब्राह्मण धर्म-कर्म के लिए इसप्रकार दूसरों का एजेण्ट बन गया और दान-दक्षिणा आदि लेकर दूसरों के लिए धर्म-कर्म करने में लग गया। इसीकारण ब्राह्मण का धर्म-कर्म धार्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा धार्मिक व्यवसाय अधिक बन गया। ब्राह्मण को दी गई दान-दक्षिणा और मन्दिरों आदि पर चढ़ावे आदि के अनुपात से धर्म-कर्म का पुण्य प्राप्त होने की भावना बद्धमूल हो गई। ब्राह्मण ने धर्म-कर्म के अनुष्ठान की सारी जिम्मेवारी अपने पर लेकर शेष-समाज को उससे विमुख कर दिया और स्वयं भी दान-दक्षिणा आदि पर निर्भर होने के कारण निठल्ला बन गया। यह निठल्लापन तब चरमसीमा पर पहुँच गया, जब धार्मिक व सामाजिक-व्यवस्था का मूल-आधार जन्म की आकस्मिक-घटना को मान लिया गया। 'ब्राह्मणत्व' की प्राप्ति के लिए जब ब्राह्मण के घर में पैदा होना पर्याप्त समझ लिया गया, तब उसके सम्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार का श्रम करने की आवश्यकता नहीं रही। शूद्र के घर में पैदा होने वाले के लिए कितना भी श्रम करने पर शूद्रत्व से छुटकारा पाना सम्भव न रहा। सारांश यह है कि ब्राह्मण-धर्म की व्यवस्था में श्रम का महत्त्व नहीं रहा। ___ इसके विपरीत श्रमण-संस्कृति का मूल आधार वह श्रम है, जिसके द्वारा आत्मविकास में संलग्न-व्यक्ति अणुव्रतों और महाव्रतों का पालन करते हुए इसी जन्म में इसी तन के साथ भगवान् पद की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए तन को त्यागने के बाद ही मोक्ष-प्राप्ति की अनिवार्यता नहीं है। लोकभाषा में यह कहा जा सकता है कि जैनधर्म की मान्यता यह है कि 'जैसा करोगे, वैसा भरोगे'। अपने श्रम के अनुसार हर व्यक्ति को उसका परिणाम भोगना ही
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2002
10 17