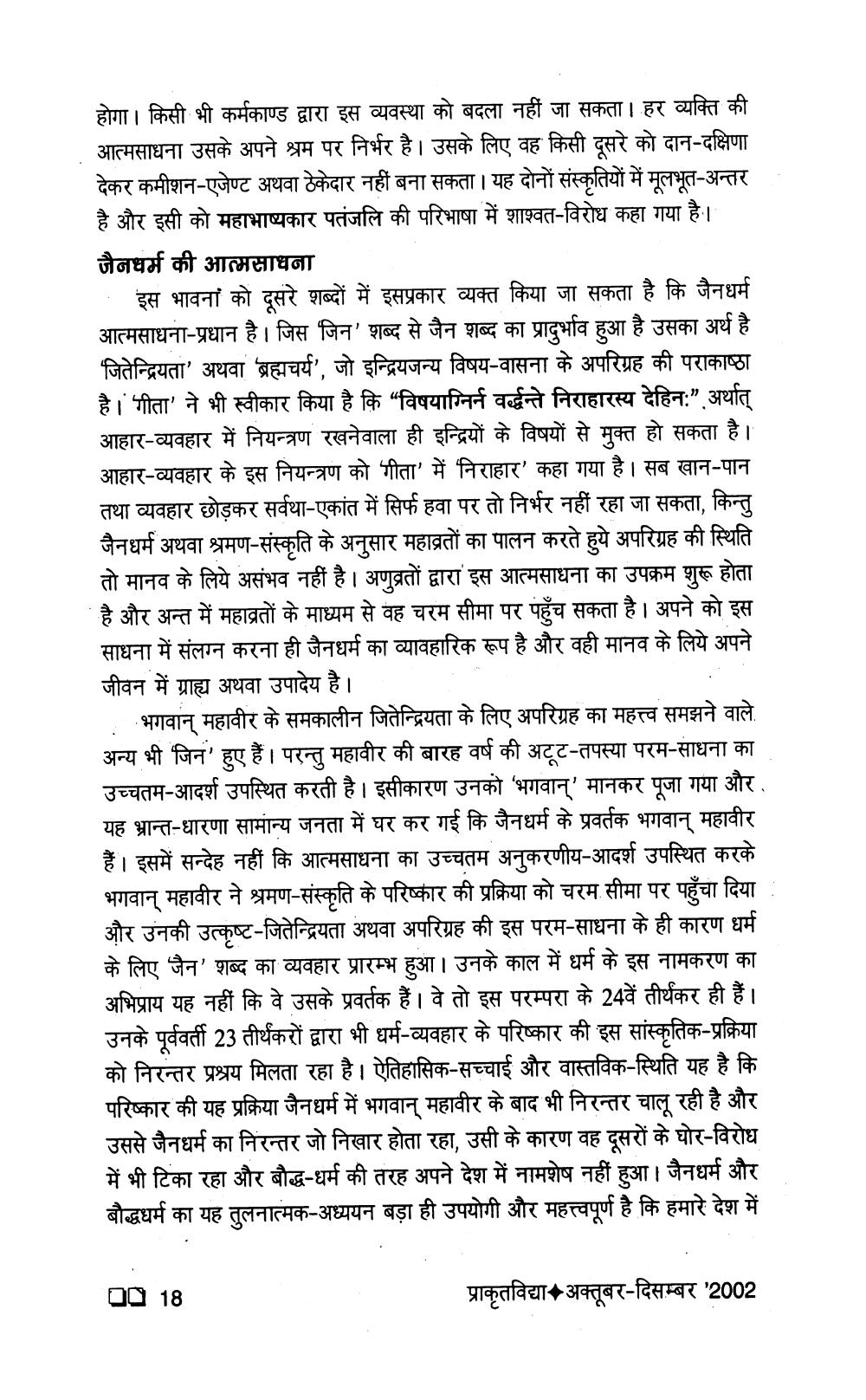________________
होगा। किसी भी कर्मकाण्ड द्वारा इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। हर व्यक्ति की आत्मसाधना उसके अपने श्रम पर निर्भर है। उसके लिए वह किसी दूसरे को दान-दक्षिणा देकर कमीशन-एजेण्ट अथवा ठेकेदार नहीं बना सकता। यह दोनों संस्कृतियों में मूलभूत-अन्तर है और इसी को महाभाष्यकार पतंजलि की परिभाषा में शाश्वत-विरोध कहा गया है। जैनधर्म की आत्मसाधना . इस भावना को दूसरे शब्दों में इसप्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि जैनधर्म आत्मसाधना-प्रधान है। जिस 'जिन' शब्द से जैन शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है उसका अर्थ है 'जितेन्द्रियता' अथवा 'ब्रह्मचर्य', जो इन्द्रियजन्य विषय-वासना के अपरिग्रह की पराकाष्ठा है। 'गीता' ने भी स्वीकार किया है कि “विषयाग्निर्न वर्द्धन्ते निराहारस्य देहिनः” अर्थात् आहार-व्यवहार में नियन्त्रण रखनेवाला ही इन्द्रियों के विषयों से मुक्त हो सकता है। आहार-व्यवहार के इस नियन्त्रण को 'गीता' में 'निराहार' कहा गया है। सब खान-पान तथा व्यवहार छोड़कर सर्वथा-एकांत में सिर्फ हवा पर तो निर्भर नहीं रहा जा सकता, किन्तु जैनधर्म अथवा श्रमण-संस्कृति के अनुसार महाव्रतों का पालन करते हुये अपरिग्रह की स्थिति तो मानव के लिये असंभव नहीं है। अणुव्रतों द्वारा इस आत्मसाधना का उपक्रम शुरू होता है और अन्त में महाव्रतों के माध्यम से वह चरम सीमा पर पहुँच सकता है। अपने को इस साधना में संलग्न करना ही जैनधर्म का व्यावहारिक रूप है और वही मानव के लिये अपने जीवन में ग्राह्य अथवा उपादेय है। . भगवान् महावीर के समकालीन जितेन्द्रियता के लिए अपरिग्रह का महत्त्व समझने वाले अन्य भी 'जिन' हुए हैं। परन्तु महावीर की बारह वर्ष की अटूट-तपस्या परम-साधना का उच्चतम-आदर्श उपस्थित करती है। इसीकारण उनको 'भगवान्' मानकर पूजा गया और यह भ्रान्त-धारणा सामान्य जनता में घर कर गई कि जैनधर्म के प्रवर्तक भगवान् महावीर हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आत्मसाधना का उच्चतम अनुकरणीय-आदर्श उपस्थित करके भगवान् महावीर ने श्रमण-संस्कृति के परिष्कार की प्रक्रिया को चरम सीमा पर पहुँचा दिया और उनकी उत्कृष्ट-जितेन्द्रियता अथवा अपरिग्रह की इस परम-साधना के ही कारण धर्म के लिए जैन' शब्द का व्यवहार प्रारम्भ हुआ। उनके काल में धर्म के इस नामकरण का अभिप्राय यह नहीं कि वे उसके प्रवर्तक हैं। वे तो इस परम्परा के 24वें तीर्थंकर ही हैं। उनके पूर्ववर्ती 23 तीर्थंकरों द्वारा भी धर्म-व्यवहार के परिष्कार की इस सांस्कृतिक-प्रक्रिया को निरन्तर प्रश्रय मिलता रहा है। ऐतिहासिक-सच्चाई और वास्तविक स्थिति यह है कि परिष्कार की यह प्रक्रिया जैनधर्म में भगवान् महावीर के बाद भी निरन्तर चालू रही है और उससे जैनधर्म का निरन्तर जो निखार होता रहा, उसी के कारण वह दूसरों के घोर-विरोध में भी टिका रहा और बौद्ध-धर्म की तरह अपने देश में नामशेष नहीं हुआ। जैनधर्म और बौद्धधर्म का यह तुलनात्मक-अध्ययन बड़ा ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है कि हमारे देश में
10 18
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2002