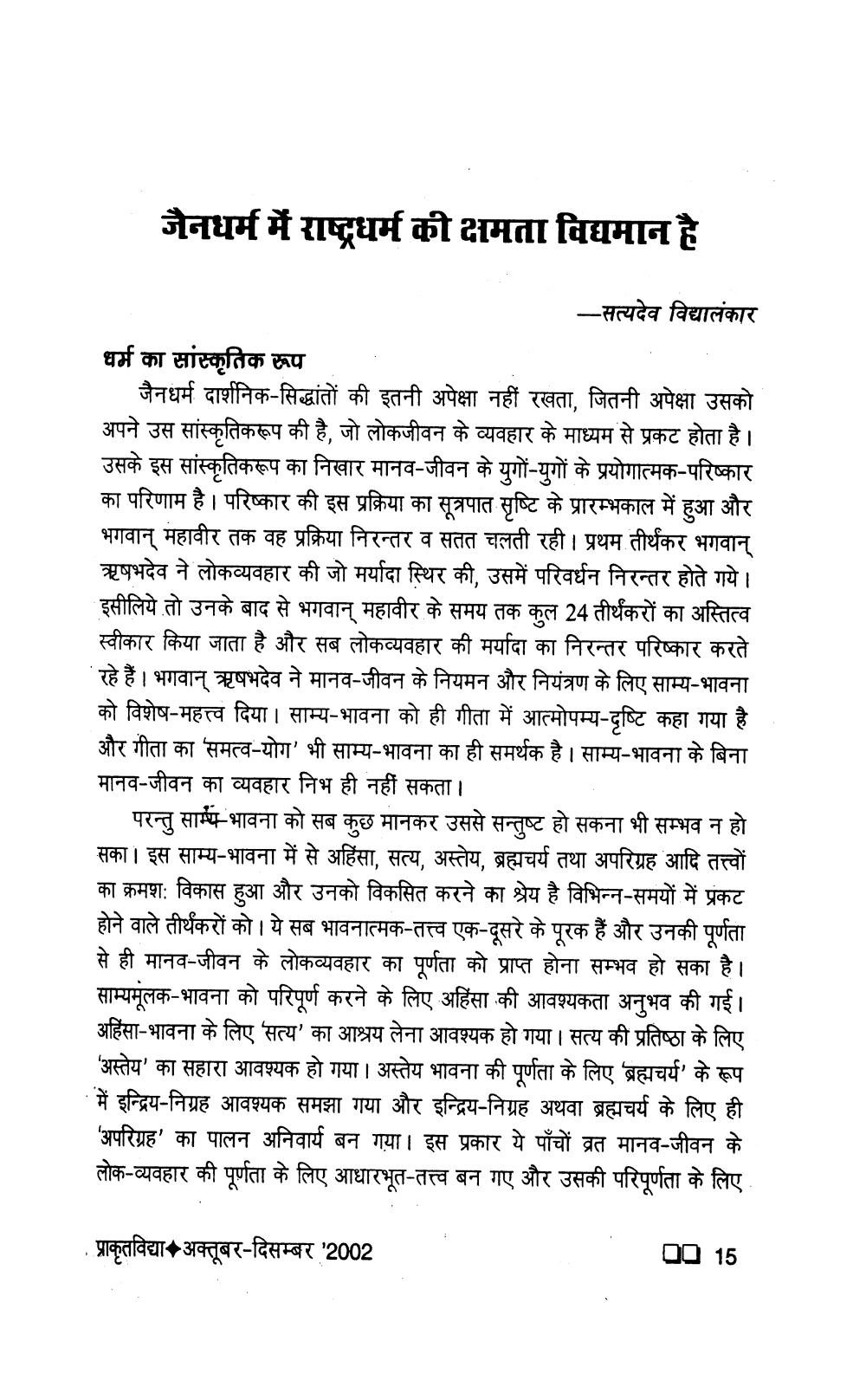________________
जैनधर्म में राष्ट्रधर्म की क्षमता विद्यमान है
-सत्यदेव विद्यालंकार
धर्म का सांस्कृतिक रूप
जैनधर्म दार्शनिक-सिद्धांतों की इतनी अपेक्षा नहीं रखता, जितनी अपेक्षा उसको अपने उस सांस्कृतिकरूप की है, जो लोकजीवन के व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है। उसके इस सांस्कृतिकरूप का निखार मानव-जीवन के युगों-युगों के प्रयोगात्मक-परिष्कार का परिणाम है। परिष्कार की इस प्रक्रिया का सूत्रपात सृष्टि के प्रारम्भकाल में हुआ और भगवान् महावीर तक वह प्रक्रिया निरन्तर व सतत चलती रही। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने लोकव्यवहार की जो मर्यादा स्थिर की, उसमें परिवर्धन निरन्तर होते गये। इसीलिये तो उनके बाद से भगवान् महावीर के समय तक कुल 24 तीर्थंकरों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और सब लोकव्यवहार की मर्यादा का निरन्तर परिष्कार करते रहे हैं। भगवान् ऋषभदेव ने मानव-जीवन के नियमन और नियंत्रण के लिए साम्य-भावना को विशेष महत्त्व दिया। साम्य-भावना को ही गीता में आत्मोपम्य-दृष्टि कहा गया है और गीता का समत्व-योग' भी साम्य-भावना का ही समर्थक है। साम्य-भावना के बिना मानव-जीवन का व्यवहार निभ ही नहीं सकता। ___ परन्तु साम्य भावना को सब कुछ मानकर उससे सन्तुष्ट हो सकना भी सम्भव न हो सका। इस साम्य-भावना में से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि तत्त्वों का क्रमश: विकास हुआ और उनको विकसित करने का श्रेय है विभिन्न-समयों में प्रकट होने वाले तीर्थंकरों को। ये सब भावनात्मक-तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं और उनकी पूर्णता से ही मानव-जीवन के लोकव्यवहार का पूर्णता को प्राप्त होना सम्भव हो सका है। साम्यमूलक-भावना को परिपूर्ण करने के लिए अहिंसा की आवश्यकता अनुभव की गई। अहिंसा-भावना के लिए 'सत्य' का आश्रय लेना आवश्यक हो गया। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 'अस्तेय' का सहारा आवश्यक हो गया। अस्तेय भावना की पूर्णता के लिए 'ब्रह्मचर्य' के रूप में इन्द्रिय-निग्रह आवश्यक समझा गया और इन्द्रिय-निग्रह अथवा ब्रह्मचर्य के लिए ही 'अपरिग्रह' का पालन अनिवार्य बन गया। इस प्रकार ये पाँचों व्रत मानव-जीवन के लोक-व्यवहार की पूर्णता के लिए आधारभूत-तत्त्व बन गए और उसकी परिपूर्णता के लिए
. प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2002
00 15