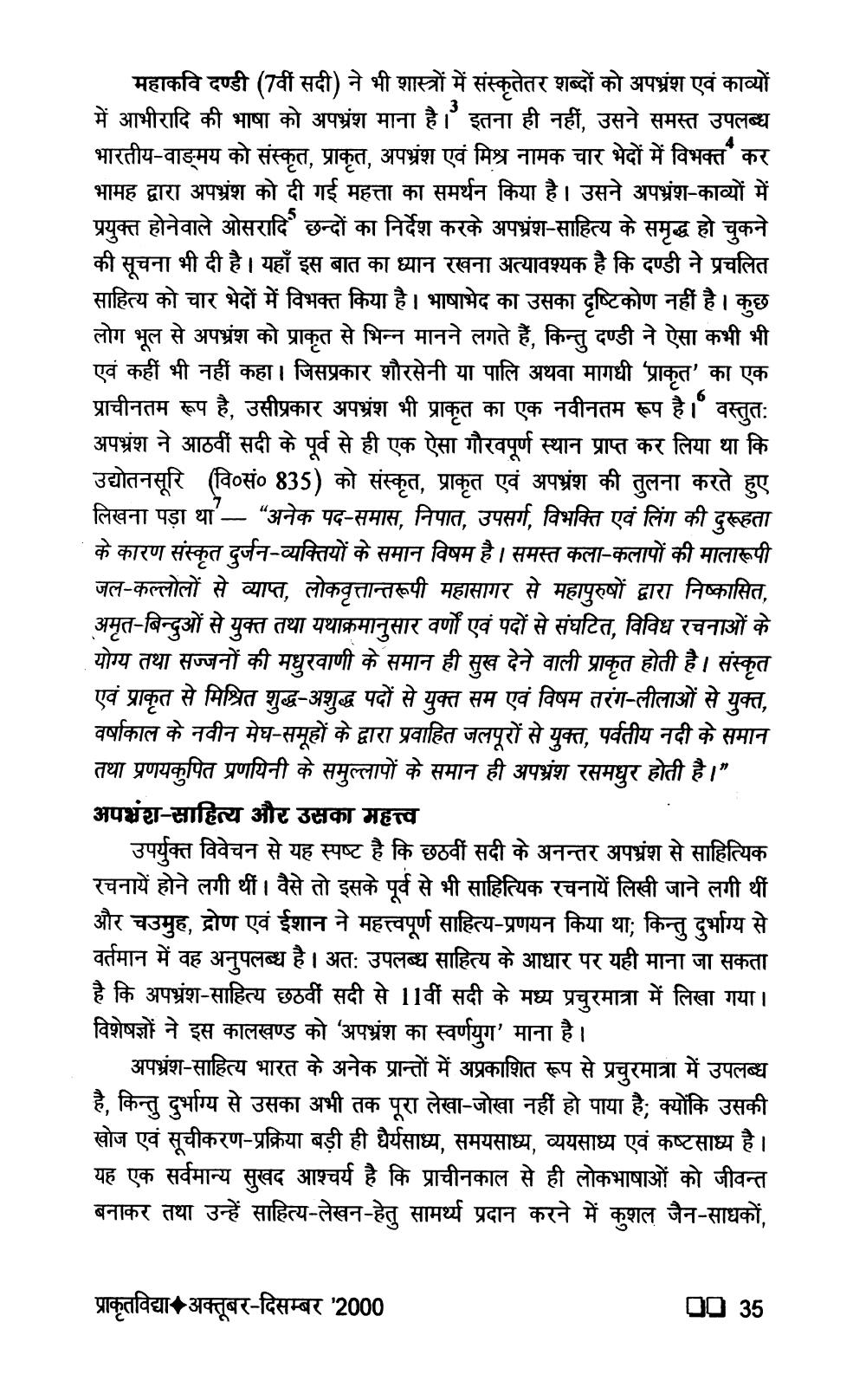________________
महाकवि दण्डी (7वीं सदी) ने भी शास्त्रों में संस्कृतेतर शब्दों को अपभ्रंश एवं काव्यों में आभीरादि की भाषा को अपभ्रंश माना है। इतना ही नहीं, उसने समस्त उपलब्ध भारतीय-वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मिश्र नामक चार भेदों में विभक्त कर भामह द्वारा अपभ्रंश को दी गई महत्ता का समर्थन किया है। उसने अपभ्रंश-काव्यों में प्रयुक्त होनेवाले ओसरादि छन्दों का निर्देश करके अपभ्रंश-साहित्य के समृद्ध हो चुकने की सूचना भी दी है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि दण्डी ने प्रचलित साहित्य को चार भेदों में विभक्त किया है। भाषाभेद का उसका दृष्टिकोण नहीं है। कुछ लोग भूल से अपभ्रंश को प्राकृत से भिन्न मानने लगते हैं, किन्तु दण्डी ने ऐसा कभी भी एवं कहीं भी नहीं कहा। जिसप्रकार शौरसेनी या पालि अथवा मागधी 'प्राकृत' का एक प्राचीनतम रूप है, उसीप्रकार अपभ्रंश भी प्राकृत का एक नवीनतम रूप है। वस्तुत: अपभ्रंश ने आठवीं सदी के पूर्व से ही एक ऐसा गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था कि उद्योतनसूरि (वि०सं० 835) को संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की तुलना करते हुए लिखना पड़ा था- “अनेक पद-समास, निपात, उपसर्ग, विभक्ति एवं लिंग की दुरूहता के कारण संस्कृत दुर्जन-व्यक्तियों के समान विषम है। समस्त कला-कलापों की मालारूपी जल-कल्लोलों से व्याप्त, लोकवृत्तान्तरूपी महासागर से महापुरुषों द्वारा निष्कासित, अमृत-बिन्दुओं से युक्त तथा यथाक्रमानुसार वर्णों एवं पदों से संघटित, विविध रचनाओं के योग्य तथा सज्जनों की मधुरवाणी के समान ही सुख देने वाली प्राकृत होती है। संस्कृत एवं प्राकृत से मिश्रित शुद्ध-अशुद्ध पदों से युक्त सम एवं विषम तरंग-लीलाओं से युक्त, वर्षाकाल के नवीन मेघ-समूहों के द्वारा प्रवाहित जलपूरों से युक्त, पर्वतीय नदी के समान तथा प्रणयकुपित प्रणयिनी के समुल्लापों के समान ही अपभ्रंश रसमधुर होती है।" अपभ्रंश-साहित्य और उसका महत्त्व
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छठवीं सदी के अनन्तर अपभ्रंश से साहित्यिक रचनायें होने लगी थीं। वैसे तो इसके पूर्व से भी साहित्यिक रचनायें लिखी जाने लगी थीं
और चउमुह, द्रोण एवं ईशान ने महत्त्वपूर्ण साहित्य-प्रणयन किया था; किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में वह अनुपलब्ध है। अत: उपलब्ध साहित्य के आधार पर यही माना जा सकता है कि अपभ्रंश-साहित्य छठवीं सदी से 11वीं सदी के मध्य प्रचुरमात्रा में लिखा गया। विशेषज्ञों ने इस कालखण्ड को 'अपभ्रंश का स्वर्णयुग' माना है।
__ अपभ्रंश-साहित्य भारत के अनेक प्रान्तों में अप्रकाशित रूप से प्रचुरमात्रा में उपलब्ध है, किन्तु दुर्भाग्य से उसका अभी तक पूरा लेखा-जोखा नहीं हो पाया है; क्योंकि उसकी खोज एवं सूचीकरण-प्रक्रिया बड़ी ही धैर्यसाध्य, समयसाध्य, व्ययसाध्य एवं कष्टसाध्य है। यह एक सर्वमान्य सुखद आश्चर्य है कि प्राचीनकाल से ही लोकभाषाओं को जीवन्त बनाकर तथा उन्हें साहित्य-लेखन-हेतु सामर्थ्य प्रदान करने में कुशल जैन-साधकों,
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000
00 35