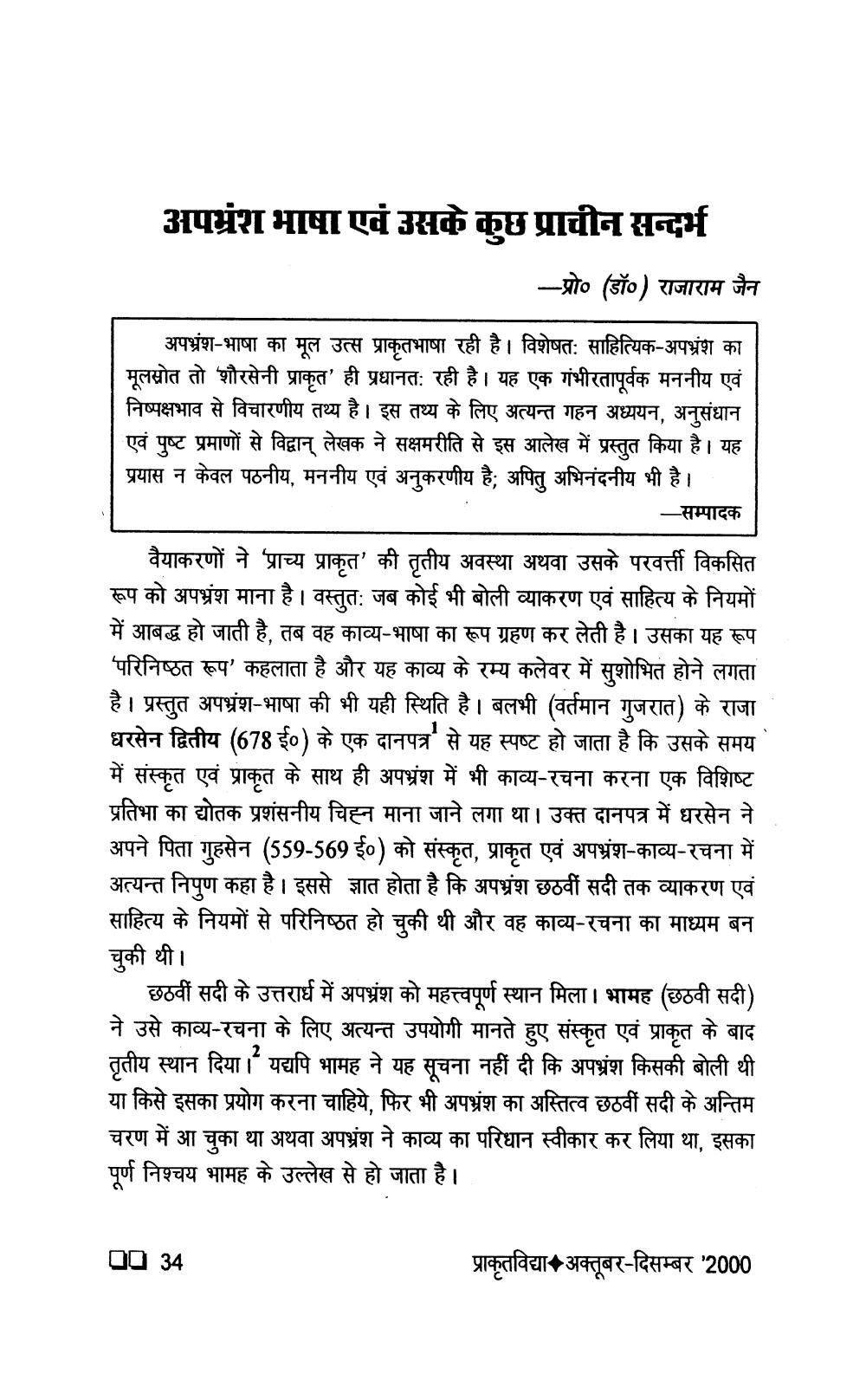________________
अपभ्रंश भाषा एवं उसके कुछ प्राचीन सन्दर्भ
-प्रो० (डॉ०) राजाराम जैन
अपभ्रंश-भाषा का मूल उत्स प्राकृतभाषा रही है। विशेषत: साहित्यिक-अपभ्रंश का मूलस्रोत तो शौरसेनी प्राकृत' ही प्रधानत: रही है। यह एक गंभीरतापूर्वक मननीय एवं निष्पक्षभाव से विचारणीय तथ्य है। इस तथ्य के लिए अत्यन्त गहन अध्ययन, अनुसंधान एवं पुष्ट प्रमाणों से विद्वान् लेखक ने सक्षमरीति से इस आलेख में प्रस्तुत किया है। यह प्रयास न केवल पठनीय, मननीय एवं अनुकरणीय है; अपितु अभिनंदनीय भी है।
–सम्पादक
वैयाकरणों ने 'प्राच्य प्राकृत' की तृतीय अवस्था अथवा उसके परवर्ती विकसित रूप को अपभ्रंश माना है। वस्तुत: जब कोई भी बोली व्याकरण एवं साहित्य के नियमों में आबद्ध हो जाती है, तब वह काव्य-भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। उसका यह रूप 'परिनिष्ठत रूप' कहलाता है और यह काव्य के रम्य कलेवर में सुशोभित होने लगता है। प्रस्तुत अपभ्रंश-भाषा की भी यही स्थिति है। बलभी (वर्तमान गुजरात) के राजा धरसेन द्वितीय (678 ई०) के एक दानपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके समय में संस्कृत एवं प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश में भी काव्य-रचना करना एक विशिष्ट प्रतिभा का द्योतक प्रशंसनीय चिह्न माना जाने लगा था। उक्त दानपत्र में धरसेन ने अपने पिता गुहसेन (559-569 ई०) को संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश-काव्य-रचना में अत्यन्त निपुण कहा है। इससे ज्ञात होता है कि अपभ्रंश छठवीं सदी तक व्याकरण एवं साहित्य के नियमों से परिनिष्ठत हो चुकी थी और वह काव्य-रचना का माध्यम बन चुकी थी। ___ छठवीं सदी के उत्तरार्ध में अपभ्रंश को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। भामह (छठवी सदी) ने उसे काव्य-रचना के लिए अत्यन्त उपयोगी मानते हुए संस्कृत एवं प्राकृत के बाद तृतीय स्थान दिया। यद्यपि भामह ने यह सूचना नहीं दी कि अपभ्रंश किसकी बोली थी या किसे इसका प्रयोग करना चाहिये, फिर भी अपभ्रंश का अस्तित्व छठवीं सदी के अन्तिम चरण में आ चुका था अथवा अपभ्रंश ने काव्य का परिधान स्वीकार कर लिया था, इसका पूर्ण निश्चय भामह के उल्लेख से हो जाता है।
40 34
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000