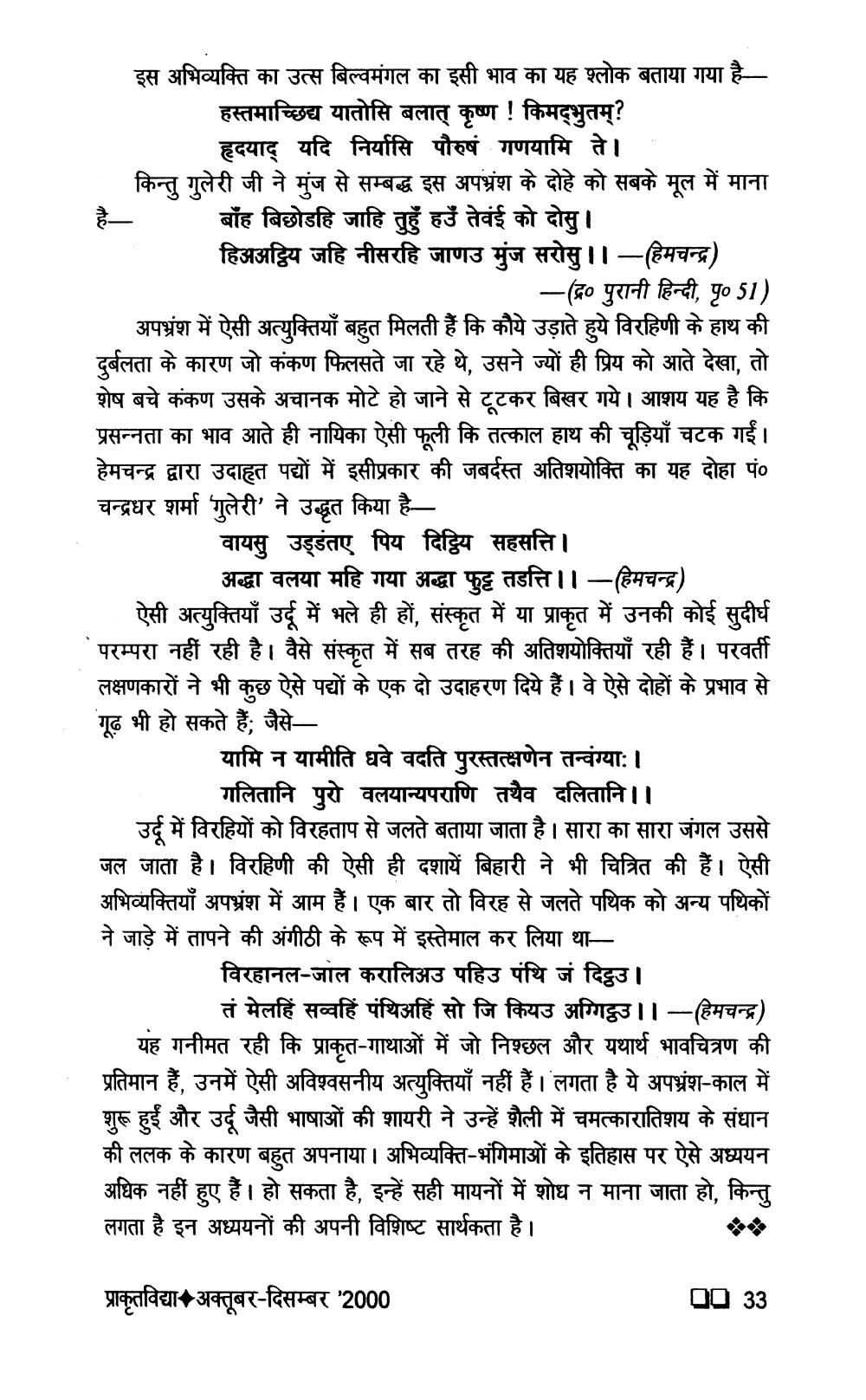________________
है
इस अभिव्यक्ति का उत्स बिल्वमंगल का इसी भाव का यह श्लोक बताया गया है
हस्तमाच्छिद्य यातोसि बलात् कृष्ण ! किमद्भुतम्?
हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। किन्तु गुलेरी जी ने मुंज से सम्बद्ध इस अपभ्रंश के दोहे को सबके मूल में माना
बाँह बिछोडहि जाहि तुहुँ हउँ तेवंई को दोसु। हिअअट्ठिय जहि नीसरहि जाणउ मुंज सरोसु ।। -हिमचन्द्र)
-(द्र० पुरानी हिन्दी, पृ0 51) अपभ्रंश में ऐसी अत्युक्तियाँ बहुत मिलती हैं कि कौये उड़ाते हुये विरहिणी के हाथ की दुर्बलता के कारण जो कंकण फिलसते जा रहे थे, उसने ज्यों ही प्रिय को आते देखा, तो शेष बचे कंकण उसके अचानक मोटे हो जाने से टूटकर बिखर गये। आशय यह है कि प्रसन्नता का भाव आते ही नायिका ऐसी फूली कि तत्काल हाथ की चूड़ियाँ चटक गईं। हेमचन्द्र द्वारा उदाहृत पद्यों में इसीप्रकार की जबर्दस्त अतिशयोक्ति का यह दोहा पं० चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने उद्धत किया है
वायसु उड्डतए पिय दिट्ठिय सहसत्ति।
अद्धा वलया महि गया अद्धा फुट्ट तडत्ति ।। -हिमचन्द्र) ऐसी अत्युक्तियाँ उर्दू में भले ही हों, संस्कृत में या प्राकृत में उनकी कोई सुदीर्घ परम्परा नहीं रही है। वैसे संस्कृत में सब तरह की अतिशयोक्तियाँ रही हैं। परवर्ती लक्षणकारों ने भी कुछ ऐसे पद्यों के एक दो उदाहरण दिये हैं। वे ऐसे दोहों के प्रभाव से गूढ़ भी हो सकते हैं; जैसे
यामि न यामीति धवे वदति पुरस्तत्क्षणेन तन्वंग्या: ।
गलितानि पुरो वलयान्यपराणि तथैव दलितानि।। उर्द में विरहियों को विरहताप से जलते बताया जाता है। सारा का सारा जंगल उससे जल जाता है। विरहिणी की ऐसी ही दशायें बिहारी ने भी चित्रित की हैं। ऐसी अभिव्यक्तियाँ अपभ्रंश में आम हैं। एक बार तो विरह से जलते पथिक को अन्य पथिकों ने जाड़े में तापने की अंगीठी के रूप में इस्तेमाल कर लिया था—
विरहानल-जाल करालिअउ पहिउ पंथि जं दिट्ठउ।
तं मेलहिं सवहिं पंथिअहिं सो जि कियउ अग्गिट्ठ।। -(हमचन्द्र) यह गनीमत रही कि प्राकृत-गाथाओं में जो निश्छल और यथार्थ भावचित्रण की प्रतिमान हैं, उनमें ऐसी अविश्वसनीय अत्युक्तियाँ नहीं हैं। लगता है ये अपभ्रंश-काल में शुरू हुईं और उर्दू जैसी भाषाओं की शायरी ने उन्हें शैली में चमत्कारातिशय के संधान की ललक के कारण बहुत अपनाया। अभिव्यक्ति-भंगिमाओं के इतिहास पर ऐसे अध्ययन अधिक नहीं हुए हैं। हो सकता है, इन्हें सही मायनों में शोध न माना जाता हो, किन्तु लगता है इन अध्ययनों की अपनी विशिष्ट सार्थकता है।
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर "2000
0033