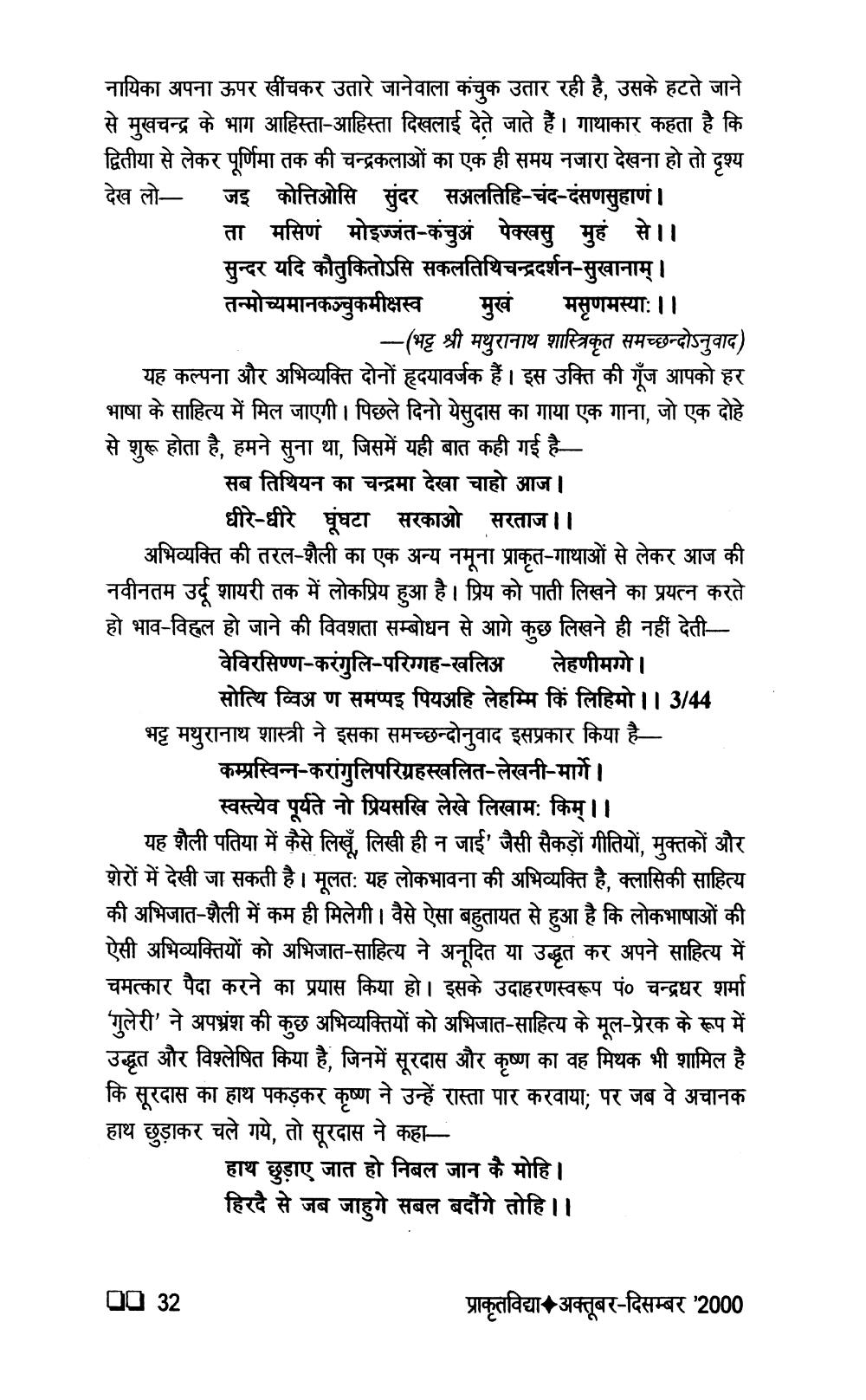________________
नायिका अपना ऊपर खींचकर उतारे जानेवाला कंचुक उतार रही है, उसके हटते जाने से मुखचन्द्र के भाग आहिस्ता-आहिस्ता दिखलाई देते जाते हैं। गाथाकार कहता है कि द्वितीया से लेकर पूर्णिमा तक की चन्द्रकलाओं का एक ही समय नजारा देखना हो तो दृश्य देख लो- जइ कोत्तिओसि सुंदर सअलतिहि-चंद-दसणसुहाणं।
ता मसिणं मोइज्जंत-कंचुअं पेक्खसु मुहं से।। सुन्दर यदि कौतुकितोऽसि सकलतिथिचन्द्रदर्शन-सुखानाम् । तन्मोच्यमानकञ्चुकमीक्षस्व मुखं मसृणमस्या: ।।
-(भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्रिकृत समच्छन्दोऽनुवाद) यह कल्पना और अभिव्यक्ति दोनों हृदयावर्जक हैं। इस उक्ति की गूंज आपको हर भाषा के साहित्य में मिल जाएगी। पिछले दिनो येसुदास का गाया एक गाना, जो एक दोहे से शुरू होता है, हमने सुना था, जिसमें यही बात कही गई है
सब तिथियन का चन्द्रमा देखा चाहो आज ।
धीरे-धीरे बूंघटा सरकाओ सरताज ।। अभिव्यक्ति की तरल-शैली का एक अन्य नमूना प्राकृत-गाथाओं से लेकर आज की नवीनतम उर्दू शायरी तक में लोकप्रिय हुआ है। प्रिय को पाती लिखने का प्रयत्न करते हो भाव-विह्वल हो जाने की विवशता सम्बोधन से आगे कुछ लिखने ही नहीं देती
वेविरसिण्ण-करंगुलि-परिगह-खलिअ लेहणीमग्गे।
सोत्यि व्विअ ण समप्पइ पियअहि लेहम्मि किं लिहिमो।। 3/44 भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने इसका समच्छन्दोनुवाद इसप्रकार किया है
कम्प्रस्विन्न-करांगुलिपरिग्रहस्खलित-लेखनी-मार्गे।
स्वस्त्येव पूर्यते नो प्रियसखि लेखे लिखाम: किम् ।। यह शैली पतिया में कैसे लिखू, लिखी ही न जाई' जैसी सैकड़ों गीतियों, मुक्तकों और शेरों में देखी जा सकती है। मूलत: यह लोकभावना की अभिव्यक्ति है, क्लासिकी साहित्य की अभिजात-शैली में कम ही मिलेगी। वैसे ऐसा बहुतायत से हुआ है कि लोकभाषाओं की ऐसी अभिव्यक्तियों को अभिजात-साहित्य ने अनूदित या उद्धृत कर अपने साहित्य में चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया हो। इसके उदाहरणस्वरूप पं० चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने अपभ्रंश की कुछ अभिव्यक्तियों को अभिजात-साहित्य के मूल-प्रेरक के रूप में उद्धत और विश्लेषित किया है, जिनमें सूरदास और कृष्ण का वह मिथक भी शामिल है कि सूरदास का हाथ पकड़कर कृष्ण ने उन्हें रास्ता पार करवाया; पर जब वे अचानक हाथ छुड़ाकर चले गये, तो सूरदास ने कहा
हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान कै मोहि। हिरदै से जब जाहुगे सबल बदौंगे तोहि ।।
0032
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000