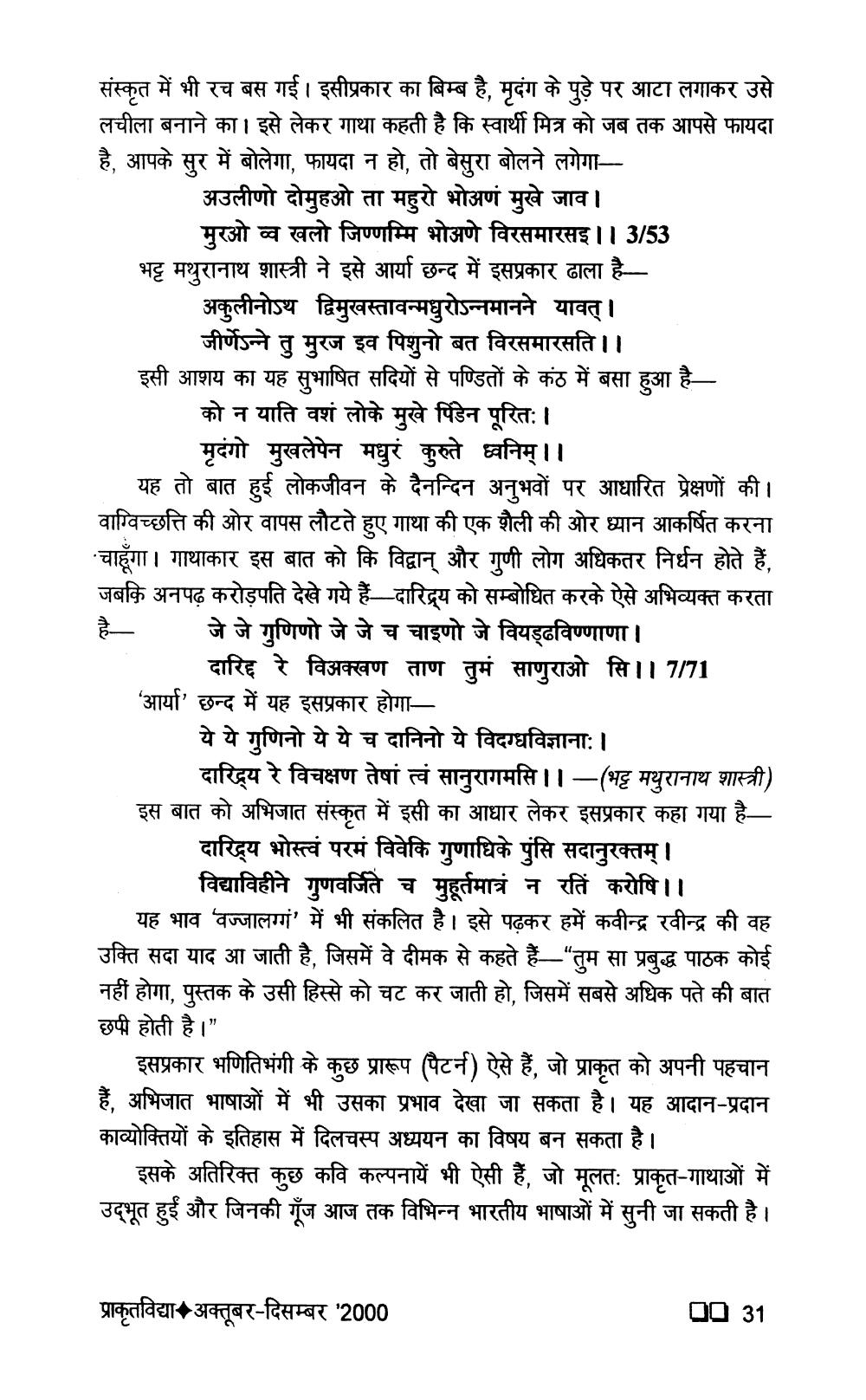________________
संस्कृत में भी रच बस गई। इसीप्रकार का बिम्ब है, मृदंग के पुड़े पर आटा लगाकर उसे लचीला बनाने का। इसे लेकर गाथा कहती है कि स्वार्थी मित्र को जब तक आपसे फायदा है, आपके सुर में बोलेगा, फायदा न हो, तो बेसुरा बोलने लगेगा
अउलीणो दोमुहओ ता महुरो भोअणं मुखे जाव।
मुरओ व्व खलो जिण्णम्मि भोअणे विरसमारसइ ।। 3/53 भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने इसे आर्या छन्द में इसप्रकार ढाला है
अकुलीनोऽथ द्विमुखस्तावन्मधुरोऽन्नमानने यावत् ।
जीर्णेऽन्ने तु मुरज इव पिशुनो बत विरसमारसति ।। इसी आशय का यह सुभाषित सदियों से पण्डितों के कंठ में बसा हुआ है—
को न याति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरित:।।
मृदंगो मुखलेपेन मधुरं कुरुते ध्वनिम् ।। __यह तो बात हुई लोकजीवन के दैनन्दिन अनुभवों पर आधारित प्रेक्षणों की। वाग्विच्छत्ति की ओर वापस लौटते हुए गाथा की एक शैली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। गाथाकार इस बात को कि विद्वान् और गुणी लोग अधिकतर निर्धन होते हैं, जबकि अनपढ़ करोड़पति देखे गये हैं—दारिद्र्य को सम्बोधित करके ऐसे अभिव्यक्त करता है- जे जे गणिणो जे जे च चाइणो जे वियड्ढविण्णाणा।
दारिद्द रे विअक्खण ताण तुमं साणुराओ सि।। 7/71 'आर्या' छन्द में यह इसप्रकार होगा
ये ये गुणिनो ये ये च दानिनो ये विदग्धविज्ञाना:।
दारिद्र्य रे विचक्षण तेषां त्वं सानुरागमसि ।। -(भट्ट मथुरानाथ शास्त्री) इस बात को अभिजात संस्कृत में इसी का आधार लेकर इसप्रकार कहा गया है—
दारिद्र्य भोस्त्वं परमं विवेकि गुणाधिके पुंसि सदानुरक्तम् ।
विद्याविहीने गुणवर्जिते च मुहूर्तमानं न रतिं करोषि।। यह भाव 'वज्जालग्गं' में भी संकलित है। इसे पढ़कर हमें कवीन्द्र रवीन्द्र की वह उक्ति सदा याद आ जाती है, जिसमें वे दीमक से कहते हैं—“तुम सा प्रबुद्ध पाठक कोई नहीं होगा, पुस्तक के उसी हिस्से को चट कर जाती हो, जिसमें सबसे अधिक पते की बात छपी होती है।" ___इसप्रकार भणितिभंगी के कुछ प्रारूप (पैटर्न) ऐसे हैं, जो प्राकृत को अपनी पहचान हैं, अभिजात भाषाओं में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। यह आदान-प्रदान काव्योक्तियों के इतिहास में दिलचस्प अध्ययन का विषय बन सकता है।
इसके अतिरिक्त कुछ कवि कल्पनायें भी ऐसी हैं, जो मूलत: प्राकृत-गाथाओं में उद्भूत हुईं और जिनकी गूंज आज तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुनी जा सकती है।
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000
40 31