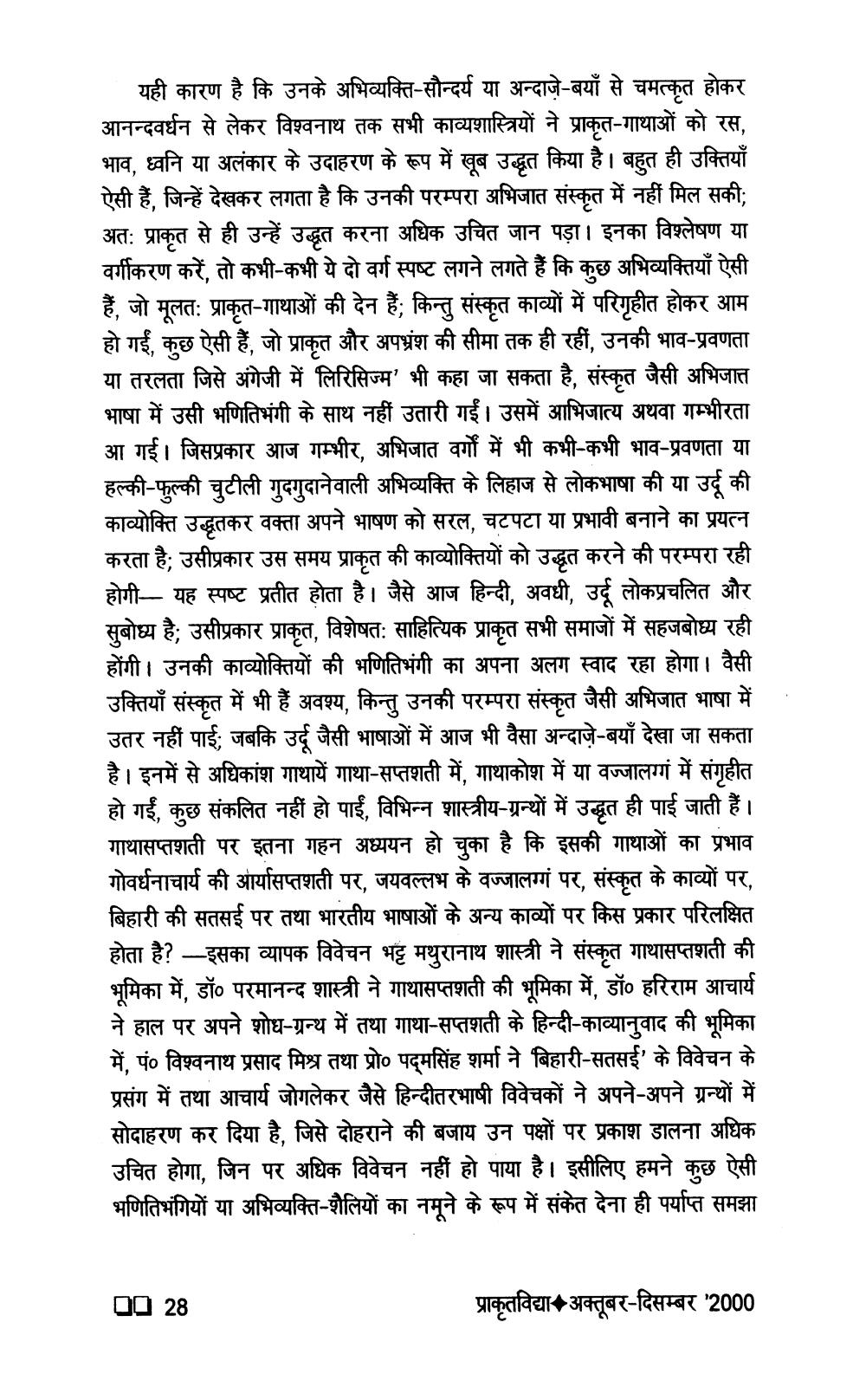________________
यही कारण है कि उनके अभिव्यक्ति-सौन्दर्य या अन्दाजे-बयाँ से चमत्कृत होकर आनन्दवर्धन से लेकर विश्वनाथ तक सभी काव्यशास्त्रियों ने प्राकृत-गाथाओं को रस, भाव, ध्वनि या अलंकार के उदाहरण के रूप में खूब उद्धत किया है। बहुत ही उक्तियाँ ऐसी हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उनकी परम्परा अभिजात संस्कृत में नहीं मिल सकी; अत: प्राकृत से ही उन्हें उद्धृत करना अधिक उचित जान पड़ा। इनका विश्लेषण या वर्गीकरण करें, तो कभी-कभी ये दो वर्ग स्पष्ट लगने लगते हैं कि कुछ अभिव्यक्तियाँ ऐसी हैं, जो मूलत: प्राकृत-गाथाओं की देन हैं; किन्तु संस्कृत काव्यों में परिगृहीत होकर आम हो गईं, कुछ ऐसी हैं, जो प्राकृत और अपभ्रंश की सीमा तक ही रहीं, उनकी भाव-प्रवणता या तरलता जिसे अंग्रेजी में लिरिसिज्म' भी कहा जा सकता है, संस्कृत जैसी अभिजात भाषा में उसी भणितिभंगी के साथ नहीं उतारी गईं। उसमें आभिजात्य अथवा गम्भीरता आ गई। जिसप्रकार आज गम्भीर, अभिजात वर्गों में भी कभी-कभी भाव-प्रवणता या हल्की-फुल्की चुटीली गुदगुदानेवाली अभिव्यक्ति के लिहाज से लोकभाषा की या उर्दू की काव्योक्ति उद्धृतकर वक्ता अपने भाषण को सरल, चटपटा या प्रभावी बनाने का प्रयत्न करता है; उसीप्रकार उस समय प्राकृत की काव्योक्तियों को उद्धत करने की परम्परा रही होगी- यह स्पष्ट प्रतीत होता है। जैसे आज हिन्दी, अवधी, उर्दू लोकप्रचलित और सुबोध्य है; उसीप्रकार प्राकृत, विशेषत: साहित्यिक प्राकृत सभी समाजों में सहजबोध्य रही होंगी। उनकी काव्योक्तियों की भणितिभंगी का अपना अलग स्वाद रहा होगा। वैसी उक्तियाँ संस्कृत में भी हैं अवश्य, किन्तु उनकी परम्परा संस्कृत जैसी अभिजात भाषा में उतर नहीं पाई; जबकि उर्दू जैसी भाषाओं में आज भी वैसा अन्दाजे-बयाँ देखा जा सकता है। इनमें से अधिकांश गाथायें गाथा-सप्तशती में, गाथाकोश में या वज्जालग्गं में संग्रहीत हो गईं, कुछ संकलित नहीं हो पाईं, विभिन्न शास्त्रीय-ग्रन्थों में उद्धृत ही पाई जाती हैं। गाथासप्तशती पर इतना गहन अध्ययन हो चुका है कि इसकी गाथाओं का प्रभाव गोवर्धनाचार्य की आर्यासप्तशती पर, जयवल्लभ के वज्जालग्गं पर, संस्कृत के काव्यों पर, बिहारी की सतसई पर तथा भारतीय भाषाओं के अन्य काव्यों पर किस प्रकार परिलक्षित होता है? – इसका व्यापक विवेचन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने संस्कृत गाथासप्तशती की भूमिका में, डॉ० परमानन्द शास्त्री ने गाथासप्तशती की भूमिका में, डॉ० हरिराम आचार्य ने हाल पर अपने शोध-ग्रन्थ में तथा गाथा-सप्तशती के हिन्दी-काव्यानुवाद की भूमिका में, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा प्रो० पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी-सतसई' के विवेचन के प्रसंग में तथा आचार्य जोगलेकर जैसे हिन्दीतरभाषी विवेचकों ने अपने-अपने ग्रन्थों में सोदाहरण कर दिया है, जिसे दोहराने की बजाय उन पक्षों पर प्रकाश डालना अधिक उचित होगा, जिन पर अधिक विवेचन नहीं हो पाया है। इसीलिए हमने कुछ ऐसी भणितिभंगियों या अभिव्यक्ति-शैलियों का नमूने के रूप में संकेत देना ही पर्याप्त समझा
00 28
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000