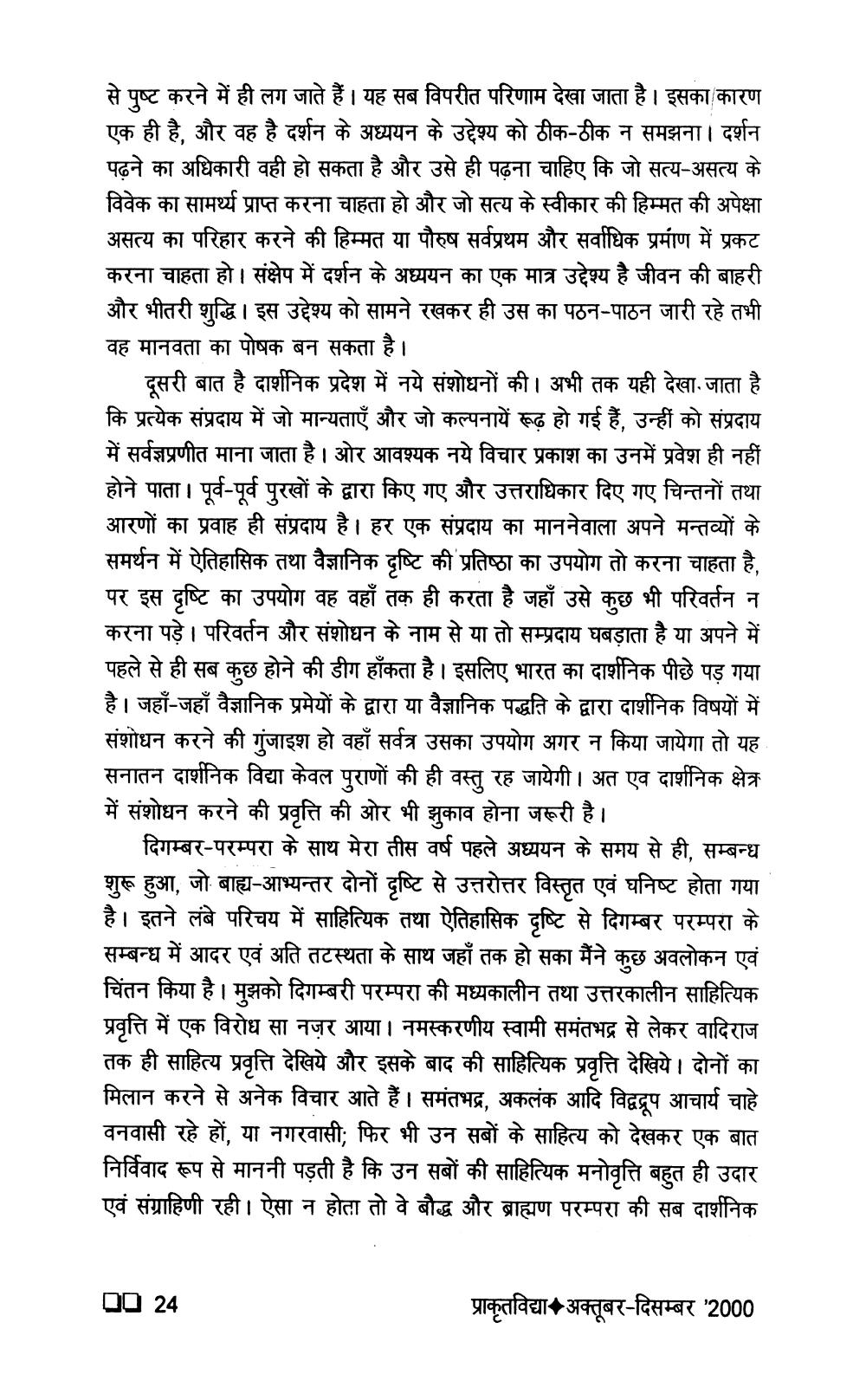________________
से
पुष्ट
करने में ही लग जाते हैं । यह सब विपरीत परिणाम देखा जाता है । इसका कारण एक ही है, और वह है दर्शन के अध्ययन के उद्देश्य को ठीक-ठीक न समझना । दर्शन पढ़ने का अधिकारी वही हो सकता है और उसे ही पढ़ना चाहिए कि जो सत्य-असत्य के विवेक का सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता हो और जो सत्य के स्वीकार की हिम्मत की अपेक्षा असत्य का परिहार करने की हिम्मत या पौरुष सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रमाण में प्रकट करना चाहता हो। संक्षेप में दर्शन के अध्ययन का एक मात्र उद्देश्य है जीवन की बाहरी और भीतरी शुद्धि। इस उद्देश्य को सामने रखकर ही उस का पठन-पाठन जारी रहे तभी वह मानवता का पोषक बन सकता है ।
दूसरी बात है दार्शनिक प्रदेश में नये संशोधनों की । अभी तक यही देखा जाता है कि प्रत्येक संप्रदाय में जो मान्यताएँ और जो कल्पनायें रूढ़ हो गई हैं, उन्हीं को संप्रदाय में सर्वज्ञप्रणीत माना जाता है। ओर आवश्यक नये विचार प्रकाश का उनमें प्रवेश ही नहीं होने पाता । पूर्व-पूर्व पुरखों के द्वारा किए गए और उत्तराधिकार दिए गए चिन्तनों तथा आरणों का प्रवाह ही संप्रदाय है । हर एक संप्रदाय का माननेवाला अपने मन्तव्यों के समर्थन में ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि की प्रतिष्ठा का उपयोग तो करना चाहता है, पर इस दृष्टि का उपयोग वह वहाँ तक ही करता है जहाँ उसे कुछ भी परिवर्तन न करना पड़े । परिवर्तन और संशोधन के नाम से या तो सम्प्रदाय घबड़ाता है या अपने में पहले से ही सब कुछ होने की डीग हाँकता है। इसलिए भारत का दार्शनिक पीछे पड़ गया है । जहाँ-जहाँ वैज्ञानिक प्रमेयों के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा दार्शनिक विषयों में संशोधन करने की गुंजाइश हो वहाँ सर्वत्र उसका उपयोग अगर न किया जायेगा तो यह सनातन दार्शनिक विद्या केवल पुराणों की ही वस्तु रह जायेगी । अत एव दार्शनिक क्षेत्र में संशोधन करने की प्रवृत्ति की ओर भी झुकाव होना जरूरी है।
दिगम्बर - परम्परा के साथ मेरा तीस वर्ष पहले अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुरू हुआ, जो बाह्य- आभ्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरोत्तर विस्तृत एवं घनिष्ट होता गया है। इतने लंबे परिचय में साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा के सम्बन्ध में आदर एवं अति तटस्थता के साथ जहाँ तक हो सका मैंने कुछ अवलोकन एवं चिंतन किया है। मुझको दिगम्बरी परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकालीन साहित्यिक प्रवृत्ति में एक विरोध सा नज़र आया । नमस्करणीय स्वामी समंतभद्र से लेकर वादिराज तक ही साहित्य प्रवृत्ति देखिये और इसके बाद की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिये । दोनों का मिलान करने से अनेक विचार आते हैं । समंतभद्र, अकलंक आदि विद्वद्रूप आचार्य चाहे वनवासी रहे हों, या नगरवासी; फिर भी उन सबों के साहित्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पड़ती है कि उन सबों की साहित्यिक मनोवृत्ति बहुत ही उदार एवं संग्राहिणी रही । ऐसा न होता तो वे बौद्ध और ब्राह्मण परम्परा की सब दार्शनिक
1
☐☐ 24
प्राकृतविद्या+अक्तूबर-दिसम्बर 2000