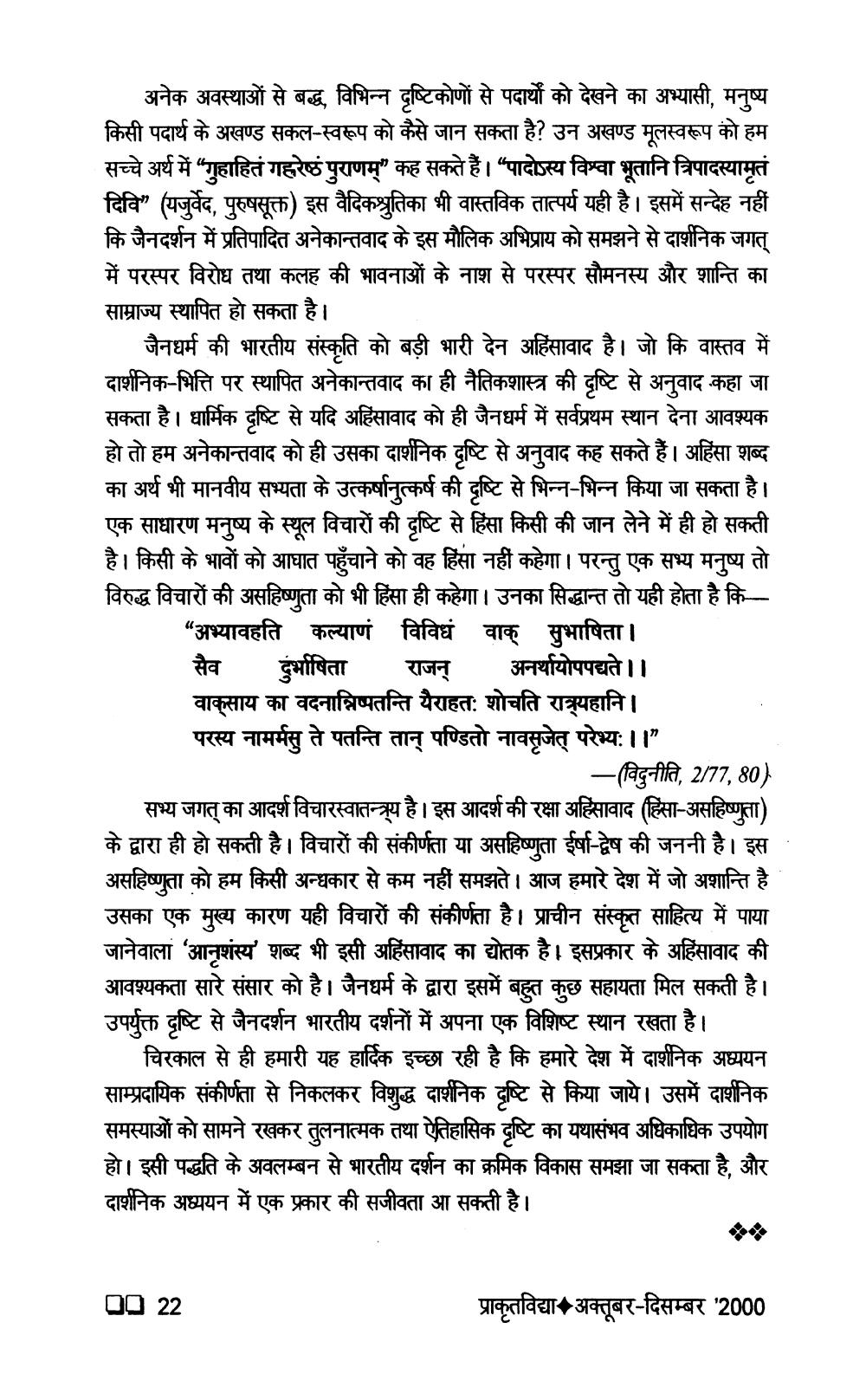________________
अनेक अवस्थाओं से बद्ध, विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थों को देखने का अभ्यासी, मनुष्य किसी पदार्थ के अखण्ड सकल-स्वरूप को कैसे जान सकता है? उन अखण्ड मूलस्वरूप को हम सच्चे अर्थ में "गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्" कह सकते हैं। “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" (यजुर्वेद, पुरुषसूक्त) इस वैदिकश्रुतिका भी वास्तविक तात्पर्य यही है। इसमें सन्देह नहीं कि जैनदर्शन में प्रतिपादित अनेकान्तवाद के इस मौलिक अभिप्राय को समझने से दार्शनिक जगत् में परस्पर विरोध तथा कलह की भावनाओं के नाश से परस्पर सौमनस्य और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है।
जैनधर्म की भारतीय संस्कृति को बड़ी भारी देन अहिंसावाद है। जो कि वास्तव में दार्शनिक-भित्ति पर स्थापित अनेकान्तवाद का ही नैतिकशास्त्र की दृष्टि से अनुवाद कहा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से यदि अहिंसावाद को ही जैनधर्म में सर्वप्रथम स्थान देना आवश्यक हो तो हम अनेकान्तवाद को ही उसका दार्शनिक दृष्टि से अनुवाद कह सकते हैं। अहिंसा शब्द का अर्थ भी मानवीय सभ्यता के उत्कर्षानुत्कर्ष की दृष्टि से भिन्न-भिन्न किया जा सकता है। एक साधारण मनुष्य के स्थूल विचारों की दृष्टि से हिंसा किसी की जान लेने में ही हो सकती है। किसी के भावों को आघात पहुंचाने को वह हिंसा नहीं कहेगा। परन्तु एक सभ्य मनुष्य तो विरुद्ध विचारों की असहिष्णुता को भी हिंसा ही कहेगा। उनका सिद्धान्त तो यही होता है कि
"अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता। सैव दुर्भाषिता राजन् अनायोपपद्यते।। वाक्साय का वदनानिष्पतन्ति यैराहत: शोचति रात्र्यहानि। परस्य नामर्मसु ते पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजेत् परेभ्यः ।।"
-(विदुनीति, 2/77, 80) सभ्य जगत् का आदर्श विचारस्वातन्त्र्य है। इस आदर्श की रक्षा अहिंसावाद (हिंसा-असहिष्णुता) के द्वारा ही हो सकती है। विचारों की संकीर्णता या असहिष्णुता ईर्षा-द्वेष की जननी है। इस . असहिष्णुता को हम किसी अन्धकार से कम नहीं समझते। आज हमारे देश में जो अशान्ति है उसका एक मुख्य कारण यही विचारों की संकीर्णता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाया जानेवाला 'आनृशंस्य' शब्द भी इसी अहिंसावाद का द्योतक है। इसप्रकार के अहिंसावाद की आवश्यकता सारे संसार को है। जैनधर्म के द्वारा इसमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। उपर्युक्त दृष्टि से जैनदर्शन भारतीय दर्शनों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।
चिरकाल से ही हमारी यह हार्दिक इच्छा रही है कि हमारे देश में दार्शनिक अध्ययन साम्प्रदायिक संकीर्णता से निकलकर विशुद्ध दार्शनिक दृष्टि से किया जाये। उसमें दार्शनिक समस्याओं को सामने रखकर तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि का यथासंभव अधिकाधिक उपयोग हो। इसी पद्धति के अवलम्बन से भारतीय दर्शन का क्रमिक विकास समझा जा सकता है, और दार्शनिक अध्ययन में एक प्रकार की सजीवता आ सकती है।
0022
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000