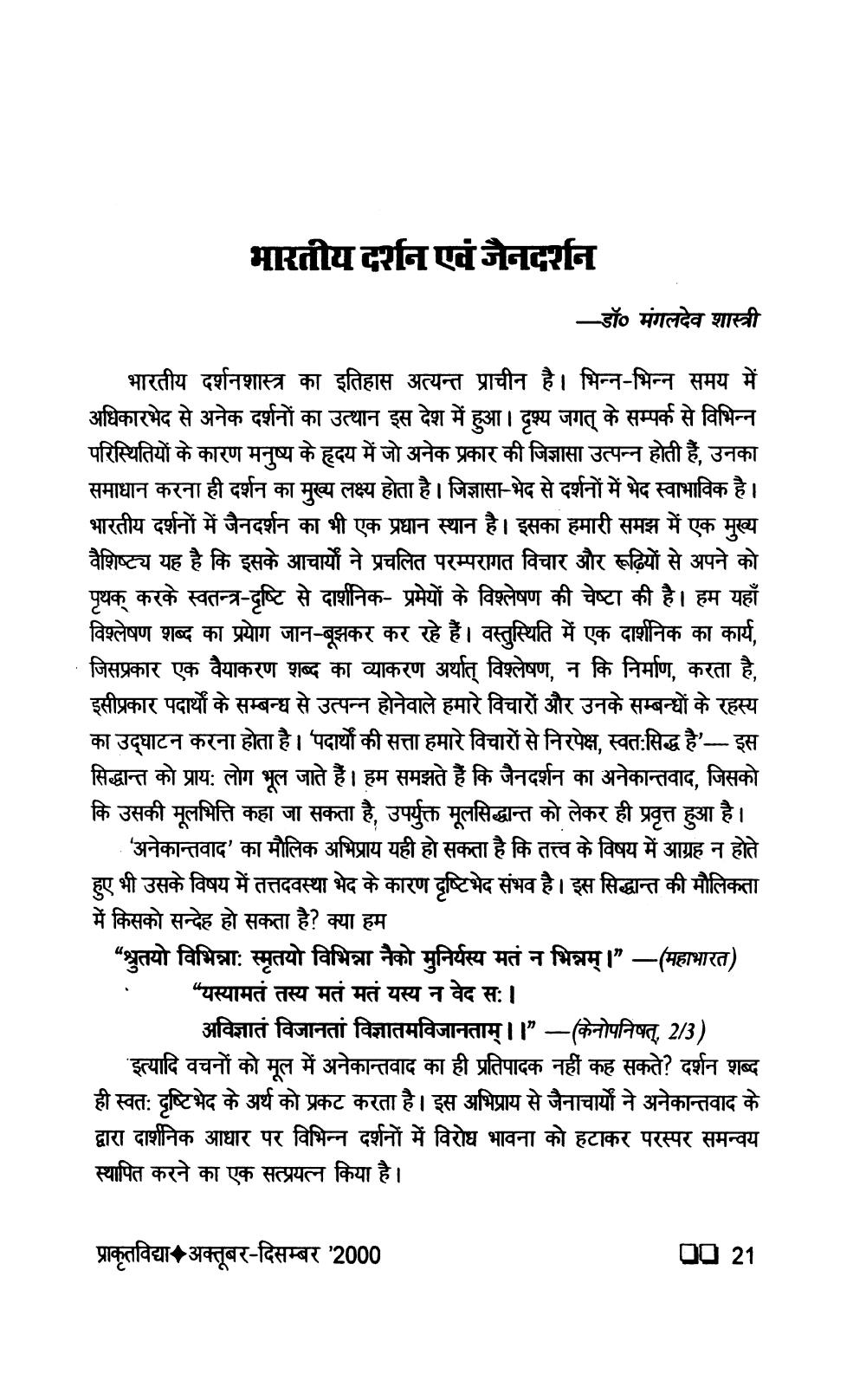________________
भारतीय दर्शन एवं जैनदर्शन
-डॉ० मंगलदेव शास्त्री
भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। भिन्न-भिन्न समय में अधिकारभेद से अनेक दर्शनों का उत्थान इस देश में हुआ। दृश्य जगत् के सम्पर्क से विभिन्न परिस्थितियों के कारण मनुष्य के हृदय में जो अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान करना ही दर्शन का मुख्य लक्ष्य होता है। जिज्ञासा-भेद से दर्शनों में भेद स्वाभाविक है। भारतीय दर्शनों में जैनदर्शन का भी एक प्रधान स्थान है। इसका हमारी समझ में एक मुख्य वैशिष्ट्य यह है कि इसके आचार्यों ने प्रचलित परम्परागत विचार और रूढ़ियों से अपने को पृथक् करके स्वतन्त्र-दृष्टि से दार्शनिक- प्रमेयों के विश्लेषण की चेष्टा की है। हम यहाँ विश्लेषण शब्द का प्रयोग जान-बूझकर कर रहे हैं। वस्तुस्थिति में एक दार्शनिक का कार्य, जिसप्रकार एक वैयाकरण शब्द का व्याकरण अर्थात् विश्लेषण, न कि निर्माण, करता है, इसीप्रकार पदार्थों के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले हमारे विचारों और उनके सम्बन्धों के रहस्य का उद्घाटन करना होता है। ‘पदार्थों की सत्ता हमारे विचारों से निरपेक्ष, स्वत:सिद्ध है'- इस सिद्धान्त को प्राय: लोग भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि जैनदर्शन का अनेकान्तवाद, जिसको कि उसकी मूलभित्ति कहा जा सकता है, उपर्युक्त मूलसिद्धान्त को लेकर ही प्रवृत्त हुआ है।
'अनेकान्तवाद' का मौलिक अभिप्राय यही हो सकता है कि तत्त्व के विषय में आग्रह न होते हुए भी उसके विषय में तत्तदवस्था भेद के कारण दृष्टिभेद संभव है। इस सिद्धान्त की मौलिकता में किसको सन्देह हो सकता है? क्या हम "श्रुतयो विभिन्ना: स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् ।” – (महाभारत) ___ “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स:।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ।।" -(केनोपनिषत्, 2/3) 'इत्यादि वचनों को मूल में अनेकान्तवाद का ही प्रतिपादक नहीं कह सकते? दर्शन शब्द ही स्वत: दृष्टिभेद के अर्थ को प्रकट करता है। इस अभिप्राय से जैनाचार्यों ने अनेकान्तवाद के द्वारा दार्शनिक आधार पर विभिन्न दर्शनों में विरोध भावना को हटाकर परस्पर समन्वय स्थापित करने का एक सत्प्रयत्न किया है।
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000
0021