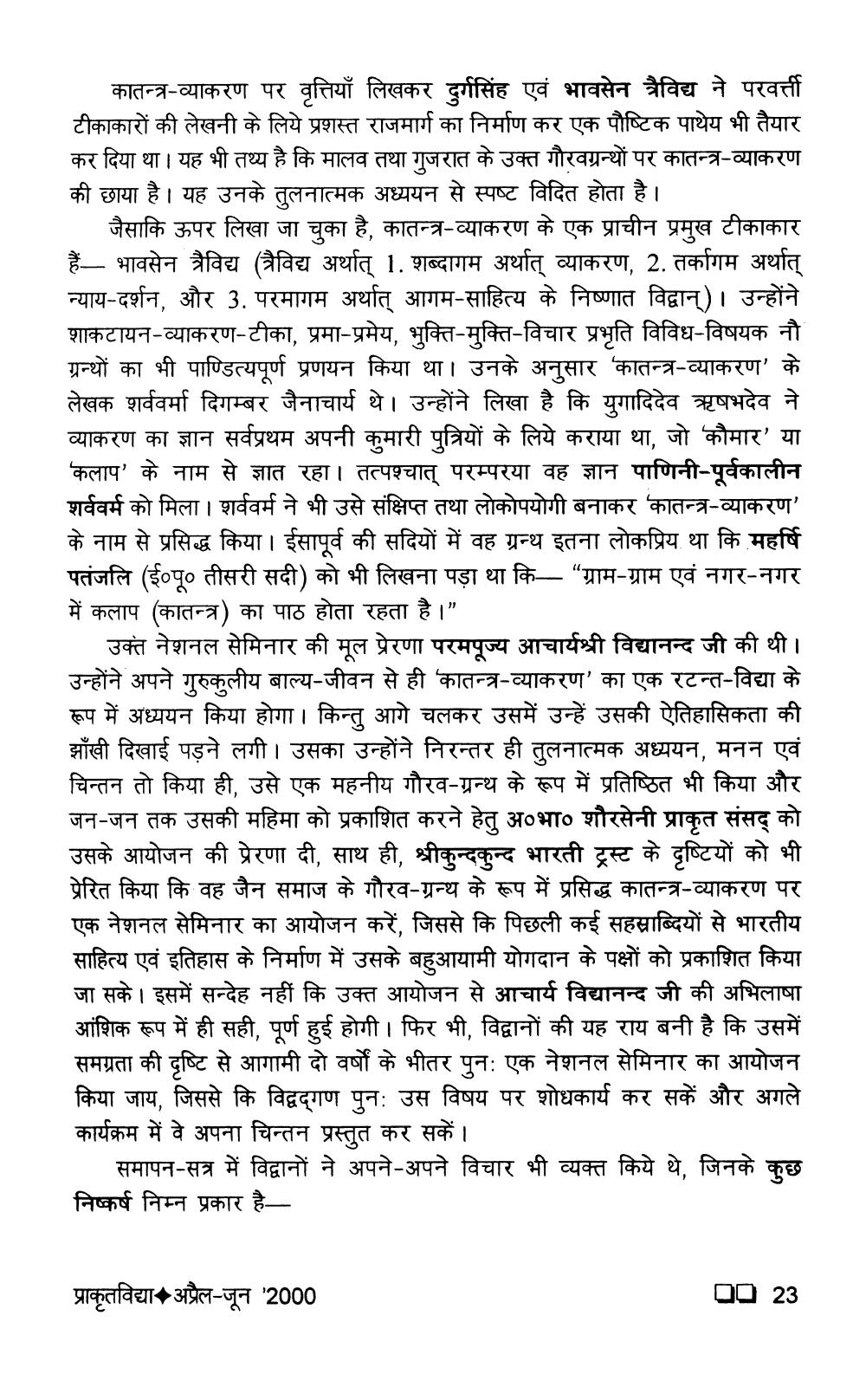________________
कातन्त्र-व्याकरण पर वृत्तियाँ लिखकर दुर्गसिंह एवं भावसेन विद्य ने परवर्ती टीकाकारों की लेखनी के लिये प्रशस्त राजमार्ग का निर्माण कर एक पौष्टिक पाथेय भी तैयार कर दिया था। यह भी तथ्य है कि मालव तथा गुजरात के उक्त गौरवग्रन्थों पर कातन्त्र-व्याकरण की छाया है। यह उनके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट विदित होता है।
जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, कातन्त्र-व्याकरण के एक प्राचीन प्रमुख टीकाकार हैं— भावसेन त्रैविद्य (विद्य अर्थात् 1. शब्दागम अर्थात् व्याकरण, 2. तर्कागम अर्थात् न्याय-दर्शन, और 3. परमागम अर्थात् आगम-साहित्य के निष्णात विद्वान्)। उन्होंने शाकटायन-व्याकरण-टीका, प्रमा-प्रमेय, भुक्ति-मुक्ति-विचार प्रभृति विविध-विषयक नौ ग्रन्थों का भी पाण्डित्यपूर्ण प्रणयन किया था। उनके अनुसार 'कातन्त्र-व्याकरण' के लेखक शर्ववर्मा दिगम्बर जैनाचार्य थे। उन्होंने लिखा है कि युगादिदेव ऋषभदेव ने व्याकरण का ज्ञान सर्वप्रथम अपनी कुमारी पुत्रियों के लिये कराया था, जो कौमार' या 'कलाप' के नाम से ज्ञात रहा। तत्पश्चात् परम्परया वह ज्ञान पाणिनी-पूर्वकालीन शर्ववर्म को मिला। शर्ववर्म ने भी उसे संक्षिप्त तथा लोकोपयोगी बनाकर कातन्त्र-व्याकरण' के नाम से प्रसिद्ध किया। ईसापूर्व की सदियों में वह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय था कि महर्षि पतंजलि (ई०पू० तीसरी सदी) को भी लिखना पड़ा था कि- “ग्राम-ग्राम एवं नगर-नगर में कलाप (कातन्त्र) का पाठ होता रहता है।"
उक्त नेशनल सेमिनार की मूल प्रेरणा परमपूज्य आचार्यश्री विद्यानन्द जी की थी। उन्होंने अपने गुरुकुलीय बाल्य-जीवन से ही कातन्त्र-व्याकरण' का एक रटन्त-विद्या के रूप में अध्ययन किया होगा। किन्तु आगे चलकर उसमें उन्हें उसकी ऐतिहासिकता की झाँखी दिखाई पड़ने लगी। उसका उन्होंने निरन्तर ही तुलनात्मक अध्ययन, मनन एवं चिन्तन तो किया ही, उसे एक महनीय गौरव-ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित भी किया और जन-जन तक उसकी महिमा को प्रकाशित करने हेतु अ०भा० शौरसेनी प्राकृत संसद् को उसके आयोजन की प्रेरणा दी, साथ ही, श्रीकुन्दकुन्द भारती ट्रस्ट के दृष्टियों को भी प्रेरित किया कि वह जैन समाज के गौरव-ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध कातन्त्र-व्याकरण पर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन करें, जिससे कि पिछली कई सहस्राब्दियों से भारतीय साहित्य एवं इतिहास के निर्माण में उसके बहुआयामी योगदान के पक्षों को प्रकाशित किया जा सके। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त आयोजन से आचार्य विद्यानन्द जी की अभिलाषा आंशिक रूप में ही सही, पूर्ण हुई होगी। फिर भी, विद्वानों की यह राय बनी है कि उसमें समग्रता की दृष्टि से आगामी दो वर्षों के भीतर पुन: एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाय, जिससे कि विद्वद्गण पुन: उस विषय पर शोधकार्य कर सकें और अगले कार्यक्रम में वे अपना चिन्तन प्रस्तुत कर सकें।
समापन-सत्र में विद्वानों ने अपने-अपने विचार भी व्यक्त किये थे, जिनके कुछ निष्कर्ष निम्न प्रकार है
प्राकृतविद्या अप्रैल-जून "2000
00 23