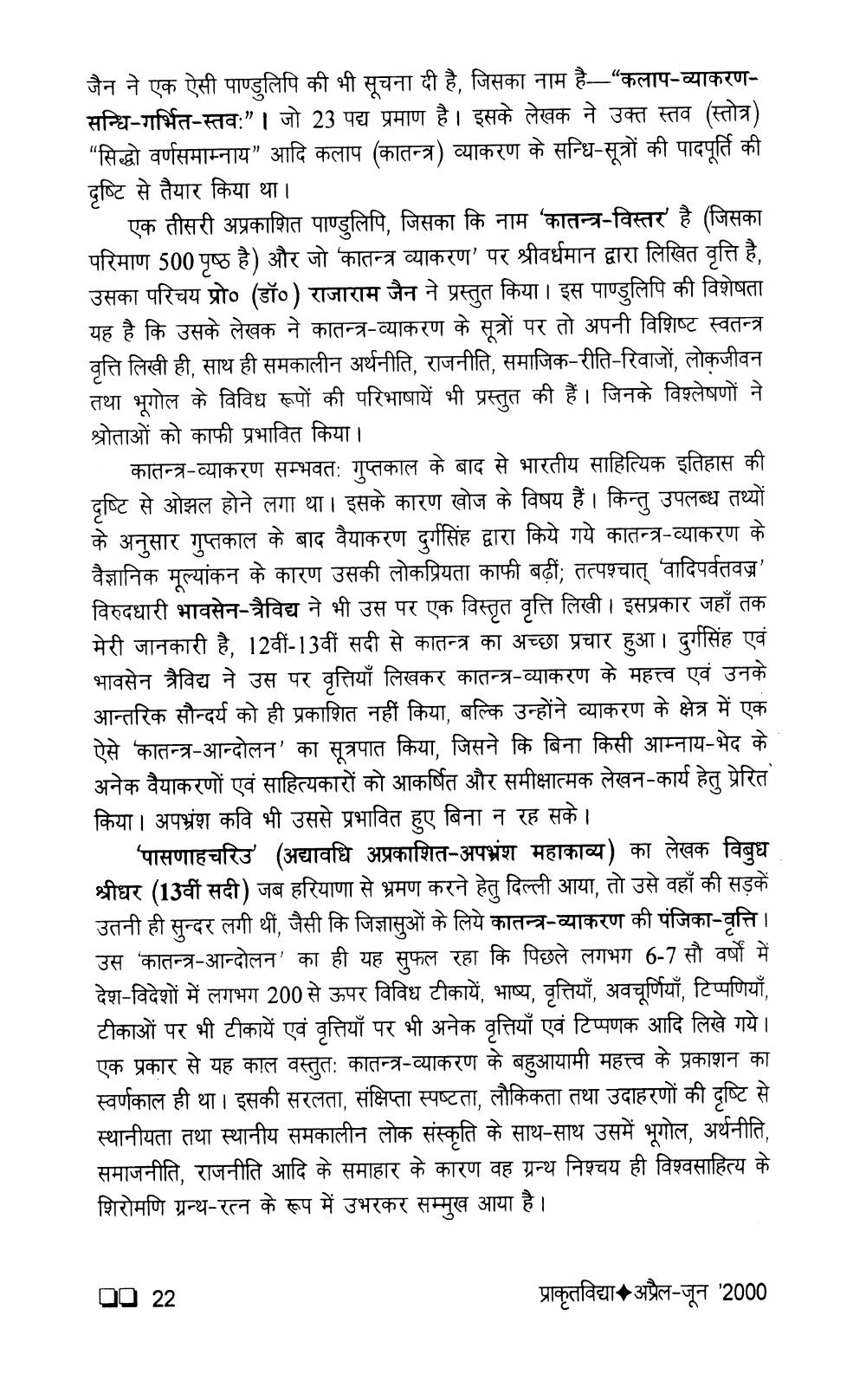________________
जैन ने एक ऐसी पाण्डुलिपि की भी सूचना दी है, जिसका नाम है—“कलाप-व्याकरणसन्धि-गर्भित-स्तवः” । जो 23 पद्य प्रमाण है। इसके लेखक ने उक्त स्तव (स्तोत्र) "सिद्धो वर्णसमाम्नाय" आदि कलाप (कातन्त्र) व्याकरण के सन्धि-सूत्रों की पादपूर्ति की दृष्टि से तैयार किया था। ____ एक तीसरी अप्रकाशित पाण्डुलिपि, जिसका कि नाम 'कातन्त्र-विस्तर' है (जिसका परिमाण 500 पृष्ठ है) और जो कातन्त्र व्याकरण' पर श्रीवर्धमान द्वारा लिखित वृत्ति है, उसका परिचय प्रो० (डॉ०) राजाराम जैन ने प्रस्तुत किया। इस पाण्डुलिपि की विशेषता यह है कि उसके लेखक ने कातन्त्र-व्याकरण के सूत्रों पर तो अपनी विशिष्ट स्वतन्त्र वृत्ति लिखी ही, साथ ही समकालीन अर्थनीति, राजनीति, समाजिक-रीति-रिवाजों, लोकजीवन तथा भूगोल के विविध रूपों की परिभाषायें भी प्रस्तुत की हैं। जिनके विश्लेषणों ने श्रोताओं को काफी प्रभावित किया।
कातन्त्र-व्याकरण सम्भवत: गुप्तकाल के बाद से भारतीय साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से ओझल होने लगा था। इसके कारण खोज के विषय हैं। किन्तु उपलब्ध तथ्यों के अनुसार गुप्तकाल के बाद वैयाकरण दुर्गसिंह द्वारा किये गये कातन्त्र-व्याकरण के वैज्ञानिक मूल्यांकन के कारण उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ीं; तत्पश्चात् 'वादिपर्वतवज्र' विरुदधारी भावसेन-त्रैविद्य ने भी उस पर एक विस्तृत वृत्ति लिखी। इसप्रकार जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12वीं-13वीं सदी से कातन्त्र का अच्छा प्रचार हुआ। दुर्गसिंह एवं भावसेन त्रैविद्य ने उस पर वृत्तियाँ लिखकर कातन्त्र-व्याकरण के महत्त्व एवं उनके आन्तरिक सौन्दर्य को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में एक ऐसे कातन्त्र-आन्दोलन' का सूत्रपात किया, जिसने कि बिना किसी आम्नाय-भेद के अनेक वैयाकरणों एवं साहित्यकारों को आकर्षित और समीक्षात्मक लेखन-कार्य हेतु प्रेरित किया। अपभ्रंश कवि भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके।
‘पासणाहचरिउ' (अद्यावधि अप्रकाशित-अपभ्रंश महाकाव्य) का लेखक विबुध श्रीधर (13वीं सदी) जब हरियाणा से भ्रमण करने हेतु दिल्ली आया, तो उसे वहाँ की सड़कें उतनी ही सुन्दर लगी थीं, जैसी कि जिज्ञासुओं के लिये कातन्त्र-व्याकरण की पंजिका-वृत्ति। उस 'कातन्त्र-आन्दोलन' का ही यह सुफल रहा कि पिछले लगभग 6-7 सौ वर्षों में देश-विदेशों में लगभग 200 से ऊपर विविध टीकायें, भाष्य, वृत्तियाँ, अवचूर्णियाँ, टिप्पणियाँ, टीकाओं पर भी टीकायें एवं वृत्तियाँ पर भी अनेक वृत्तियाँ एवं टिप्पणक आदि लिखे गये। एक प्रकार से यह काल वस्तुत: कातन्त्र-व्याकरण के बहुआयामी महत्त्व के प्रकाशन का स्वर्णकाल ही था। इसकी सरलता, संक्षिप्ता स्पष्टता, लौकिकता तथा उदाहरणों की दृष्टि से स्थानीयता तथा स्थानीय समकालीन लोक संस्कृति के साथ-साथ उसमें भूगोल, अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति आदि के समाहार के कारण वह ग्रन्थ निश्चय ही विश्वसाहित्य के शिरोमणि ग्रन्थ-रत्न के रूप में उभरकर सम्मुख आया है।
0022
प्राकृतविद्या अप्रैल-जून '2000