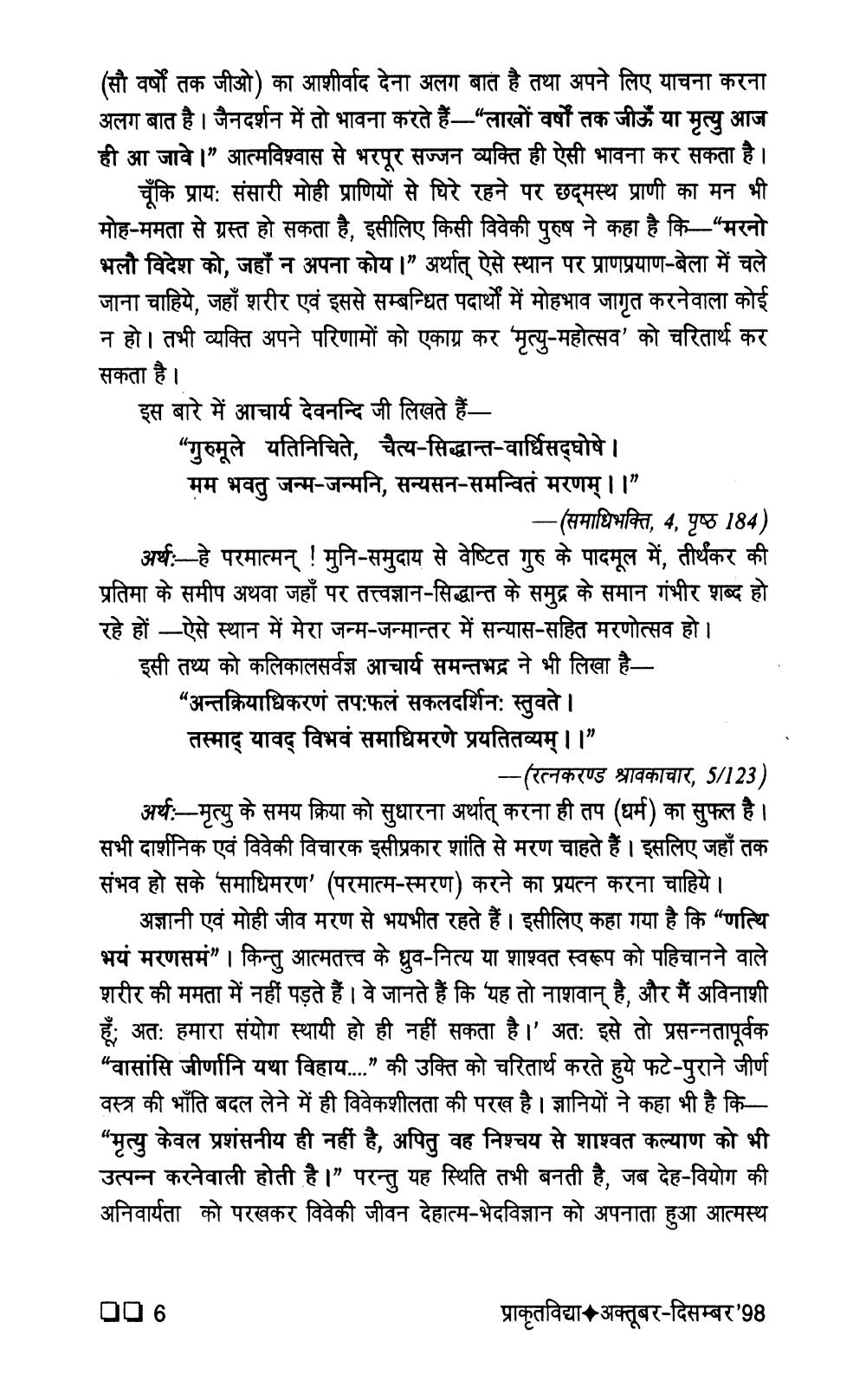________________
(सौ वर्षों तक जीओ) का आशीर्वाद देना अलग बात है तथा अपने लिए याचना करना अलग बात है। जैनदर्शन में तो भावना करते हैं—“लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे।" आत्मविश्वास से भरपूर सज्जन व्यक्ति ही ऐसी भावना कर सकता है।
चूँकि प्राय: संसारी मोही प्राणियों से घिरे रहने पर छद्मस्थ प्राणी का मन भी मोह-ममता से ग्रस्त हो सकता है, इसीलिए किसी विवेकी पुरुष ने कहा है कि-"मरनो भलौ विदेश को, जहाँ न अपना कोय ।" अर्थात् ऐसे स्थान पर प्राणप्रयाण-बेला में चले जाना चाहिये, जहाँ शरीर एवं इससे सम्बन्धित पदार्थों में मोहभाव जागृत करनेवाला कोई न हो। तभी व्यक्ति अपने परिणामों को एकाग्र कर 'मृत्यु-महोत्सव' को चरितार्थ कर सकता है। इस बारे में आचार्य देवनन्दि जी लिखते हैं
"गुरुमूले यतिनिचिते, चैत्य-सिद्धान्त-वार्धिसद्घोषे। मम भवतु जन्म-जन्मनि, सन्यसन-समन्वितं मरणम् ।।"
-(समाधिभक्ति, 4, पृष्ठ 184) अर्थ:-हे परमात्मन् ! मुनि-समुदाय से वेष्टित गुरु के पादमूल में, तीर्थंकर की प्रतिमा के समीप अथवा जहाँ पर तत्त्वज्ञान-सिद्धान्त के समुद्र के समान गंभीर शब्द हो रहे हों ऐसे स्थान में मेरा जन्म-जन्मान्तर में सन्यास-सहित मरणोत्सव हो। इसी तथ्य को कलिकालसर्वज्ञ आचार्य समन्तभद्र ने भी लिखा है
“अन्तक्रियाधिकरणं तप:फलं सकलदर्शिन: स्तुवते । तस्माद् यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ।।"
-(रत्नकरण्ड श्रावकाचार, 5/123) अर्थ:-मृत्यु के समय क्रिया को सुधारना अर्थात् करना ही तप (धर्म) का सुफल है। सभी दार्शनिक एवं विवेकी विचारक इसीप्रकार शांति से मरण चाहते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके 'समाधिमरण' (परमात्म-स्मरण) करने का प्रयत्न करना चाहिये।
अज्ञानी एवं मोही जीव मरण से भयभीत रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि "णत्थि भयं मरणसमं"। किन्तु आत्मतत्त्व के ध्रुव-नित्य या शाश्वत स्वरूप को पहिचानने वाले शरीर की ममता में नहीं पड़ते हैं। वे जानते हैं कि 'यह तो नाशवान् है, और मैं अविनाशी हूँ; अत: हमारा संयोग स्थायी हो ही नहीं सकता है।' अत: इसे तो प्रसन्नतापूर्वक "वासांसि जीर्णानि यथा विहाय....” की उक्ति को चरितार्थ करते हुये फटे-पुराने जीर्ण वस्त्र की भाँति बदल लेने में ही विवेकशीलता की परख है। ज्ञानियों ने कहा भी है कि"मृत्यु केवल प्रशंसनीय ही नहीं है, अपितु वह निश्चय से शाश्वत कल्याण को भी उत्पन्न करनेवाली होती है।” परन्तु यह स्थिति तभी बनती है, जब देह-वियोग की अनिवार्यता को परखकर विवेकी जीवन देहात्म-भेदविज्ञान को अपनाता हुआ आत्मस्थ
006
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर'98